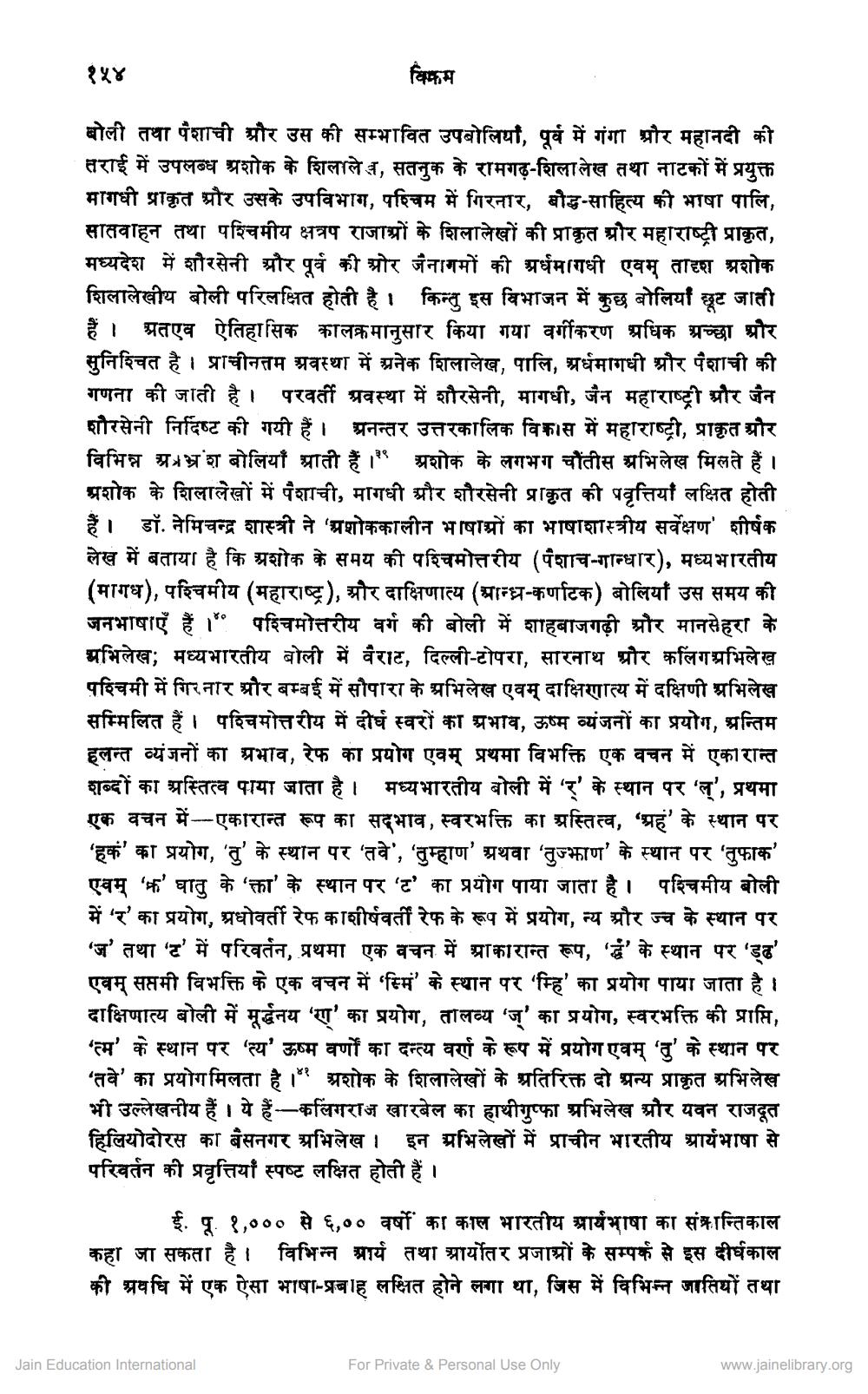________________
१५४
विक्रम
बोली तथा पैशाची और उस की सम्भावित उपबोलियाँ, पूर्व में गंगा और महानदी की तराई में उपलब्ध अशोक के शिलालेख, सतनुक के रामगढ़-शिलालेख तथा नाटकों में प्रयुक्त मागधी प्राकृत और उसके उपविभाग, पश्चिम में गिरनार, बौद्ध-साहित्य की भाषा पालि, सातवाहन तथा पश्चिमीय क्षत्रप राजाओं के शिलालेखों की प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत, मध्यदेश में शौरसेनी और पूर्व की ओर जैनागमों की अर्धमागधी एवम् तादृश अशोक शिलालेखीय बोली परिलक्षित होती है। किन्तु इस विभाजन में कुछ बोलियां छूट जाती हैं। अतएव ऐतिहासिक कालक्रमानुसार किया गया वर्गीकरण अधिक अच्छा और सुनिश्चित है। प्राचीनतम अवस्था में अनेक शिलालेख, पालि, अर्धमागधी और पैशाची की गणना की जाती है। परवर्ती अवस्था में शौरसेनी, मागधी, जैन महाराष्ट्री और जैन शौरसेनी निर्दिष्ट की गयी हैं। अनन्तर उत्तरकालिक विकास में महाराष्ट्री, प्राकृत और विभिन्न अभ्रश बोलियाँ आती हैं ।३९ अशोक के लगभग चौंतीस अभिलेख मिलते हैं । प्रशोक के शिलालेखों में पैशाची, मागधी और शौरसेनी प्राकृत की प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं। डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री ने 'अशोककालीन भाषाओं का भाषाशास्त्रीय सर्वेक्षण' शीर्षक लेख में बताया है कि अशोक के समय की पश्चिमोत्तरीय (पैशाच-गान्धार), मध्य भारतीय (मागध), पश्चिमीय (महाराष्ट्र), और दाक्षिणात्य (आन्ध्र-कर्णाटक) बोलियाँ उस समय की जनभाषाएँ हैं । पश्चिमोत्तरीय वर्ग की बोली में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख; मध्यभारतीय बोली में वैराट, दिल्ली-टोपरा, सारनाथ और कलिंगअभिलेख पश्चिमी में गिरनार और बम्बई में सौपारा के अभिलेख एवम् दाक्षिणात्य में दक्षिणी अभिलेख सम्मिलित हैं। पश्चिमोत्तरीय में दीर्घ स्वरों का प्रभाव, ऊष्म व्यंजनों का प्रयोग, अन्तिम हलन्त व्यंजनों का प्रभाव, रेफ का प्रयोग एवम् प्रथमा विभक्ति एक वचन में एकारान्त शब्दों का अस्तित्व पाया जाता है। मध्यभारतीय बोली में 'र' के स्थान पर 'ल', प्रथमा एक वचन में-एकारान्त रूप का सद्भाव, स्वरभक्ति का अस्तित्व, 'अहं' के स्थान पर 'हक' का प्रयोग, 'तु' के स्थान पर 'तवे', 'तुम्हाण' अथवा 'तुज्झाण' के स्थान पर 'तुफाक' एवम् 'क' घातु के 'क्ता' के स्थान पर 'ट' का प्रयोग पाया जाता है। पश्चिमीय बोली में 'र' का प्रयोग, अधोवर्ती रेफ काशीर्षवर्ती रेफ के रूप में प्रयोग, न्य और ज्च के स्थान पर 'ज' तथा 'ट' में परिवर्तन, प्रथमा एक वचन में प्राकारान्त रूप, 'x' के स्थान पर 'ड्ढ' एवम् सप्तमी विभक्ति के एक वचन में 'स्मि' के स्थान पर 'म्हि' का प्रयोग पाया जाता है । दाक्षिणात्य बोली में मूर्द्धनय 'रण' का प्रयोग, तालव्य 'ज्' का प्रयोग, स्वरभक्ति की प्राप्ति, 'त्म' के स्थान पर 'त्य' ऊष्म वर्णों का दन्त्य वर्ण के रूप में प्रयोग एवम् 'तु' के स्थान पर 'तवे' का प्रयोग मिलता है। अशोक के शिलालेखों के अतिरिक्त दो अन्य प्राकृत अभिलेख भी उल्लेखनीय हैं । ये हैं--कलिंगराज खारबेल का हाथीगुप्फा अभिलेख और यवन राजदूत हिलियोदोरस का बैसनगर अभिलेख। इन अभिलेखों में प्राचीन भारतीय आर्यभाषा से परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट लक्षित होती हैं ।
__ ई. पू. १,००० से ६,०० वर्षों का काल भारतीय आर्यभाषा का संक्रान्तिकाल कहा जा सकता है। विभिन्न आर्य तथा आर्योतर प्रजात्रों के सम्पर्क से इस दीर्घकाल की अवधि में एक ऐसा भाषा-प्रबाह लक्षित होने लगा था, जिस में विभिन्न जातियों तथा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org