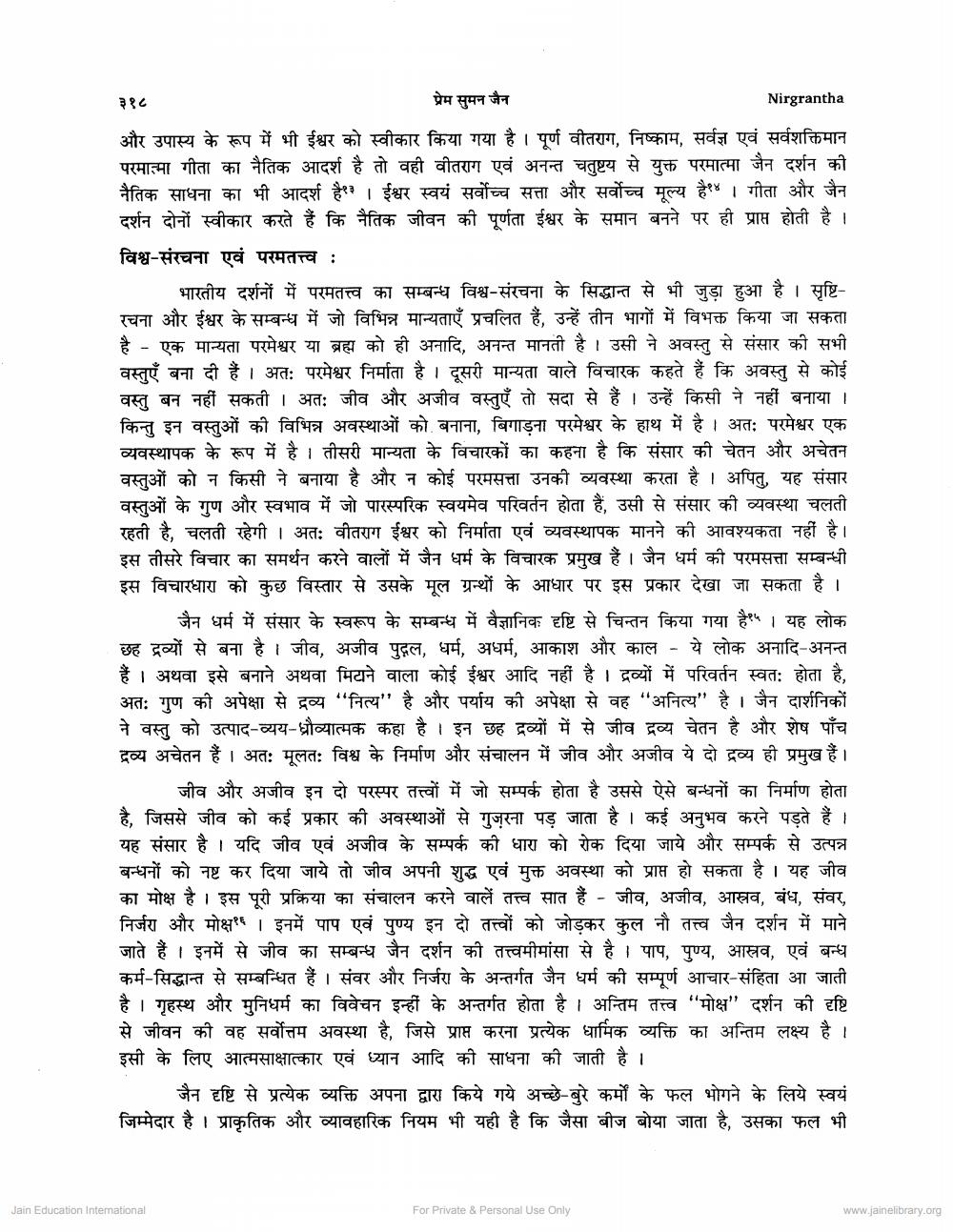________________
३१८
प्रेम सुमन जैन
Nirgrantha
और उपास्य के रूप में भी ईश्वर को स्वीकार किया गया है। पूर्ण वीतराग, निष्काम, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा गीता का नैतिक आदर्श है तो वही वीतराग एवं अनन्त चतुष्टय से युक्त परमात्मा जैन दर्शन की नैतिक साधना का भी आदर्श है" ईश्वर स्वयं सर्वोच्च सत्ता और सर्वोच्च मूल्य है। गीता और जैन दर्शन दोनों स्वीकार करते हैं कि नैतिक जीवन की पूर्णता ईश्वर के समान बनने पर ही प्राप्त होती है ।
विश्व संरचना एवं परमतत्त्व
भारतीय दर्शनों में परमतत्त्व का सम्बन्ध विश्व-संरचना के सिद्धान्त से भी जुड़ा हुआ है । सृष्टिरचना और ईश्वर के सम्बन्ध में जो विभिन्न मान्यताएँ प्रचलित है, उन्हें तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है - एक मान्यता परमेश्वर या ब्रह्म को ही अनादि, अनन्त मानती है। उसी ने अवस्तु से संसार की सभी वस्तुएँ बना दी हैं। अतः परमेश्वर निर्माता है। दूसरी मान्यता वाले विचारक कहते हैं कि अवस्तु से कोई वस्तु बन नहीं सकती। अतः जीव और अजीव वस्तुएँ तो सदा से हैं उन्हें किसी ने नहीं बनाया । किन्तु इन वस्तुओं की विभिन्न अवस्थाओं को बनाना, बिगाड़ना परमेश्वर के हाथ में है। अतः परमेश्वर एक व्यवस्थापक के रूप में है तीसरी मान्यता के विचारकों का कहना है कि संसार की चेतन और अचेतन वस्तुओं को न किसी ने बनाया है और न कोई परमसत्ता उनकी व्यवस्था करता है। अपितु यह संसार वस्तुओं के गुण और स्वभाव में जो पारस्परिक स्वयमेव परिवर्तन होता हैं, उसी से संसार की व्यवस्था चलती रहती है, चलती रहेगी । अतः वीतराग ईश्वर को निर्माता एवं व्यवस्थापक मानने की आवश्यकता नहीं है। इस तीसरे विचार का समर्थन करने वालों में जैन धर्म के विचारक प्रमुख हैं। जैन धर्म की परमसत्ता सम्बन्धी इस विचारधारा को कुछ विस्तार से उसके मूल ग्रन्थों के आधार पर इस प्रकार देखा जा सकता है ।
1
जैन धर्म में संसार के स्वरूप के सम्बन्ध में वैज्ञानिक दृष्टि से चिन्तन किया गया है १५ । यह लोक छह द्रव्यों से बना है। जीव, अजीव पुगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल - ये लोक अनादि-अनन्त हैं। अथवा इसे बनाने अथवा मिटाने वाला कोई ईश्वर आदि नहीं है। द्रव्यों में परिवर्तन स्वतः होता है, अतः गुण की अपेक्षा से द्रव्य "नित्य" है और पर्याय की अपेक्षा से वह "अनित्य" है। जैन दार्शनिकों ने वस्तु को उत्पाद - व्यय- ध्रौव्यात्मक कहा है । इन छह द्रव्यों में से जीव द्रव्य चेतन है और शेष पाँच द्रव्य अचेतन है । अतः मूलतः विश्व के निर्माण और संचालन में जीव और अजीव ये दो द्रव्य ही प्रमुख हैं।
जीव और अजीव इन दो परस्पर तत्त्वों में जो सम्पर्क होता है उससे ऐसे बन्धनों का निर्माण होता है, जिससे जीव को कई प्रकार की अवस्थाओं से गुज़रना पड़ जाता है। कई अनुभव करने पड़ते हैं । यह संसार है। यदि जीव एवं अजीव के सम्पर्क की धारा को रोक दिया जाये और सम्पर्क से उत्पन्न बन्धनों को नष्ट कर दिया जाये तो जीव अपनी शुद्ध एवं मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकता है । यह जीव का मोक्ष है । इस पूरी प्रक्रिया का संचालन करने वालें तत्त्व सात हैं- जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष १६ । इनमें पाप एवं पुण्य इन दो तत्त्वों को जोड़कर कुल नौ तत्त्व जैन दर्शन में माने जाते हैं। इनमें से जीव का सम्बन्ध जैन दर्शन की तत्त्वमीमांसा से है। पाप, पुण्य, आस्रव, एवं बन्ध कर्म सिद्धान्त से सम्बन्धित है। संवर और निर्जरा के अन्तर्गत जैन धर्म की सम्पूर्ण आचार संहिता आ जाती है। गृहस्थ और मुनिधर्म का विवेचन इन्हीं के अन्तर्गत होता है। अन्तिम तत्त्व "मोक्ष" दर्शन की दृष्टि से जीवन की वह सर्वोत्तम अवस्था है, जिसे प्राप्त करना प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का अन्तिम लक्ष्य है । इसी के लिए आत्मसाक्षात्कार एवं ध्यान आदि की साधना की जाती है।
जैन दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपना द्वारा किये गये अच्छे-बुरे कर्मों के फल भोगने के लिये स्वयं जिम्मेदार है । प्राकृतिक और व्यावहारिक नियम भी यही है कि जैसा बीज बोया जाता है, उसका फल भी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org