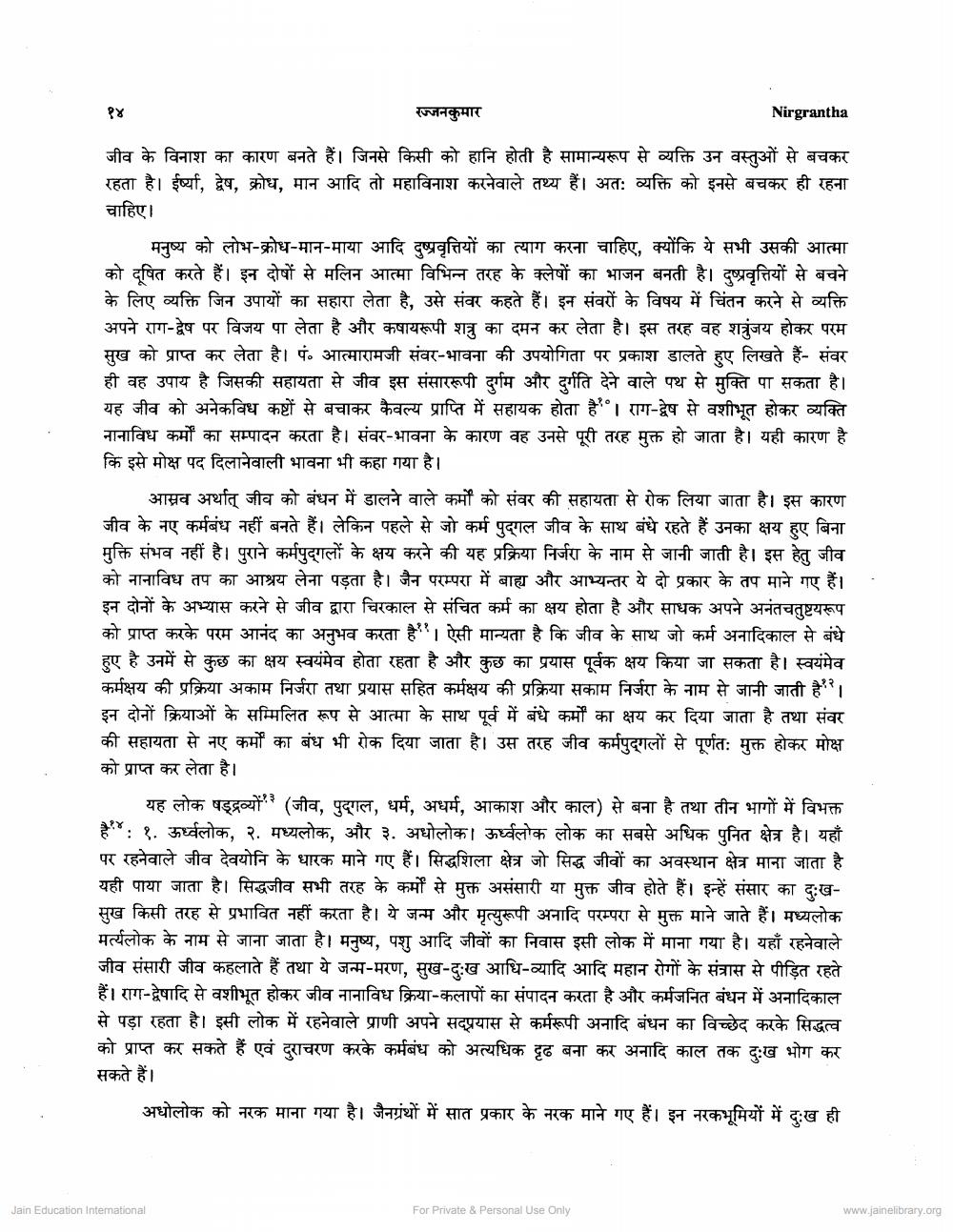________________
रज्जनकुमार
Nirgrantha
जीव के विनाश का कारण बनते हैं। जिनसे किसी को हानि होती है सामान्यरूप से व्यक्ति उन वस्तुओं से बचकर रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मान आदि तो महाविनाश करनेवाले तथ्य हैं। अत: व्यक्ति को इनसे बचकर ही रहना चाहिए।
मनुष्य को लोभ-क्रोध-मान-माया आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सभी उसकी आत्मा को दूषित करते हैं। इन दोषों से मलिन आत्मा विभिन्न तरह के क्लेषों का भाजन बनती है। दुष्प्रवृत्तियों से बचने के लिए व्यक्ति जिन उपायों का सहारा लेता है, उसे संवर कहते हैं। इन संवरों के विषय में चिंतन करने से व्यक्ति अपने राग-द्वेष पर विजय पा लेता है और कषायरूपी शत्रु का दमन कर लेता है। इस तरह वह शत्रुजय होकर परम सुख को प्राप्त कर लेता है। पं. आत्मारामजी संवर-भावना की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं- संवर ही वह उपाय है जिसकी सहायता से जीव इस संसाररूपी दुर्गम और दुर्गति देने वाले पथ से मुक्ति पा सकता है। यह जीव को अनेकविध कष्टों से बचाकर कैवल्य प्राप्ति में सहायक होता है। राग-द्वेष से वशीभूत होकर व्यक्ति नानाविध कर्मों का सम्पादन करता है। संवर-भावना के कारण वह उनसे पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे मोक्ष पद दिलानेवाली भावना भी कहा गया है।
आस्रव अर्थात् जीव को बंधन में डालने वाले कर्मों को संवर की सहायता से रोक लिया जाता है। इस कारण जीव के नए कर्मबंध नहीं बनते हैं। लेकिन पहले से जो कर्म पुद्गल जीव के साथ बंधे रहते हैं उनका क्षय हुए बिना मुक्ति संभव नहीं है। पुराने कर्मपुद्गलों के क्षय करने की यह प्रक्रिया निर्जरा के नाम से जानी जाती है। इस हेतु जीव को नानाविध तप का आश्रय लेना पड़ता है। जैन परम्परा में बाह्य और आभ्यन्तर ये दो प्रकार के तप माने गए हैं। . इन दोनों के अभ्यास करने से जीव द्वारा चिरकाल से संचित कर्म का क्षय होता है और साधक अपने अनंतचतुष्टयरूप को प्राप्त करके परम आनंद का अनुभव करता है। ऐसी मान्यता है कि जीव के साथ जो कर्म अनादिकाल से बंधे हुए है उनमें से कुछ का क्षय स्वयंमेव होता रहता है और कुछ का प्रयास पूर्वक क्षय किया जा सकता है। स्वयंमेव कर्मक्षय की प्रक्रिया अकाम निर्जरा तथा प्रयास सहित कर्मक्षय की प्रक्रिया सकाम निर्जरा के नाम से जानी जाती है। इन दोनों क्रियाओं के सम्मिलित रूप से आत्मा के साथ पूर्व में बंधे कर्मों का क्षय कर दिया जाता है तथा संवर की सहायता से नए कर्मों का बंध भी रोक दिया जाता है। उस तरह जीव कर्मपुद्गलों से पूर्णत: मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
यह लोक षड्द्रव्यों (जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल) से बना है तथा तीन भागों में विभक्त हैं: १. ऊर्ध्वलोक, २. मध्यलोक, और ३. अधोलोक। ऊर्ध्वलोक लोक का सबसे अधिक पुनित क्षेत्र है। यहाँ पर रहनेवाले जीव देवयोनि के धारक माने गए हैं। सिद्धशिला क्षेत्र जो सिद्ध जीवों का अवस्थान क्षेत्र माना जाता है यही पाया जाता है। सिद्धजीव सभी तरह के कर्मों से मुक्त असंसारी या मुक्त जीव होते हैं। इन्हें संसार का दुःखसुख किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है। ये जन्म और मृत्युरूपी अनादि परम्परा से मुक्त माने जाते हैं। मध्यलोक मर्त्यलोक के नाम से जाना जाता है। मनुष्य, पशु आदि जीवों का निवास इसी लोक में माना गया है। यहाँ रहनेवाले जीव संसारी जीव कहलाते हैं तथा ये जन्म-मरण, सुख-दु:ख आधि-व्यादि आदि महान रोगों के संत्रास से पीड़ित रहते हैं। राग-द्वेषादि से वशीभूत होकर जीव नानाविध क्रिया-कलापों का संपादन करता है और कर्मजनित बंधन में अनादिकाल से पड़ा रहता है। इसी लोक में रहनेवाले प्राणी अपने सद्प्रयास से कर्मरूपी अनादि बंधन का विच्छेद करके सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं एवं दुराचरण करके कर्मबंध को अत्यधिक दृढ बना कर अनादि काल तक दुःख भोग कर सकते हैं।
अधोलोक को नरक माना गया है। जैनग्रंथों में सात प्रकार के नरक माने गए हैं। इन नरकभूमियों में दुःख ही
Jain Education Intemational
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org