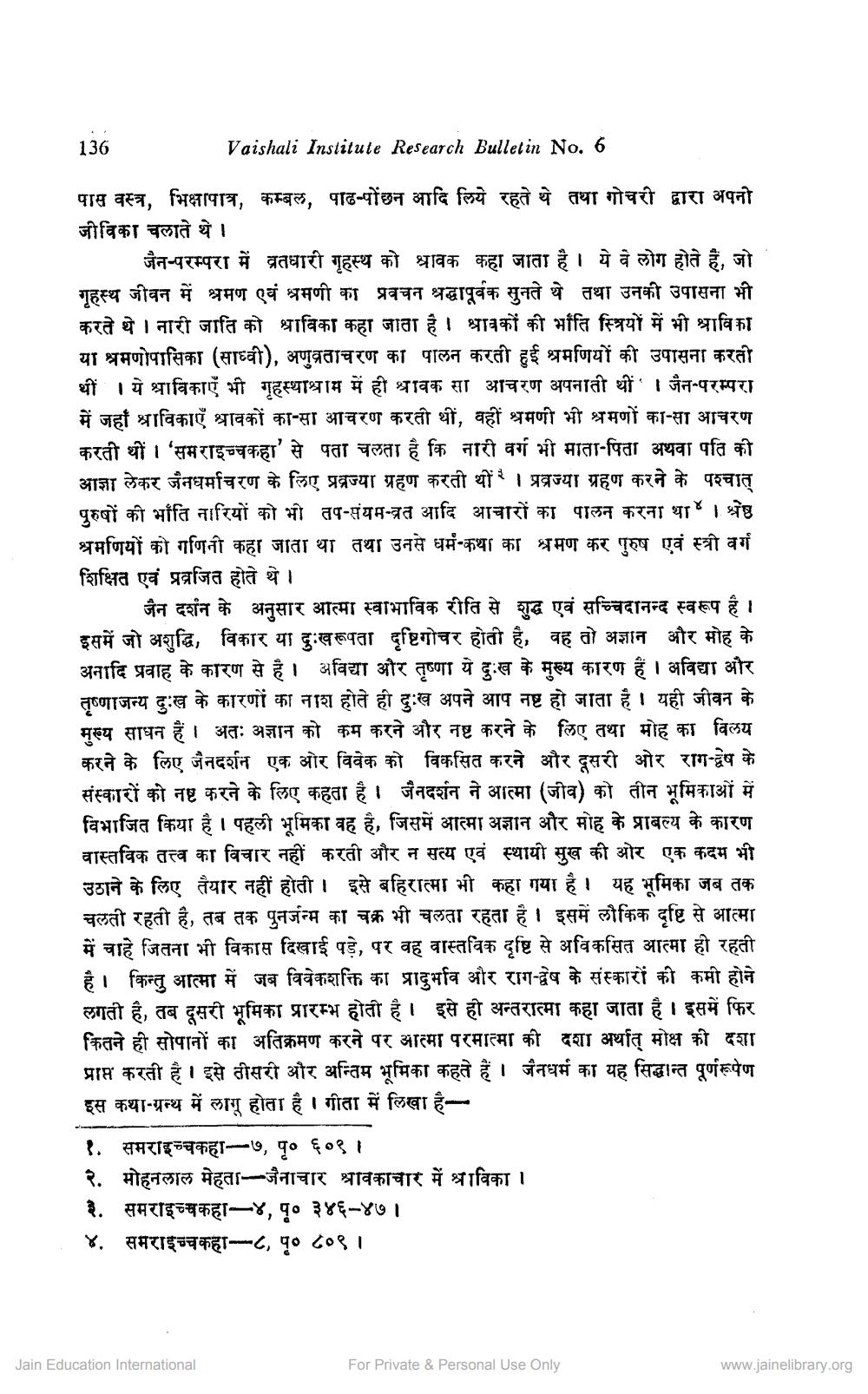________________
136
Vaishali Institute Research Bulletin No. 6
पास वस्त्र, भिक्षापात्र, कम्बल, पाढ-पोंछन आदि लिये रहते थे तथा गोचरी द्वारा अपनी जीविका चलाते थे।
जैन-परम्परा में व्रतधारी गृहस्थ को श्रावक कहा जाता है। ये वे लोग होते हैं, जो गृहस्थ जीवन में श्रमण एवं श्रमणी का प्रवचन श्रद्धापूर्वक सुनते थे तथा उनकी उपासना भी करते थे । नारी जाति को श्राविका कहा जाता है। श्रावकों की भांति स्त्रियों में भी श्राविका या श्रमणोपासिका (साध्वी), अणुव्रताचरण का पालन करती हुई श्रमणियों की उपासना करती थीं । ये श्राविकाएँ भी गृहस्थाश्राम में ही श्रावक सा आचरण अपनाती थीं । जैन-परम्परा में जहाँ श्राविकाएँ श्रावकों का-सा आचरण करती थीं, वहीं श्रमणी भी श्रमणों का-सा आचरण करती थीं। 'समराइच्चकहा' से पता चलता है कि नारी वर्ग भी माता-पिता अथवा पति की आज्ञा लेकर जैनधर्माचरण के लिए प्रव्रज्या ग्रहण करती थीं । प्रव्रज्या ग्रहण करने के पश्चात् पुरुषों की भाँति नारियों को भी तप-संयम-व्रत आदि आचारों का पालन करना था । श्रेष्ठ श्रमणियों को गणिनी कहा जाता था तथा उनसे धर्म-कथा का श्रमण कर पुरुष एवं स्त्री वर्ग शिक्षित एवं प्रवजित होते थे।।
जैन दर्शन के अनुसार आत्मा स्वाभाविक रीति से शुद्ध एवं सच्चिदानन्द स्वरूप है । इसमें जो अशुद्धि, विकार या दुःखरूपता दृष्टिगोचर होती है, वह तो अज्ञान और मोह के अनादि प्रवाह के कारण से है। अविद्या और तृष्णा ये दुःख के मुख्य कारण हैं । अविद्या और तृष्णाजन्य दुःख के कारणों का नाश होते ही दुःख अपने आप नष्ट हो जाता है । यही जीवन के मुख्य साधन हैं। अतः अज्ञान को कम करने और नष्ट करने के लिए तथा मोह का विलय करने के लिए जैनदर्शन एक ओर विवेक को विकसित करने और दूसरी ओर राग-द्वेष के संस्कारों को नष्ट करने के लिए कहता है । जैनदर्शन ने आत्मा (जीव) को तीन भूमिकाओं में विभाजित किया है । पहली भूमिका वह है, जिसमें आत्मा अज्ञान और मोह के प्राबल्य के कारण वास्तविक तत्त्व का विचार नहीं करती और न सत्य एवं स्थायी सूख की ओर एक कदम भी उठाने के लिए तैयार नहीं होती। इसे बहिरात्मा भी कहा गया है। यह भूमिका जब तक चलती रहती है, तब तक पुनर्जन्म का चक्र भी चलता रहता है। इसमें लौकिक दृष्टि से आत्मा में चाहे जितना भी विकास दिखाई पड़े, पर वह वास्तविक दृष्टि से अविकसित आत्मा ही रहती है। किन्तु आत्मा में जब विवेकशक्ति का प्रादुर्भाव और राग-द्वेष के संस्कारों की कमी होने लगती है, तब दूसरी भूमिका प्रारम्भ होती है। इसे ही अन्तरात्मा कहा जाता है । इसमें फिर कितने ही सोपानों का अतिक्रमण करने पर आत्मा परमात्मा की दशा अर्थात् मोक्ष की दशा प्राप्त करती है । इसे तीसरी और अन्तिम भूमिका कहते हैं। जैनधर्म का यह सिद्धान्त पूर्णरूपेण इस कथा-ग्रन्थ में लागू होता है । गीता में लिखा है१. समराइच्चकहा-७, पृ० ६०९ । २. मोहनलाल मेहता-जैनाचार श्रावकाचार में श्राविका । ३. समराइच्चकहा-४, पृ० ३४६-४७ । ४. समराइच्चकहा-८, पृ० ८०९ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org