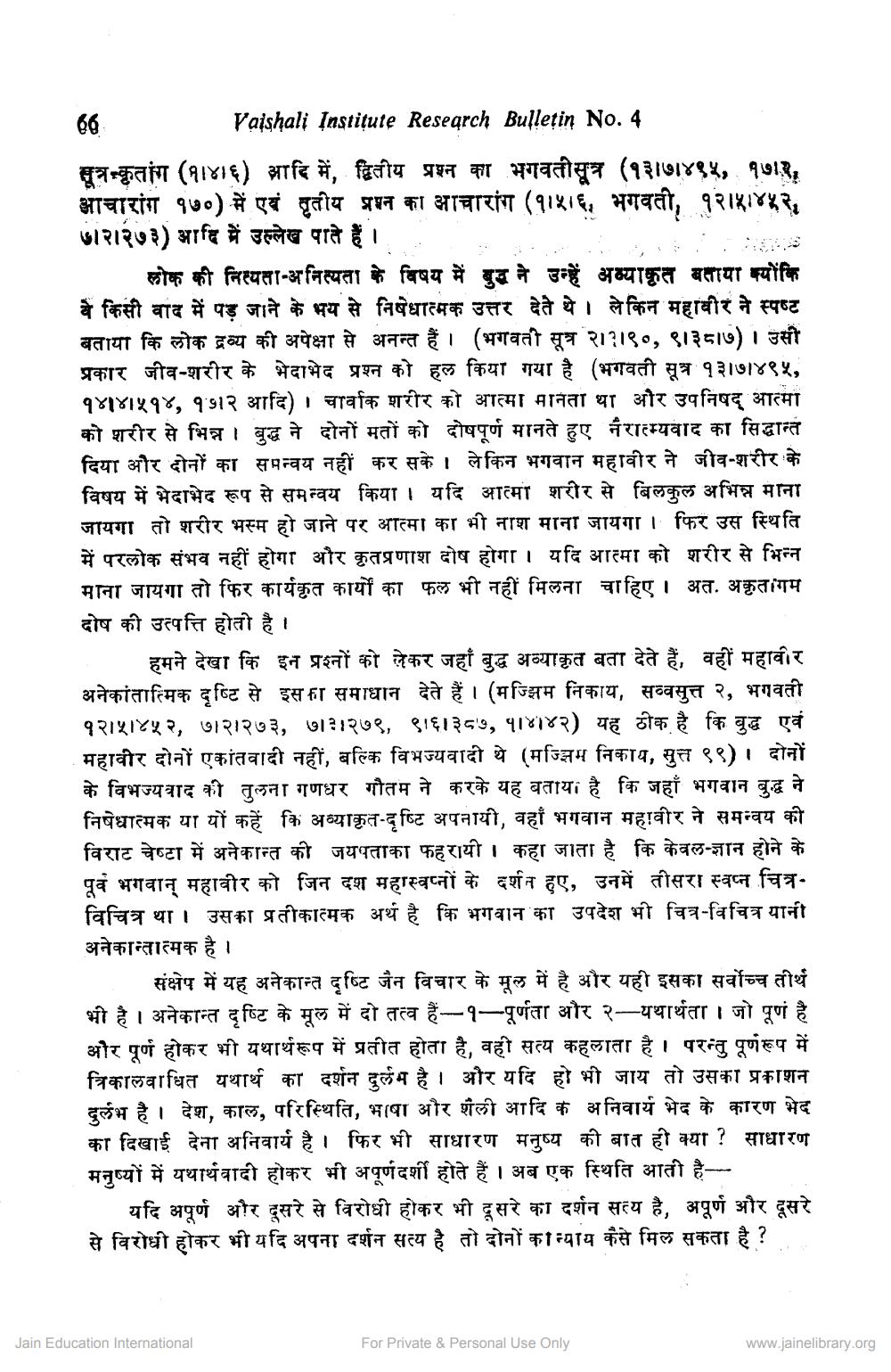________________
66
Vaishali Institute Research Bulletin No. 4
सूत्र - कृतांग (१।४।६) आदि में, द्वितीय प्रश्न का भगवतीसूत्र (१३/७/४९५, १७१२ आचारांग १७० ) में एवं तृतीय प्रश्न का आचारांग (१।५।६, भगवती १२५/४५२० ७।२।२७३) आदि में उल्लेख पाते हैं ।
A
लोक की freeता अनित्यता के विषय में बुद्ध ने उन्हें अव्याकृत बताया क्योंकि वे किसी वाद में पड़ जाने के भय से निषेधात्मक उत्तर देते थे। लेकिन महावीर ने स्पष्ट बताया कि लोक द्रव्य की अपेक्षा से अनन्त हैं । ( भगवती सूत्र २।३।९०, ९ ३ ८ ७) । उसी प्रकार जीव- शरीर के भेदाभेद प्रश्न को हल किया गया है ( भगवती सूत्र १३।७।४९५, १४।४।५१४, १७।२ आदि) । चार्वाक शरीर को आत्मा मानता था और उपनिषद् आत्मा को शरीर से भिन्न । बुद्ध ने दोनों मतों को दोषपूर्ण मानते हुए नैरात्म्यवाद का सिद्धान्तं दिया और दोनों का समन्वय नहीं कर सके । लेकिन भगवान महावीर ने जीव-शरीर के विषय में भेदाभेद रूप से समन्वय किया । यदि आत्मा शरीर से बिलकुल अभिन्न माना जायगा तो शरीर भस्म हो जाने पर आत्मा का भी नाश माना जायगा । फिर उस स्थिति में परलोक संभव नहीं होगा और कृतप्रणाश दोष होगा । यदि आत्मा को माना जायगा तो फिर कार्यकृत कार्यों का फल भी नहीं मिलना चाहिए । दोष की उत्पत्ति होती है ।
हमने देखा कि इन प्रश्नों को लेकर जहाँ बुद्ध अव्याकृत बता देते हैं, वहीं महावीर अनेकांतात्मक दृष्टि से इसका समाधान देते हैं । ( मज्झिमनिकाय, सव्वसुत्त २, भगवती १२।५।४५२, ७।२।२७३, ७३२७९, ९।६।३८७, १।४।४२ ) यह ठीक है कि बुद्ध एवं महावीर दोनों एकांतवादी नहीं, बल्कि विभज्यवादी थे (मज्झिम निकाय, सुत्त ९९ ) । दोनों के विभज्यवाद की तुलना गणधर गौतम ने करके यह बताया है कि जहाँ भगवान बुद्ध ने निषेधात्मक या यों कहें कि अव्याकृत दृष्टि अपनायी, वहाँ भगवान महावीर ने समन्वय की विराट चेष्टा में अनेकान्त की जयपताका फहरायी । कहा जाता है कि केवल ज्ञान होने के पूर्व भगवान् महावीर को जिन दश महास्वप्नों के दर्शन हुए, उनमें तीसरा स्वप्न चित्रविचित्र था । उसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि भगवान का उपदेश भी चित्र विचित्र यानी अनेकान्तात्मक है ।
शरीर से भिन्न अत अकृतागम
संक्षेप में यह अनेकान्त दृष्टि जैन विचार के मूल है और यही इसका सर्वोच्च तीर्थं भी है । अनेकान्त दृष्टि के मूल में दो तत्व हैं - १ - पूर्णता और २ – यथार्थता । जो पूर्ण है और पूर्ण होकर भी यथार्थरूप में प्रतीत होता है, वही सत्य कहलाता है । परन्तु पूर्णरुप में त्रिकालबाधित यथार्थ का दर्शन दुर्लभ है । और यदि हो भी जाय तो उसका प्रकाशन दुर्लभ है । देश, काल, परिस्थिति, भाषा और शैली आदि क अनिवार्य भेद के कारण भेद का दिखाई देना अनिवार्य है । फिर भी साधारण मनुष्य की बात ही क्या ? साधारण मनुष्यों में यथार्थवादी होकर भी अपूर्णदर्शी होते हैं । अब एक स्थिति आती है-
यदि अपूर्ण और दूसरे से विरोधी होकर भी दूसरे का दर्शन सत्य है, अपूर्ण और दूसरे से विरोधी होकर भी यदि अपना दर्शन सत्य है तो दोनों का न्याय कैसे मिल सकता है ?
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org