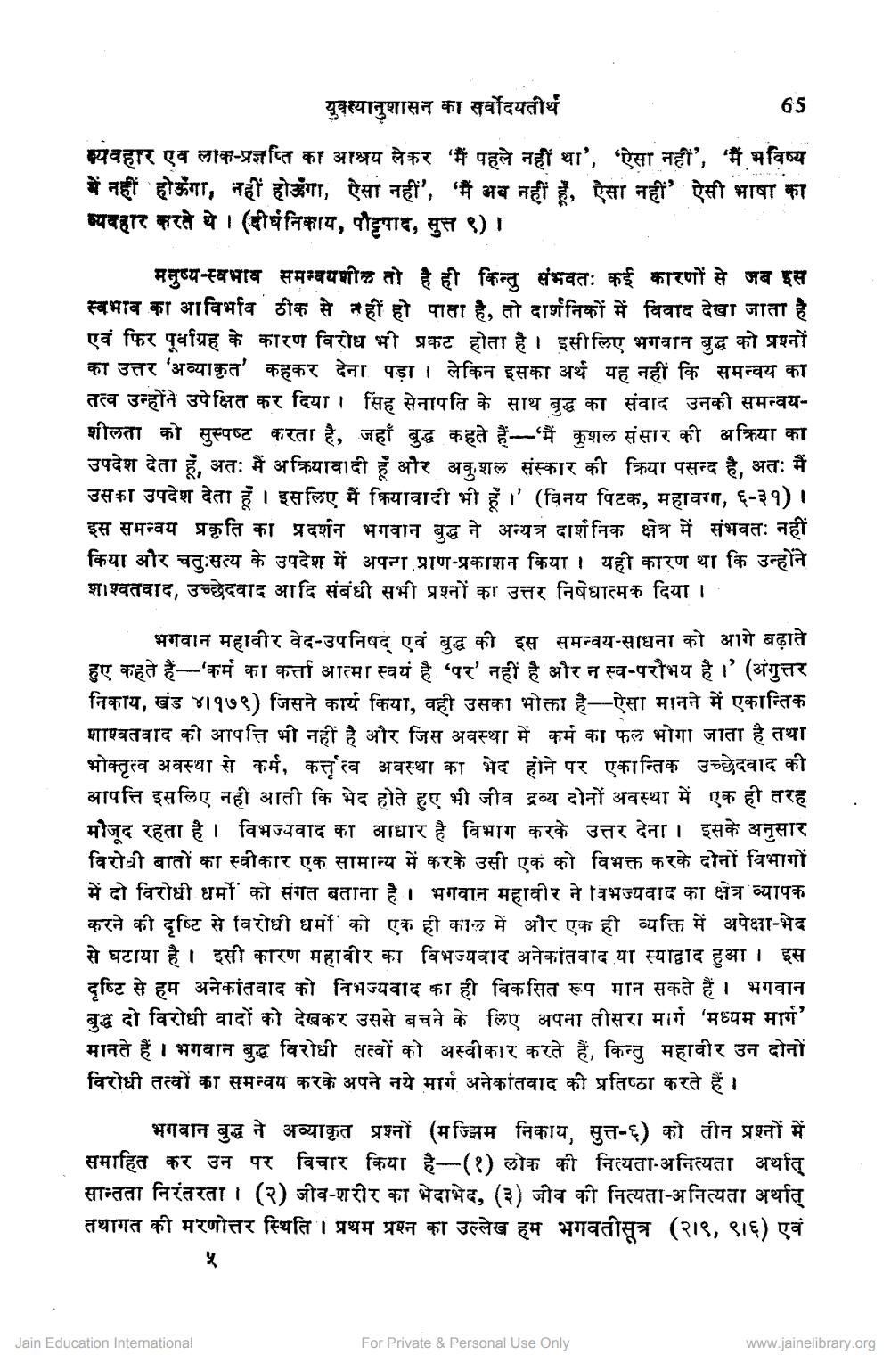________________
65
युक्त्यानुशासन का सर्वोदयतीर्थ व्यवहार एव लाक-प्रज्ञप्ति का आश्रय लेकर 'मैं पहले नहीं था', 'ऐसा नहीं', 'मैं भविष्य में नहीं होऊँगा, नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं', 'मैं अब नहीं हूँ, ऐसा नहीं' ऐसी भाषा का व्यवहार करते थे । (दीर्घनिकाय, पोट्टपाद, सुत्त ९)।
मनुष्य-स्वभाव समन्वयशील तो है ही किन्तु संभवतः कई कारणों से अब इस स्वभाव का आविर्भाव ठीक से नहीं हो पाता है, तो दार्शनिकों में विवाद देखा जाता है एवं फिर पूर्वाग्रह के कारण विरोध भी प्रकट होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध को प्रश्नों का उत्तर 'अव्याकृत' कहकर देना पड़ा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि समन्वय का तत्व उन्होंने उपेक्षित कर दिया। सिंह सेनापति के साथ बुद्ध का संवाद उनकी समन्वयशीलता को सुस्पष्ट करता है, जहाँ बुद्ध कहते हैं-'मैं कुशल संसार की अक्रिया का उपदेश देता हूँ, अतः मैं अक्रियावादी हूँ और अकुशल संस्कार की क्रिया पसन्द है, अतः मैं उसका उपदेश देता हूँ। इसलिए मैं क्रियावादी भी हूँ।' (विनय पिटक, महावग्ग, ६-३१)। इस समन्वय प्रकृति का प्रदर्शन भगवान बुद्ध ने अन्यत्र दार्शनिक क्षेत्र में संभवतः नहीं किया और चतुःसत्य के उपदेश में अपना प्राण-प्रकाशन किया। यही कारण था कि उन्होंने शाश्वतवाद, उच्छेदवाद आदि संबंधी सभी प्रश्नों का उत्तर निषेधात्मक दिया ।
भगवान महावीर वेद-उपनिषद् एवं बुद्ध की इस समन्वय-साधना को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं-'कर्म का कर्ता आत्मा स्वयं है 'पर' नहीं है और न स्व-परौभय है।' (अंगुत्तर निकाय, खंड ४।१७९) जिसने कार्य किया, वही उसका भोक्ता है-ऐसा मानने में एकान्तिक शाश्वतवाद की आपत्ति भी नहीं है और जिस अवस्था में कर्म का फल भोगा जाता है तथा भोक्तृत्व अवस्था से कर्म, कर्तृत्व अवस्था का भेद होने पर एकान्तिक उच्छेदवाद की आपत्ति इसलिए नहीं आती कि भेद होते हुए भी जीव द्रव्य दोनों अवस्था में एक ही तरह मौजूद रहता है। विभज्यवाद का आधार है विभाग करके उत्तर देना। इसके अनुसार विरोधी बातों का स्वीकार एक सामान्य में करके उसी एक को विभक्त करके दोनों विभागों में दो विरोधी धर्मो को संगत बताना है। भगवान महावीर ने विभज्यवाद का क्षेत्र व्यापक करने की दृष्टि से विरोधी धर्मों को एक ही काल में और एक ही व्यक्ति में अपेक्षा-भेद से घटाया है। इसी कारण महावीर का विभज्यवाद अनेकांतवाद या स्याद्वाद हुआ। इस दृष्टि से हम अनेकांतवाद को विभज्यवाद का ही विकसित रूप मान सकते हैं। भगवान बुद्ध दो विरोधी वादों को देखकर उससे बचने के लिए अपना तीसरा मार्ग 'मध्यम मार्ग' मानते हैं । भगवान बुद्ध विरोधी तत्वों को अस्वीकार करते हैं, किन्तु महावीर उन दोनों विरोधी तत्वों का समन्वय करके अपने नये मार्ग अनेकांतवाद की प्रतिष्ठा करते हैं।
भगवान बुद्ध ने अव्याकृत प्रश्नों (मज्झिम निकाय, सुत्त-६) को तीन प्रश्नों में समाहित कर उन पर विचार किया है--(१) लोक की नित्यता-अनित्यता अर्थात् सान्तता निरंतरता । (२) जीव-शरीर का भेदाभेद, (३) जीव की नित्यता-अनित्यता अर्थात् तथागत की मरणोत्तर स्थिति । प्रथम प्रश्न का उल्लेख हम भगवतीसूत्र (२।९, ९।६) एवं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org