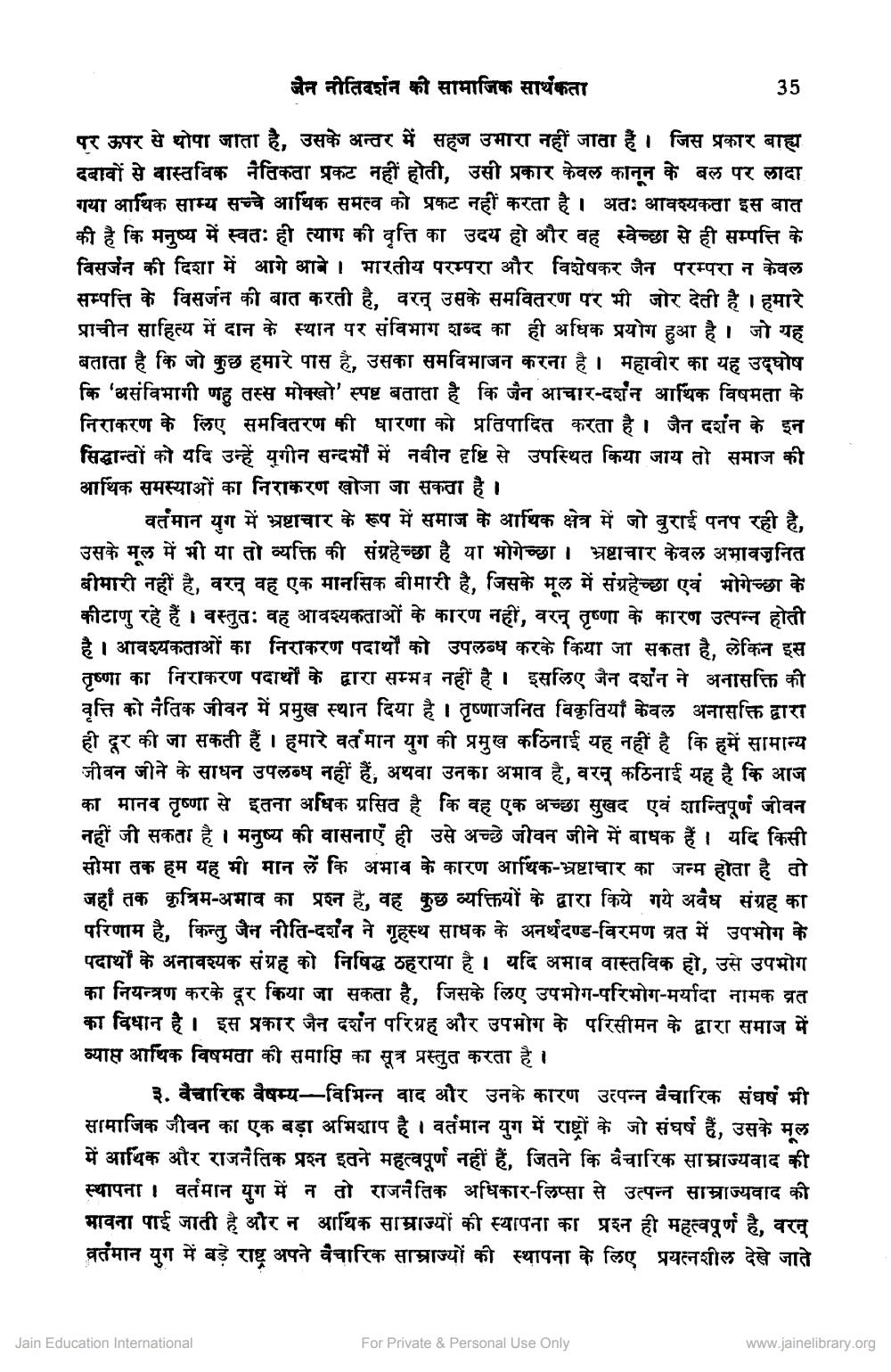________________
जैन नीतिदर्शन को सामाजिक सार्थकता
पर ऊपर थोपा जाता है, उसके अन्तर में सहज उमारा नहीं जाता हैं । जिस प्रकार बाह्य दबावों से वास्तविक नैतिकता प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार केवल कानून के बल पर लादा या आर्थिक साम्य सच्चे आर्थिक समत्व को प्रकट नहीं करता है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य में स्वतः ही त्याग की वृत्ति का उदय हो और वह स्वेच्छा से ही सम्पत्ति के विसर्जन की दिशा में आगे आने । भारतीय परम्परा और विशेषकर जैन परम्परा न केवल सम्पत्ति के विसर्जन की बात करती है, वरन् उसके समवितरण पर भी जोर देती है । हमारे प्राचीन साहित्य में दान के स्थान पर संविभाग शब्द का ही अधिक प्रयोग हुआ है । जो यह बताता है कि जो कुछ हमारे पास है, उसका समविभाजन करना है । महावीर का यह उद्घोष कि 'असंविभागी हु तस्स मोक्खो' स्पष्ट बताता है कि जैन आचार-दर्शन आर्थिक विषमता के निराकरण के लिए समवितरण की धारणा को प्रतिपादित करता है। जैन दर्शन के इन सिद्धान्तों को यदि उन्हें युगीन सन्दर्भों में नवीन दृष्टि से उपस्थित किया जाय तो समाज की afra समस्याओं का निराकरण खोजा जा सकता है ।
वर्तमान युग में भ्रष्टाचार के रूप में समाज के आर्थिक क्षेत्र में जो बुराई पनप रही है, उसके मूल में भी या तो व्यक्ति की संग्रहेच्छा है या भोगेच्छा । भ्रष्टाचार केवल अभावज्रनित बीमारी नहीं है, वरन् वह एक मानसिक बीमारी है, जिसके मूल में संग्रहेच्छा एवं भोगेच्छा के कीटाणु रहे हैं । वस्तुतः वह आवश्यकताओं के कारण नहीं, वरन् तृष्णा के कारण उत्पन्न होती है । आवश्यकताओं का निराकरण पदार्थों को उपलब्ध करके किया जा सकता है, लेकिन इस तृष्णा का निराकरण पदार्थों के द्वारा सम्भव नहीं है । इसलिए जैन दर्शन ने अनासक्ति की वृत्ति को नैतिक जीवन में प्रमुख स्थान दिया है । तृष्णाजनित विकृतियाँ केवल अनासक्ति द्वारा ही दूर की जा सकती हैं। हमारे वर्तमान युग की प्रमुख कठिनाई यह नहीं है कि हमें सामान्य जीवन जीने के साधन उपलब्ध नहीं हैं, अथवा उनका अभाव है, वरन् कठिनाई यह है कि आज का मानव तृष्णा से इतना अधिक ग्रसित है कि वह एक अच्छा सुखद एवं शान्तिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता है | मनुष्य की वासनाएँ ही उसे अच्छे जीवन जीने में बाधक हैं। यदि किसी सीमा तक हम यह भी मान लें कि अभाव के कारण आर्थिक भ्रष्टाचार का जन्म होता है तो जहाँ तक कृत्रिम अभाव का प्रश्न है, वह कुछ व्यक्तियों के द्वारा किये गये अवैध संग्रह का परिणाम है, किन्तु जैन नीति- दर्शन ने गृहस्थ साधक के अनर्थदण्ड - विरमण व्रत में उपभोग के पदार्थों के अनावश्यक संग्रह को निषिद्ध ठहराया है । यदि अभाव वास्तविक हो, उसे उपभोग का नियन्त्रण करके दूर किया जा सकता है, जिसके लिए उपभोग - परिभोग-मर्यादा नामक व्रत का विधान है। इस प्रकार जैन दर्शन परिग्रह और उपभोग के परिसीमन के द्वारा समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता की समाप्ति का सूत्र प्रस्तुत करता है ।
35
३. वैचारिक वैषम्य - विभिन्न वाद और उनके कारण उत्पन्न वैचारिक संघर्ष भी सामाजिक जीवन का एक बड़ा अभिशाप है । वर्तमान युग में राष्ट्रों के जो संघर्ष हैं, उसके मूल में आर्थिक और राजनैतिक प्रश्न इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जितने कि वैचारिक साम्राज्यवाद की स्थापना । वर्तमान युग में न तो राजनैतिक अधिकार - लिप्सा से उत्पन्न साम्राज्यवाद की भावना पाई जाती है और न आर्थिक साम्राज्यों की स्थापना का प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, वरन् वर्तमान युग में बड़े राष्ट्र अपने वैचारिक साम्राज्यों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील देखे जाते
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org