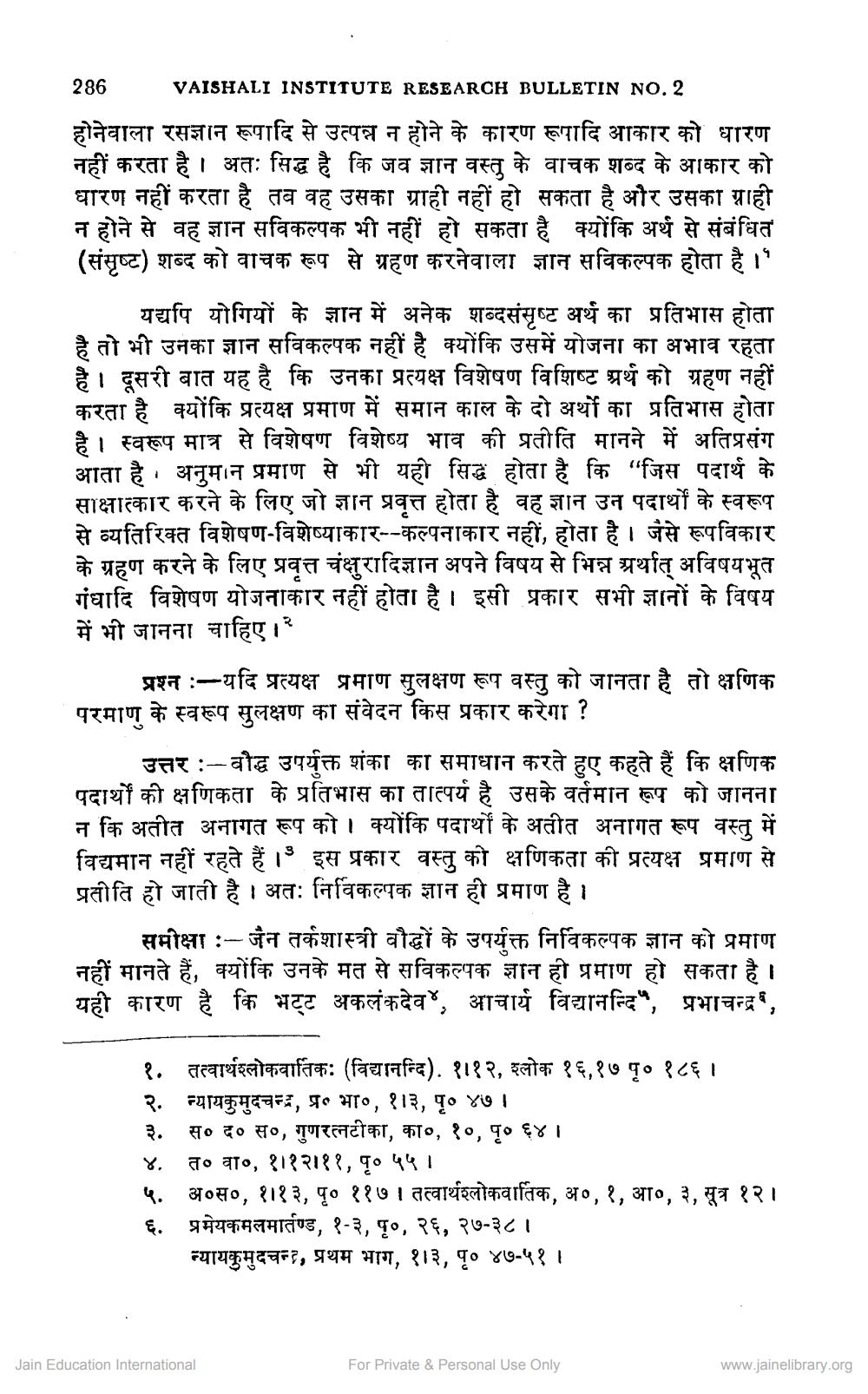________________
286 VAISHALI INSTITUTE RESEARCH BULLETIN NO. 2 होनेवाला रसज्ञान रूपादि से उत्पन्न न होने के कारण रूपादि आकार को धारण नहीं करता है। अतः सिद्ध है कि जव ज्ञान वस्तु के वाचक शब्द के आकार को धारण नहीं करता है तब वह उसका ग्राही नहीं हो सकता है और उसका नाही न होने से वह ज्ञान सविकल्पक भी नहीं हो सकता है क्योंकि अर्थ से संबंधित (संसृष्ट) शब्द को वाचक रूप से ग्रहण करनेवाला ज्ञान सविकल्पक होता है।
यद्यपि योगियों के ज्ञान में अनेक शब्दसंसृष्ट अर्थ का प्रतिभास होता है तो भी उनका ज्ञान सविकल्पक नहीं है क्योंकि उसमें योजना का अभाव रहता है। दूसरी बात यह है कि उनका प्रत्यक्ष विशेषण विशिष्ट अर्थ को ग्रहण नहीं करता है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में समान काल के दो अर्थों का प्रतिभास होता है। स्वरूप मात्र से विशेषण विशेष्य भाव की प्रतीति मानने में अतिप्रसंग आता है। अनुमान प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि "जिस पदार्थ के साक्षात्कार करने के लिए जो ज्ञान प्रवृत्त होता है वह ज्ञान उन पदार्थों के स्वरूप से व्यतिरिक्त विशेषण-विशेष्याकार--कल्पनाकार नहीं, होता है। जैसे रूपविकार के ग्रहण करने के लिए प्रवत्त चंक्षुरादिज्ञान अपने विषय से भिन्न अर्थात् अविषयभूत गंधादि विशेषण योजनाकार नहीं होता है। इसी प्रकार सभी ज्ञानों के विषय में भी जानना चाहिए।
प्रश्न :-यदि प्रत्यक्ष प्रमाण सुलक्षण रूप वस्तु को जानता है तो क्षणिक परमाणु के स्वरूप सुलक्षण का संवेदन किस प्रकार करेगा?
उत्तर :-बौद्ध उपर्युक्त शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि क्षणिक पदार्थों की क्षणिकता के प्रतिभास का तात्पर्य है उसके वर्तमान रूप को जानना न कि अतीत अनागत रूप को। क्योंकि पदार्थों के अतीत अनागत रूप वस्तु में विद्यमान नहीं रहते हैं। इस प्रकार वस्तु को क्षणिकता की प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतीति हो जाती है । अत: निर्विकल्पक ज्ञान ही प्रमाण है।
समीक्षा :- जैन तर्कशास्त्री वौद्धों के उपर्युक्त निर्विकल्पक ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके मत से सविकल्पक ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है। यही कारण है कि भट्ट अकलंकदेव, आचार्य विद्यानन्दि", प्रभाचन्द्र,
१. तत्वार्थश्लोकवार्तिकः (विद्यानन्दि). १३१२, श्लोक १६,१७ पृ० १८६ । २. न्यायकुमुदचन्द्र, प्र. भा०, ११३, पृ० ४७ । ३. स० द० स०, गुणरत्नटीका, का०, १०, पृ० ६४ । ४. त० वा०, १।१२।११, पृ० ५५ । ५. अ०स०, १११३, पृ० ११७ । तत्वार्थश्लोकवार्तिक, अ०, १, आ०, ३, सूत्र १२ ।
प्रमेयकमलमार्तण्ड, १-३, पृ०, २६, २७-३८ । न्यायकुमुदचन्द्र, प्रथम भाग, ११३, पृ० ४७-५१ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org