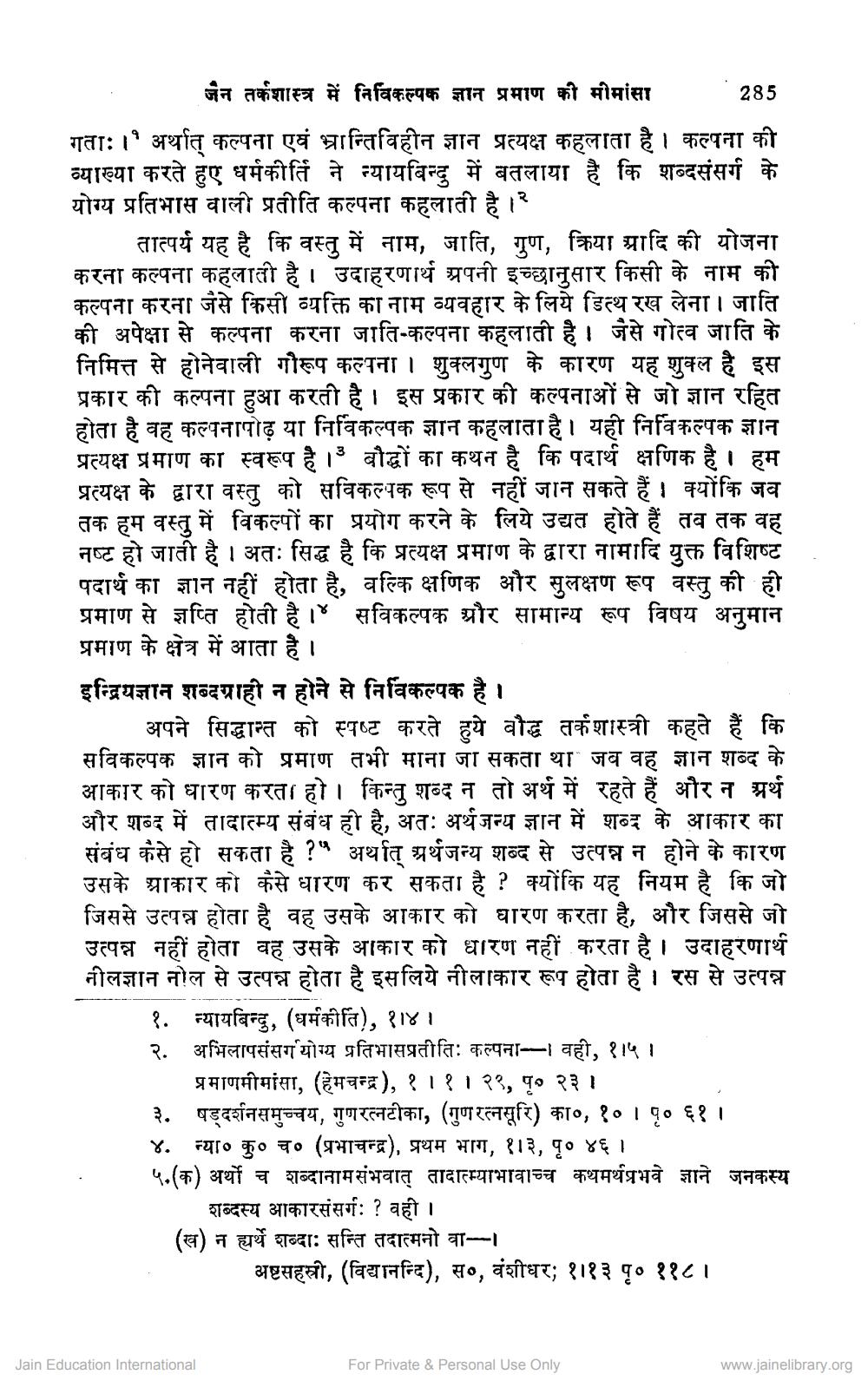________________
जैन तर्कशास्त्र में निर्विकल्पक ज्ञान प्रमाण की मीमांसा
285
गताः ।' अर्थात् कल्पना एवं भ्रान्तिविहीन ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है । कल्पना की व्याख्या करते हुए धर्मकीर्ति ने न्यायबिन्दु में बतलाया है कि शब्दसंसर्ग के योग्य प्रतिभास वाली प्रतीति कल्पना कहलाती है । 2
तात्पर्य यह है कि वस्तु में नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि की योजना करना कल्पना कहलाती है । उदाहरणार्थ अपनी इच्छानुसार किसी के नाम की कल्पना करना जैसे किसी व्यक्ति का नाम व्यवहार के लिये डित्थ रख लेना । जाति की अपेक्षा से कल्पना करना जाति कल्पना कहलाती है । जैसे गोत्व जाति के निमित्त से होनेवाली गौरूप कल्पना । शुक्लगुण के कारण यह शुक्ल है इस प्रकार की कल्पना हुआ करती है। इस प्रकार की कल्पनाओं से जो ज्ञान रहित होता है वह कल्पनापोढ़ या निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है । यही निर्विकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप है । 3 बौद्धों का कथन है कि पदार्थ क्षणिक है । हम प्रत्यक्ष के द्वारा वस्तु को सविकल्पक रूप से नहीं जान सकते हैं। क्योंकि जव तक हम वस्तु में विकल्पों का प्रयोग करने के लिये उद्यत होते हैं तब तक वह नष्ट हो जाती है | अतः सिद्ध है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नामादि युक्त विशिष्ट पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, वल्कि क्षणिक और सुलक्षण रूप वस्तु की ही प्रमाण से ज्ञप्ति होती है । सविकल्पक और सामान्य रूप विषय अनुमान प्रमाण के क्षेत्र में आता है ।
इन्द्रियज्ञान शब्दग्राही न होने से निर्विकल्पक है ।
अपने सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुये बौद्ध तर्कशास्त्री कहते हैं कि सविकल्पक ज्ञान को प्रमाण तभी माना जा सकता था जब वह ज्ञान शब्द के आकार को धारण करता हो । किन्तु शब्द न तो अर्थ में रहते हैं और न अर्थ और शब्द में तादात्म्य संबंध ही है, अतः अर्थजन्य ज्ञान में शब्द के आकार का संबंध कैसे हो सकता है ?" अर्थात् श्रर्थजन्य शब्द से उत्पन्न न होने के कारण उसके श्राकार को कैसे धारण कर सकता है ? क्योंकि यह नियम है कि जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसके आकार को धारण करता है, और जिससे जी उत्पन्न नहीं होता वह उसके आकार को धारण नहीं करता है । उदाहरणार्थ नीलज्ञान नोल से उत्पन्न होता है इसलिये नीलाकार रूप होता है । रस से उत्पन्न १. न्यायबिन्दु, (धर्मकीर्ति), ११४ ।
२.
अभिलापसंसर्ग योग्य प्रतिभासप्रतीतिः कल्पना -- । वही, ११५ ।
प्रमाणमीमांसा (हेमचन्द्र ), १ । १ । २१, पृ० २३ ॥
३. षड्दर्शनसमुच्चय, गुणरत्नटीका, (गुणरत्नसूरि) का०, १० । पृ० ६१ ।
४.
न्या० कु० च० ( प्रभाचन्द्र ), प्रथम भाग, १1३, पृ० ४६ ।
५. (क) अर्थो च शब्दानामसंभवात् तादात्म्याभावाच्च कथमर्थप्रभवे ज्ञाने जनकस्य
शब्दस्य आकारसंसर्गः ? वही ।
(ख) न ह्यर्थे शब्दाः सन्ति तदात्मनो वा --
Jain Education International
अष्टसहस्र (विद्यानन्द), स०, वंशीधर; १।१३ पृ० ११८ ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org