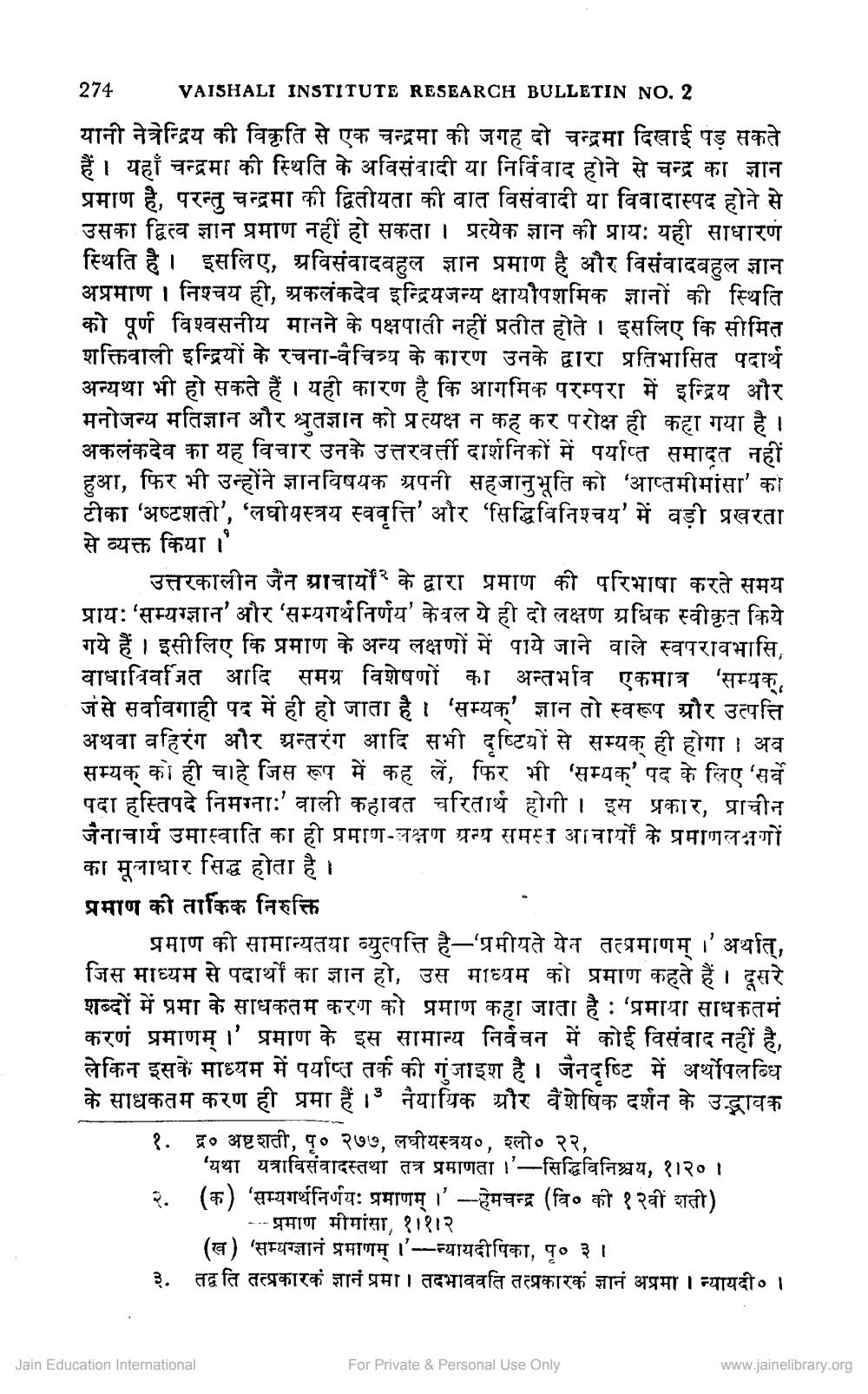________________
274 VAISHALI INSTITUTE RESEARCH BULLETIN NO. 2 यानी नेत्रेन्द्रिय की विकृति से एक चन्द्रमा की जगह दो चन्द्रमा दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ चन्द्रमा की स्थिति के अविसंवादी या निर्विवाद होने से चन्द्र का ज्ञान प्रमाण है, परन्तु चन्द्रमा की द्वितीयता की बात विसंवादी या विवादास्पद होने से उसका द्वित्व ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। प्रत्येक ज्ञान की प्रायः यही साधारण स्थिति है। इसलिए, अविसंवादबहुल ज्ञान प्रमाण है और विसंवादबहुल ज्ञान अप्रमाण । निश्चय ही, अकलंकदेव इन्द्रियजन्य क्षायौपशमिक ज्ञानों की स्थिति को पूर्ण विश्वसनीय मानने के पक्षपाती नहीं प्रतीत होते । इसलिए कि सीमित शक्तिवाली इन्द्रियों के रचना-वैचित्र्य के कारण उनके द्वारा प्रतिभासित पदार्थ अन्यथा भी हो सकते हैं । यही कारण है कि आगमिक परम्परा में इन्द्रिय और मनोजन्य मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को प्रत्यक्ष न कह कर परोक्ष ही कहा गया है। अकलंकदेव का यह विचार उनके उत्तरवर्ती दार्शनिकों में पर्याप्त समादत नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने ज्ञानविषयक अपनी सहजानुभूति को 'आप्तमीमांसा' का टीका 'अष्टशती', 'लघीयस्त्रय स्ववृत्ति' और 'सिद्धिविनिश्चय' में बड़ी प्रखरता से व्यक्त किया।
उत्तरकालीन जैन प्राचार्यों के द्वारा प्रमाण की परिभाषा करते समय प्रायः 'सम्यग्ज्ञान' और 'सम्यगर्थनिर्णय' केवल ये ही दो लक्षण अधिक स्वीकृत किये गये हैं। इसीलिए कि प्रमाण के अन्य लक्षणों में पाये जाने वाले स्वपरावभासि, वाधाविजित आदि समग्र विशेषणों का अन्तर्भाव एकमात्र 'सम्यक, जसे सर्वावगाही पद में ही हो जाता है । 'सम्यक् ज्ञान तो स्वरूप और उत्पत्ति अथवा बहिरंग और अन्तरंग आदि सभी दृष्टियों से सम्यक ही होगा। अव सम्यक् को ही चाहे जिस रूप में कह लें, फिर भी 'सम्यक्' पद के लिए 'सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्नाः' वाली कहावत चरितार्थ होगी। इस प्रकार, प्राचीन जैनाचार्य उमास्वाति का ही प्रमाण-लक्षण अन्य समस्त आचार्यों के प्रमाणलक्षणों का मूलाधार सिद्ध होता है। प्रमाण की ताकिक निरुक्ति
प्रमाण की सामान्यतया व्युत्पत्ति है-'प्रमीयते येन तत्प्रमाणम् ।' अर्थात्, जिस माध्यम से पदार्थों का ज्ञान हो, उस माध्यम को प्रमाण कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रमा के साधकतम करण को प्रमाण कहा जाता है : 'प्रमाया साधकतमं करणं प्रमाणम् ।' प्रमाण के इस सामान्य निर्वचन में कोई विसंवाद नहीं है, लेकिन इसके माध्यम में पर्याप्त तर्क की गुंजाइश है। जैनदृष्टि में अर्थोपलब्धि के साधकतम करण ही प्रमा हैं। नैयायिक और वैशेषिक दर्शन के उद्भावक
१. द्र० अष्ट शती, पृ० २७७, लघीयस्त्रय०, श्लो० २२,
__'यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता ।'-सिद्धिविनिश्चय, १।२० । २. (क) 'सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम् ।' – हेमचन्द्र (वि० की १२वीं शती)
-----प्रमाण मीमांसा, १११२ (ख) 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम् ।'-न्यायदीपिका, पृ० ३ । ३. तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं प्रमा। तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं अप्रमा। न्यायदी० ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org