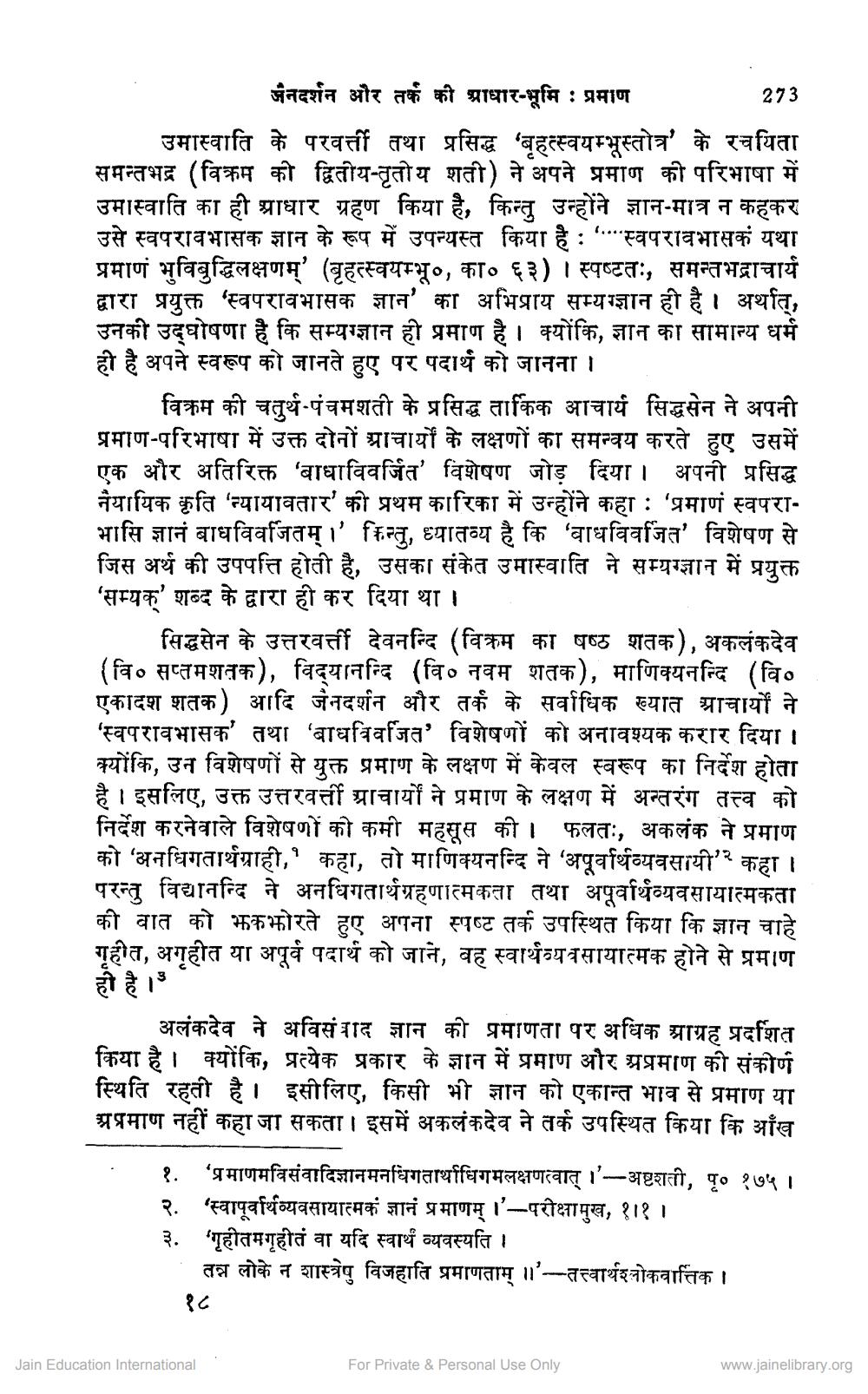________________
जनदर्शन और तर्क की आधार-भूमि : प्रमाण
273 उमास्वाति के परवर्ती तथा प्रसिद्ध 'बहत्स्वयम्भूस्तोत्र' के रचयिता समन्तभद्र (विक्रम को द्वितीय-तृतीय शती) ने अपने प्रमाण की परिभाषा में उमास्वाति का ही प्राधार ग्रहण किया है, किन्तु उन्होंने ज्ञान-मात्र न कहकर उसे स्वपरावभासक ज्ञान के रूप में उपन्यस्त किया है : .."स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुविबुद्धिलक्षणम्' (बृहत्स्वयम्भू०, का०६३) । स्पष्टतः, समन्तभद्राचार्य द्वारा प्रयुक्त 'स्वपरावभासक ज्ञान' का अभिप्राय सम्यग्ज्ञान ही है। अर्थात्, उनकी उद्घोषणा है कि सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण है। क्योंकि, ज्ञान का सामान्य धर्म ही है अपने स्वरूप को जानते हुए पर पदार्थ को जानना।
विक्रम की चतुर्थ-पंचमशती के प्रसिद्ध तार्किक आचार्य सिद्धसेन ने अपनी प्रमाण-परिभाषा में उक्त दोनों प्राचार्यों के लक्षणों का समन्वय करते हुए उसमें एक और अतिरिक्त 'बाधाविवर्जित' विशेषण जोड़ दिया। अपनी प्रसिद्ध नैयायिक कृति 'न्यायावतार' की प्रथम कारिका में उन्होंने कहा : 'प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्।' किन्तु, ध्यातव्य है कि 'बाधविजित' विशेषण से जिस अर्थ की उपपत्ति होती है, उसका संकेत उमास्वाति ने सम्यग्ज्ञान में प्रयुक्त 'सम्यक्' शब्द के द्वारा ही कर दिया था।
सिद्धसेन के उत्तरवर्ती देवनन्दि (विक्रम का षष्ठ शतक), अकलंकदेव (वि० सप्तमशतक), विद्यानन्दि (वि० नवम शतक), माणिक्यनन्दि (वि० एकादश शतक) आदि जैनदर्शन और तर्क के सर्वाधिक ख्यात आचार्यों ने 'स्वपरावभासक' तथा 'बाधविजित' विशेषणों को अनावश्यक करार दिया। क्योंकि, उन विशेषणों से युक्त प्रमाण के लक्षण में केवल स्वरूप का निर्देश होता है। इसलिए, उक्त उत्तरवर्ती प्राचार्यों ने प्रमाण के लक्षण में अन्तरंग तत्त्व को निर्देश करनेवाले विशेषणों को कमी महसूस की। फलतः, अकलंक ने प्रमाण को 'अनधिगतार्थग्राही,' कहा, तो माणिक्यनन्दि ने 'अपूर्वार्थव्यवसायी कहा। परन्तु विद्यानन्दि ने अनधिगतार्थग्रहणात्मकता तथा अपूर्वार्थव्यवसायात्मकता की बात को झकझोरते हुए अपना स्पष्ट तर्क उपस्थित किया कि ज्ञान चाहे गृहीत, अगृहीत या अपूर्व पदार्थ को जाने, वह स्वार्थव्यवसायात्मक होने से प्रमाण
अलंकदेव ने अविसंवाद ज्ञान की प्रमाणता पर अधिक आग्रह प्रदर्शित किया है। क्योंकि, प्रत्येक प्रकार के ज्ञान में प्रमाण और अप्रमाण की संकीर्ण स्थिति रहती है। इसीलिए, किसी भी ज्ञान को एकान्त भाव से प्रमाण या अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। इसमें अकलंकदेव ने तर्क उपस्थित किया कि आँख
१. 'प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात् ।'-अष्टशती, पृ० १७५ । २. 'स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।'-परीक्षामुख, ११ । ३. 'गृहीतमगृहीतं वा यदि स्वार्थं व्यवस्यति । - तन्न लोके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम् ॥'-तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक । १८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org