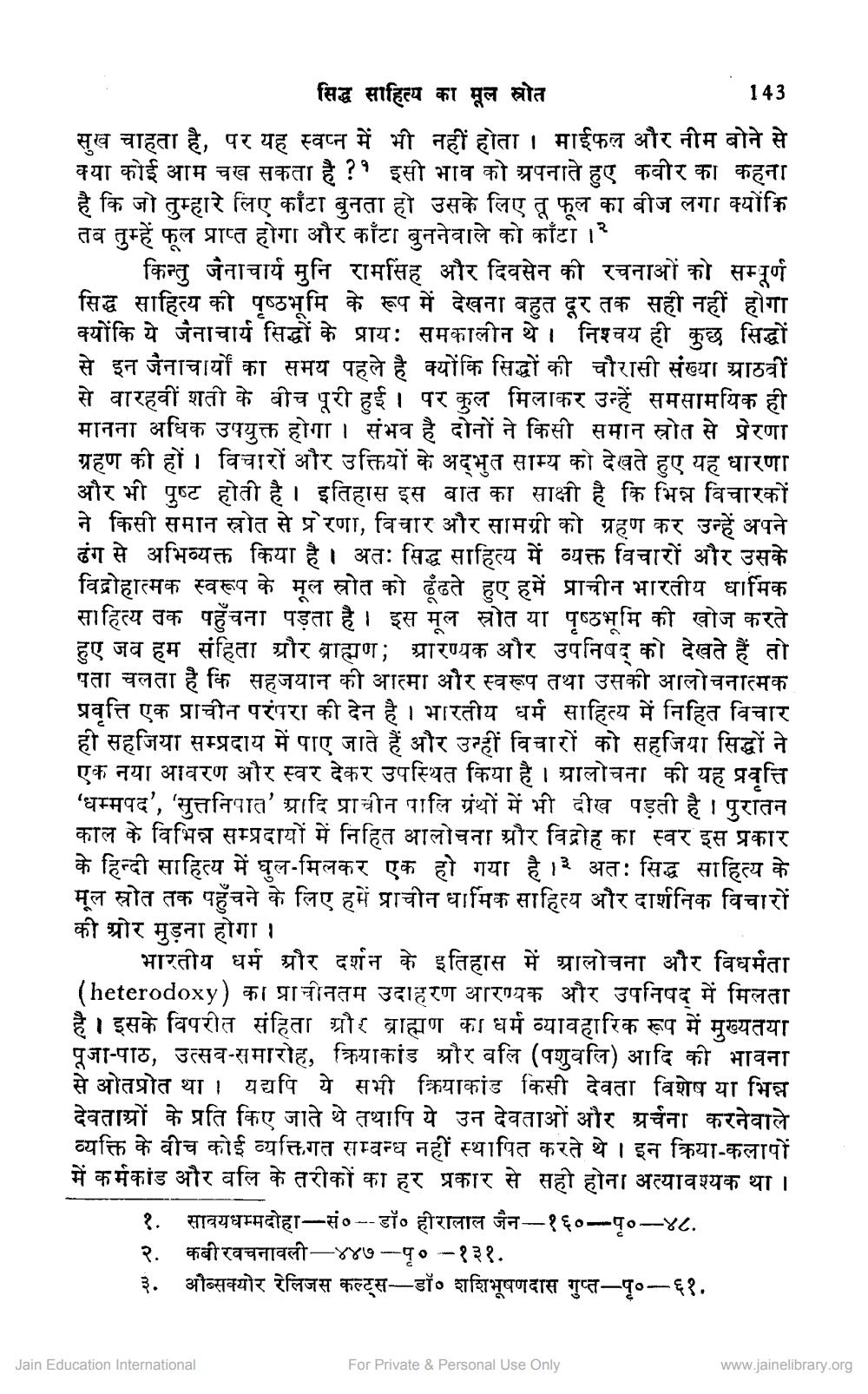________________
सिद्ध साहित्य का मूल स्रोत
__143 सुख चाहता है, पर यह स्वप्न में भी नहीं होता। माईफल और नीम बोने से क्या कोई आम चख सकता है ?' इसी भाव को अपनाते हुए कवीर का कहना है कि जो तुम्हारे लिए काँटा बुनता हो उसके लिए तू फूल का बीज लगा क्योंकि तब तुम्हें फूल प्राप्त होगा और काँटा बुननेवाले को काँटा ।
किन्तु जैनाचार्य मुनि रामसिंह और दिवसेन की रचनाओं को सम्पूर्ण सिद्ध साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में देखना बहुत दूर तक सही नहीं होगा क्योंकि ये जैनाचार्य सिद्धों के प्राय: समकालीन थे। निश्चय ही कुछ सिद्धों से इन जैनाचार्यों का समय पहले है क्योंकि सिद्धों की चौरासी संख्या आठवीं से वारहवीं शती के बीच पूरी हुई। पर कुल मिलाकर उन्हें समसामयिक ही मानना अधिक उपयुक्त होगा। संभव है दोनों ने किसी समान स्रोत से प्रेरणा ग्रहण की हों। विचारों और उक्तियों के अद्भुत साम्य को देखते हुए यह धारणा
और भी पुष्ट होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भिन्न विचारकों ने किसी समान स्रोत से प्रेरणा, विचार और सामग्री को ग्रहण कर उन्हें अपने ढंग से अभिव्यक्त किया है। अतः सिद्ध साहित्य में व्यक्त विचारों और उसके विद्रोहात्मक स्वरूप के मूल स्रोत को ढूंढते हुए हमें प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य तक पहुँचना पड़ता है। इस मूल स्रोत या पृष्ठभूमि की खोज करते हुए जब हम संहिता और ब्राह्मण; प्रारण्यक और उपनिषद् को देखते हैं तो पता चलता है कि सहजयान की आत्मा और स्वरूप तथा उसकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति एक प्राचीन परंपरा की देन है। भारतीय धर्म साहित्य में निहित विचार ही सहजिया सम्प्रदाय में पाए जाते हैं और उन्हीं विचारों को सहजिया सिद्धों ने एक नया आवरण और स्वर देकर उपस्थित किया है । अालोचना की यह प्रवृत्ति 'धम्मपद', 'सुत्तनिपात' प्रादि प्राचीन पालि ग्रंथों में भी दीख पड़ती है । पुरातन काल के विभिन्न सम्प्रदायों में निहित आलोचना और विद्रोह का स्वर इस प्रकार के हिन्दी साहित्य में घुल-मिलकर एक हो गया है।३ अत : सिद्ध साहित्य के मूल स्रोत तक पहुँचने के लिए हमें प्राचीन धार्मिक साहित्य और दार्शनिक विचारों की ओर मुड़ना होगा।
___ भारतीय धर्म और दर्शन के इतिहास में आलोचना और विधर्मता ( heterodoxy) का प्राचीनतम उदाहरण आरण्यक और उपनिषद् में मिलता है। इसके विपरीत संहिता और ब्राह्मण का धर्म व्यावहारिक रूप में मुख्यतया पूजा-पाठ, उत्सव-समारोह, क्रियाकांड और वलि (पशुवलि) आदि की भावना से ओतप्रोत था। यद्यपि ये सभी क्रियाकांड किसी देवता विशेष या भिन्न देवताओं के प्रति किए जाते थे तथापि ये उन देवताओं और अर्चना करनेवाले व्यक्ति के बीच कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं स्थापित करते थे । इन क्रिया-कलापों में कर्मकांड और वलि के तरीकों का हर प्रकार से सही होना अत्यावश्यक था।
१. सावयधम्मदोहा-सं० -- डॉ० हीरालाल जैन-१६०-पृ०-४८. २. कबीरवचनावली-४४७ -पृ० -१३१. ३. औब्सक्योर रेलिजस कल्ट्स-डॉ० शशिभूषणदास गुप्त-पृ०-६१.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org