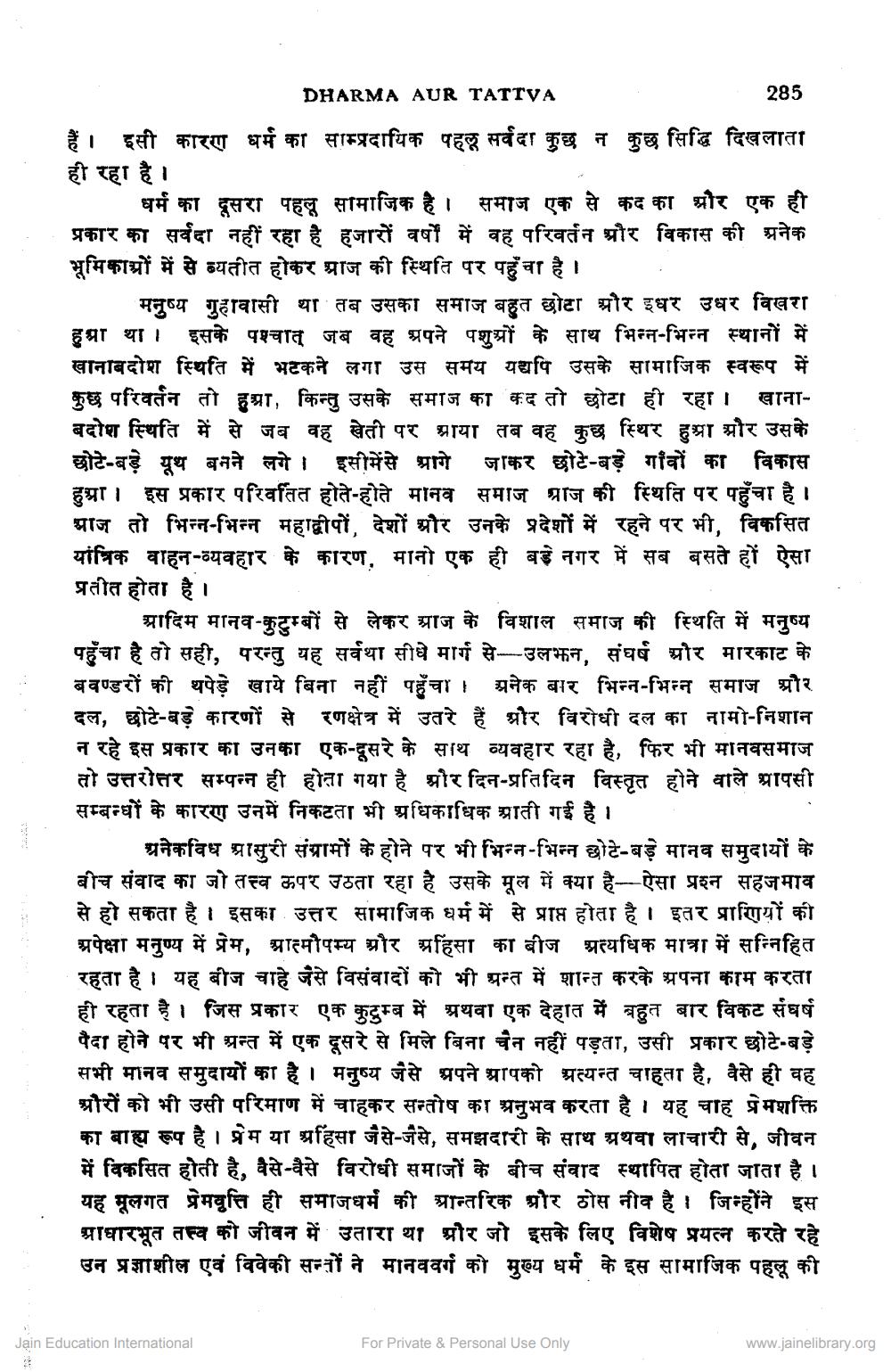________________
DHARMA AUR TATTVA
285 हैं। इसी कारण धर्म का साम्प्रदायिक पहलू सर्वदा कुछ न कुछ सिद्धि दिखलाता ही रहा है।
धर्म का दूसरा पहलू सामाजिक है। समाज एक से कद का और एक ही प्रकार का सर्वदा नहीं रहा है हजारों वर्षों में वह परिवर्तन और विकास की अनेक भूमिकाओं में से व्यतीत होकर प्राज की स्थिति पर पहुंचा है।
मनुष्य गुहावासी था तब उसका समाज बहुत छोटा और इधर उधर विखरा हुआ था। इसके पश्चात् जब वह अपने पशुओं के साथ भिन्न-भिन्न स्थानों में खानाबदोश स्थिति में भटकने लगा उस समय यद्यपि उसके सामाजिक स्वरूप में कुछ परिवर्तन तो हुआ, किन्तु उसके समाज का कद तो छोटा ही रहा। खानाबदोश स्थिति में से जब वह खेती पर आया तब वह कुछ स्थिर हुआ और उसके छोटे-बड़े यूथ बनने लगे। इसीमेंसे आगे जाकर छोटे-बड़े गांवों का विकास हुआ। इस प्रकार परिवर्तित होते-होते मानव समाज प्राज की स्थिति पर पहुँचा है। आज तो भिन्न-भिन्न महाद्वीपों, देशों और उनके प्रदेशों में रहने पर भी, विकसित यांत्रिक वाहन-व्यवहार के कारण, मानो एक ही बड़े नगर में सब बसते हों ऐसा प्रतीत होता है।
___ आदिम मानव-कुटुम्बों से लेकर आज के विशाल समाज की स्थिति में मनुष्य पहुंचा है तो सही, परन्तु यह सर्वथा सीधे मार्ग से-उलझन, संघर्ष और मारकाट के बवण्डरों की थपेड़े खाये बिना नहीं पहुंचा। अनेक बार भिन्न-भिन्न समाज और दल, छोटे-बड़े कारणों से रणक्षेत्र में उतरे हैं और विरोधी दल का नामो-निशान न रहे इस प्रकार का उनका एक-दूसरे के साथ व्यवहार रहा है, फिर भी मानवसमाज तो उत्तरोत्तर सम्पन्न ही होता गया है और दिन-प्रतिदिन विस्तृत होने वाले प्रापसी सम्बन्धों के कारण उनमें निकटता भी अधिकाधिक पाती गई है।
___ अनेकविध प्रासुरी संग्रामों के होने पर भी भिन्न-भिन्न छोटे-बड़े मानव समुदायों के बीच संवाद का जो तत्त्व ऊपर उठता रहा है उसके मूल में क्या है-ऐसा प्रश्न सहजमाव से हो सकता है। इसका उत्तर सामाजिक धर्म में से प्राप्त होता है । इतर प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में प्रेम, आत्मौपम्य और अहिंसा का बीज अत्यधिक मात्रा में सन्निहित रहता है। यह बीज चाहे जैसे विसंवादों को भी अन्त में शान्त करके अपना काम करता ही रहता है। जिस प्रकार एक कुटुम्ब में अथवा एक देहात में बहुत बार विकट संघर्ष पैदा होने पर भी अन्त में एक दूसरे से मिले बिना चैन नहीं पड़ता, उसी प्रकार छोटे-बड़े सभी मानव समुदायों का है। मनुष्य जैसे अपने आपको अत्यन्त चाहता है, वैसे ही वह औरों को भी उसी परिमाण में चाहकर सन्तोष का अनुभव करता है। यह चाह प्रेमशक्ति का बाह्य रूप है । प्रेम या अहिंसा जैसे-जैसे, समझदारी के साथ अथवा लाचारी से, जीवन में विकसित होती है, वैसे-वैसे विरोधी समाजों के बीच संवाद स्थापित होता जाता है । यह मूलगत प्रेमवृत्ति ही समाजधर्म की आन्तरिक और ठोस नीव है। जिन्होंने इस आधारभूत तत्त्व को जीवन में उतारा था और जो इसके लिए विशेष प्रयत्न करते रहे उन प्रज्ञाशील एवं विवेकी सन्तों ने मानववर्ग को मुख्य धर्म के इस सामाजिक पहलू की
Jạin Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org