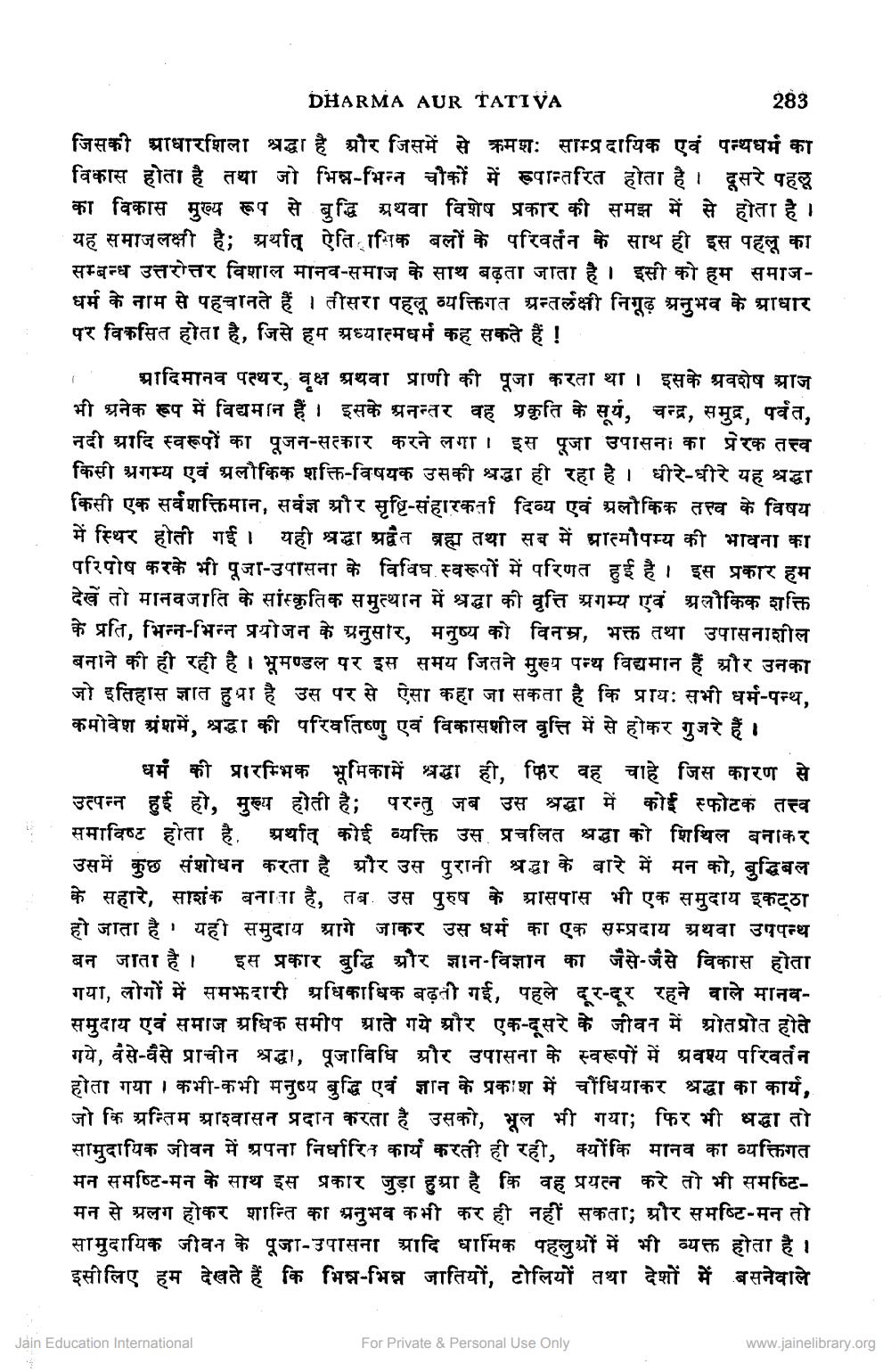________________
DHARMA AUR TATIVA
283 जिसकी आधारशिला श्रद्धा है और जिसमें से क्रमशः साम्प्रदायिक एवं पन्थधर्म का विकास होता है तथा जो भिन्न-भिन्न चौकों में रूपान्तरित होता है। दूसरे पहलू का विकास मुख्य रूप से बुद्धि अथवा विशेष प्रकार की समझ में से होता है । यह समाजलक्षी है; अर्थात् ऐति भिक बलों के परिवर्तन के साथ ही इस पहलू का सम्बन्ध उत्तरोत्तर विशाल मानव-समाज के साथ बढ़ता जाता है। इसी को हम समाजधर्म के नाम से पहचानते हैं । तीसरा पहलू व्यक्तिगत अन्तर्लक्षी निगूढ अनुभव के आधार पर विकसित होता है, जिसे हम अध्यात्मधर्म कह सकते हैं !
। प्रादिमानव पत्थर, वृक्ष अथवा प्राणी की पूजा करता था। इसके अवशेष आज भी अनेक रूप में विद्यमान हैं। इसके अनन्तर वह प्रकृति के सूर्य, चन्द्र, समुद्र, पर्वत, नदी अादि स्वरूपों का पूजन-सत्कार करने लगा। इस पूजा उपासना का प्रेरक तत्त्व किसी अगम्य एवं अलौकिक शक्ति-विषयक उसकी श्रद्धा ही रहा है । धीरे-धीरे यह श्रद्धा किसी एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सृष्टि-संहारकर्ता दिव्य एवं अलौकिक तत्त्व के विषय में स्थिर होती गई। यही श्रद्धा अद्वैत ब्रह्म तथा सब में प्रात्मौपम्य की भावना का परिपोष करके भी पूजा-उपासना के विविध स्वरूपों में परिणत हुई है। इस प्रकार हम देखें तो मानवजाति के सांस्कृतिक समुत्थान में श्रद्धा की वृत्ति अगम्य एवं अलौकिक शक्ति के प्रति, भिन्न-भिन्न प्रयोजन के अनुसार, मनुष्य को विनम्र, भक्त तथा उपासनाशील बनाने की ही रही है। भूमण्डल पर इस समय जितने मुख्य पन्थ विद्यमान हैं और उनका जो इतिहास ज्ञात हुपा है उस पर से ऐसा कहा जा सकता है कि प्रायः सभी धर्म-पन्थ, कमोवेश अंशमें, श्रद्धा की परिवतिष्णु एवं विकासशील वृत्ति में से होकर गुजरे हैं।
धर्म की प्रारम्भिक भूमिकामें श्रद्धा ही, फिर वह चाहे जिस कारण से उत्पन्न हुई हो, मुख्य होती है। परन्तु जब उस श्रद्धा में कोई स्फोटक तत्त्व समाविष्ट होता है. अर्थात् कोई व्यक्ति उस प्रचलित श्रद्धा को शिथिल बनाकर उसमें कुछ संशोधन करता है और उस पुरानी श्रद्धा के बारे में मन को, बुद्धिबल के सहारे, साशंक बनाता है, तब उस पुरुष के आसपास भी एक समुदाय इकट्ठा हो जाता है। यही समुदाय आगे जाकर उस धर्म का एक सम्प्रदाय अथवा उपपन्थ बन जाता है। इस प्रकार बुद्धि और ज्ञान-विज्ञान का जैसे-जैसे विकास होता गया, लोगों में समझदारी अधिकाधिक बढ़ती गई, पहले दूर-दूर रहने वाले मानवसमुदाय एवं समाज अधिक समीप पाते गये और एक-दूसरे के जीवन में प्रोतप्रोत होते गये, वैसे-वैसे प्राचीन श्रद्धा, पूजाविधि और उपासना के स्वरूपों में अवश्य परिवर्तन होता गया। कभी-कभी मनुष्य बुद्धि एवं ज्ञान के प्रकाश में चौंधियाकर श्रद्धा का कार्य, जो कि अन्तिम आश्वासन प्रदान करता है उसको, भूल भी गया; फिर भी श्रद्धा तो सामुदायिक जीवन में अपना निर्धारित कार्य करती ही रही, क्योंकि मानव का व्यक्तिगत मन समष्टि-मन के साथ इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि वह प्रयत्न करे तो भी समष्टिमन से अलग होकर शान्ति का अनुभव कभी कर ही नहीं सकता; और समष्टि-मन तो सामुदायिक जीवन के पूजा-उपासना आदि धार्मिक पहलुओं में भी व्यक्त होता है । इसीलिए हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न जातियों, टोलियों तथा देशों में बसनेवाले
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org