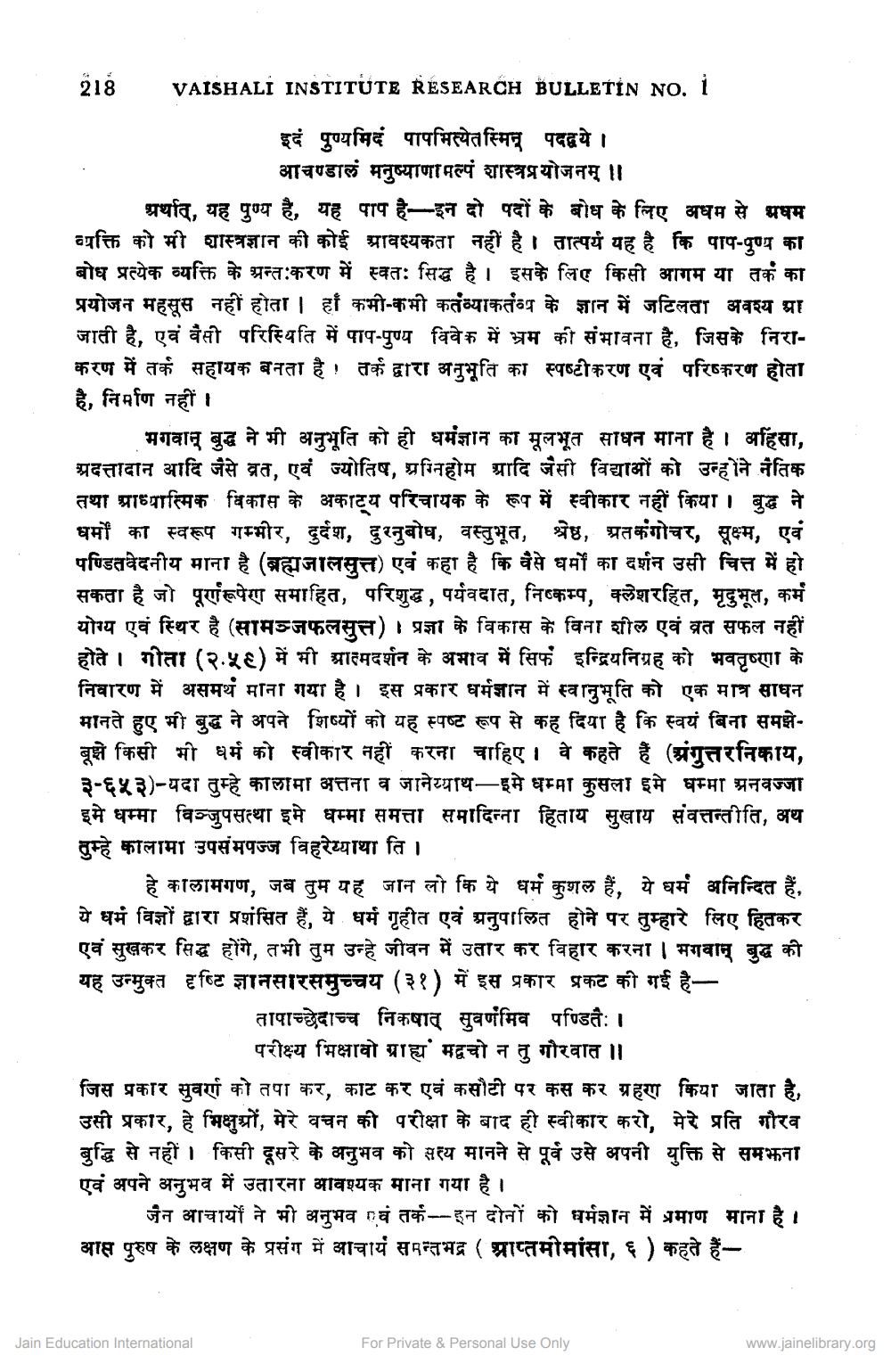________________
218
VAISHALI INSTITUTE RESEARCH BULLETIN NO. 1
इदं पुण्यमिदं पापभित्येतस्मिन् पदद्वये।
आचण्डालं मनुष्याणामल्पं शास्त्रप्रयोजनम् ।। अर्थात्, यह पुण्य है, यह पाप है-इन दो पदों के बोध के लिए अधम से अधम व्यक्ति को भी शास्त्रज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है । तात्पर्य यह है कि पाप-पुण्य का बोध प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःकरण में स्वतः सिद्ध है। इसके लिए किसी आगम या तक का प्रयोजन महसूस नहीं होता। हाँ कभी-कभी कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञान में जटिलता अवश्य प्रा जाती है, एवं वैसी परिस्थिति में पाप-पुण्य विवेक में भ्रम की संभावना है, जिसके निराकरण में तर्क सहायक बनता है। तर्क द्वारा अनुभूति का स्पष्टीकरण एवं परिष्करण होता है, निर्माण नहीं।
भगवान बुद्ध ने भी अनुभूति को ही धर्मज्ञान का मूलभूत साधन माना है । अहिंसा, अदत्तादान आदि जैसे व्रत, एवं ज्योतिष, अग्निहोम आदि जैसी विद्याओं को उन्होंने नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के अकाट्य परिचायक के रूप में स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने धर्मों का स्वरूप गम्भीर, दुर्दश, दुरनुबोध, वस्तुभूत, श्रेष्ठ, अतकंगोचर, सूक्ष्म, एवं पण्डितवेदनीय माना है (ब्रह्मजालसुत्त) एवं कहा है कि वैसे धर्मों का दर्शन उसी चित्त में हो सकता है जो पूर्णरूपेण समाहित, परिशुद्ध , पर्यवदात, निष्कम्प, क्लेशरहित, मृदुभूत, कर्म योग्य एवं स्थिर है (सामञ्जफलसुत्त)। प्रज्ञा के विकास के विना शील एवं व्रत सफल नहीं होते । गीता (२.५६) में भी आत्मदर्शन के अभाव में सिर्फ इन्द्रियनिग्रह को भवतृष्णा के निवारण में असमर्थ माना गया है। इस प्रकार धर्मज्ञान में स्वानुभूति को एक मात्र साधन मानते हुए भी बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि स्वयं बिना समझे. बूझे किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं (अंगुत्तरनिकाय, ३-६५३)-यदा तुम्हे कालामा अत्तना व जानेय्याथ-इमे धम्मा कुसला इमे धम्मा अनवज्जा इमे धम्मा विजृपसत्था इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्तीति, अथ तुम्हे कालामा उपसंमपज्ज विहरेय्याथा ति ।
हे कालामगण, जब तुम यह जान लो कि ये धर्म कुशल हैं, ये धर्म अनिन्दित हैं, ये धर्म विज्ञों द्वारा प्रशंसित हैं, ये धर्म गृहीत एवं अनुपालित होने पर तुम्हारे लिए हितकर एवं सुखकर सिद्ध होंगे, तभी तुम उन्हे जीवन में उतार कर विहार करना । भगवान् बुद्ध की यह उन्मुक्त दृष्टि ज्ञानसारसमुच्चय (३१) में इस प्रकार प्रकट की गई है
तापाच्छेदाच्च निकषात् सुवर्णमिव पण्डितैः ।
परीक्ष्य भिक्षावो ग्राह्यमद्वचो न तु गौरवात ॥ जिस प्रकार सुवर्ण को तपा कर, काट कर एवं कसौटी पर कस कर ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार, हे भिक्षुत्रों, मेरे वचन की परीक्षा के बाद ही स्वीकार करो, मेरे प्रति गौरव बुद्धि से नहीं। किसी दूसरे के अनुभव को सत्य मानने से पूर्व उसे अपनी युक्ति से समझना एवं अपने अनुभव में उतारना आवश्यक माना गया है।
जैन आचार्यों ने भी अनुभव एवं तर्क-इन दोनों को धर्मज्ञान में प्रमाण माना है। आप्त पुरुष के लक्षण के प्रसंग में आचार्य समन्तभद्र ( प्राप्तमीमांसा, ६ ) कहते हैं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org