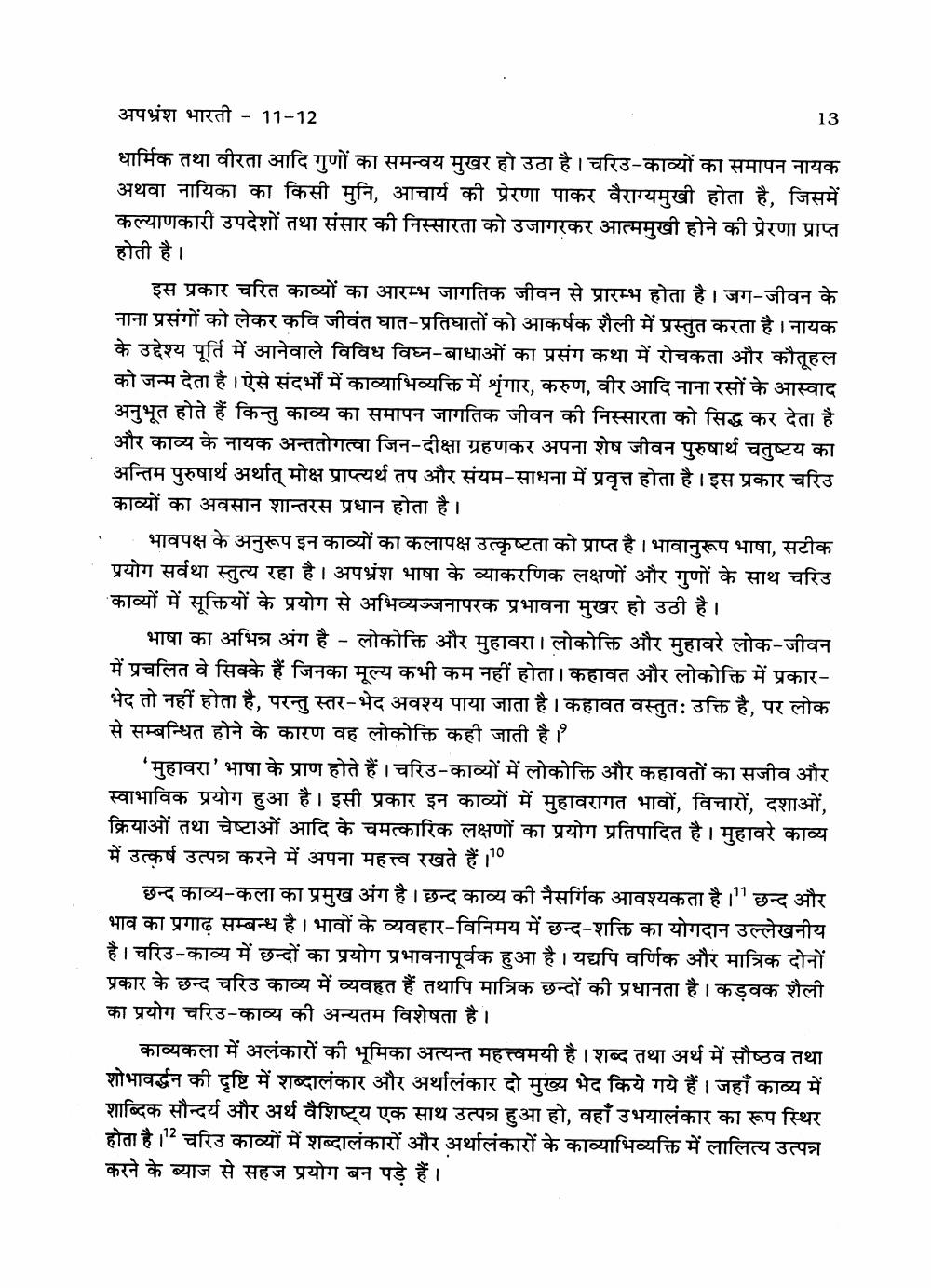________________
13
अपभ्रंश भारती - 11-12 धार्मिक तथा वीरता आदि गुणों का समन्वय मुखर हो उठा है। चरिउ-काव्यों का समापन नायक अथवा नायिका का किसी मुनि, आचार्य की प्रेरणा पाकर वैराग्यमुखी होता है, जिसमें कल्याणकारी उपदेशों तथा संसार की निस्सारता को उजागरकर आत्ममुखी होने की प्रेरणा प्राप्त होती है।
इस प्रकार चरित काव्यों का आरम्भ जागतिक जीवन से प्रारम्भ होता है। जग-जीवन के नाना प्रसंगों को लेकर कवि जीवंत घात-प्रतिघातों को आकर्षक शैली में प्रस्तुत करता है । नायक के उद्देश्य पूर्ति में आनेवाले विविध विघ्न-बाधाओं का प्रसंग कथा में रोचकता और कौतूहल को जन्म देता है । ऐसे संदर्भो में काव्याभिव्यक्ति में शृंगार, करुण, वीर आदि नाना रसों के आस्वाद अनुभूत होते हैं किन्तु काव्य का समापन जागतिक जीवन की निस्सारता को सिद्ध कर देता है और काव्य के नायक अन्ततोगत्वा जिन-दीक्षा ग्रहणकर अपना शेष जीवन पुरुषार्थ चतुष्टय का अन्तिम पुरुषार्थ अर्थात् मोक्ष प्राप्त्यर्थ तप और संयम-साधना में प्रवृत्त होता है । इस प्रकार चरिउ काव्यों का अवसान शान्तरस प्रधान होता है।
. भावपक्ष के अनरूप इन काव्यों का कलापक्ष उत्कृष्टता को प्राप्त है। भावानरूप भाषा, सटीक प्रयोग सर्वथा स्तत्य रहा है। अपभ्रंश भाषा के व्याकरणिक लक्षणों और गणों के साथ चरिउ काव्यों में सूक्तियों के प्रयोग से अभिव्यञ्जनापरक प्रभावना मुखर हो उठी है।
भाषा का अभिन्न अंग है - लोकोक्ति और मुहावरा । लोकोक्ति और मुहावरे लोक-जीवन में प्रचलित वे सिक्के हैं जिनका मूल्य कभी कम नहीं होता। कहावत और लोकोक्ति में प्रकारभेद तो नहीं होता है, परन्तु स्तर-भेद अवश्य पाया जाता है। कहावत वस्तुतः उक्ति है, पर लोक से सम्बन्धित होने के कारण वह लोकोक्ति कही जाती है।'
'मुहावरा' भाषा के प्राण होते हैं । चरिउ-काव्यों में लोकोक्ति और कहावतों का सजीव और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार इन काव्यों में मुहावरागत भावों, विचारों, दशाओं, क्रियाओं तथा चेष्टाओं आदि के चमत्कारिक लक्षणों का प्रयोग प्रतिपादित है। मुहावरे काव्य में उत्कर्ष उत्पन्न करने में अपना महत्त्व रखते हैं।
छन्द काव्य-कला का प्रमुख अंग है। छन्द काव्य की नैसर्गिक आवश्यकता है। छन्द और भाव का प्रगाढ सम्बन्ध है। भावों के व्यवहार-विनिमय में छन्द-शक्ति का योगदान उल्लेखनीय है। चरिउ-काव्य में छन्दों का प्रयोग प्रभावनापूर्वक हुआ है । यद्यपि वर्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छन्द चरिउ काव्य में व्यवहत हैं तथापि मात्रिक छन्दों की प्रधानता है। कड़वक शैली का प्रयोग चरिउ-काव्य की अन्यतम विशेषता है।
काव्यकला में अलंकारों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वमयी है । शब्द तथा अर्थ में सौष्ठव तथा शोभावर्द्धन की दृष्टि में शब्दालंकार और अर्थालंकार दो मुख्य भेद किये गये हैं । जहाँ काव्य में शाब्दिक सौन्दर्य और अर्थ वैशिष्ट्य एक साथ उत्पन्न हुआ हो, वहाँ उभयालंकार का रूप स्थिर होता है। चरिउ काव्यों में शब्दालंकारों और अर्थालंकारों के काव्याभिव्यक्ति में लालित्य उत्पन्न करने के ब्याज से सहज प्रयोग बन पड़े हैं।