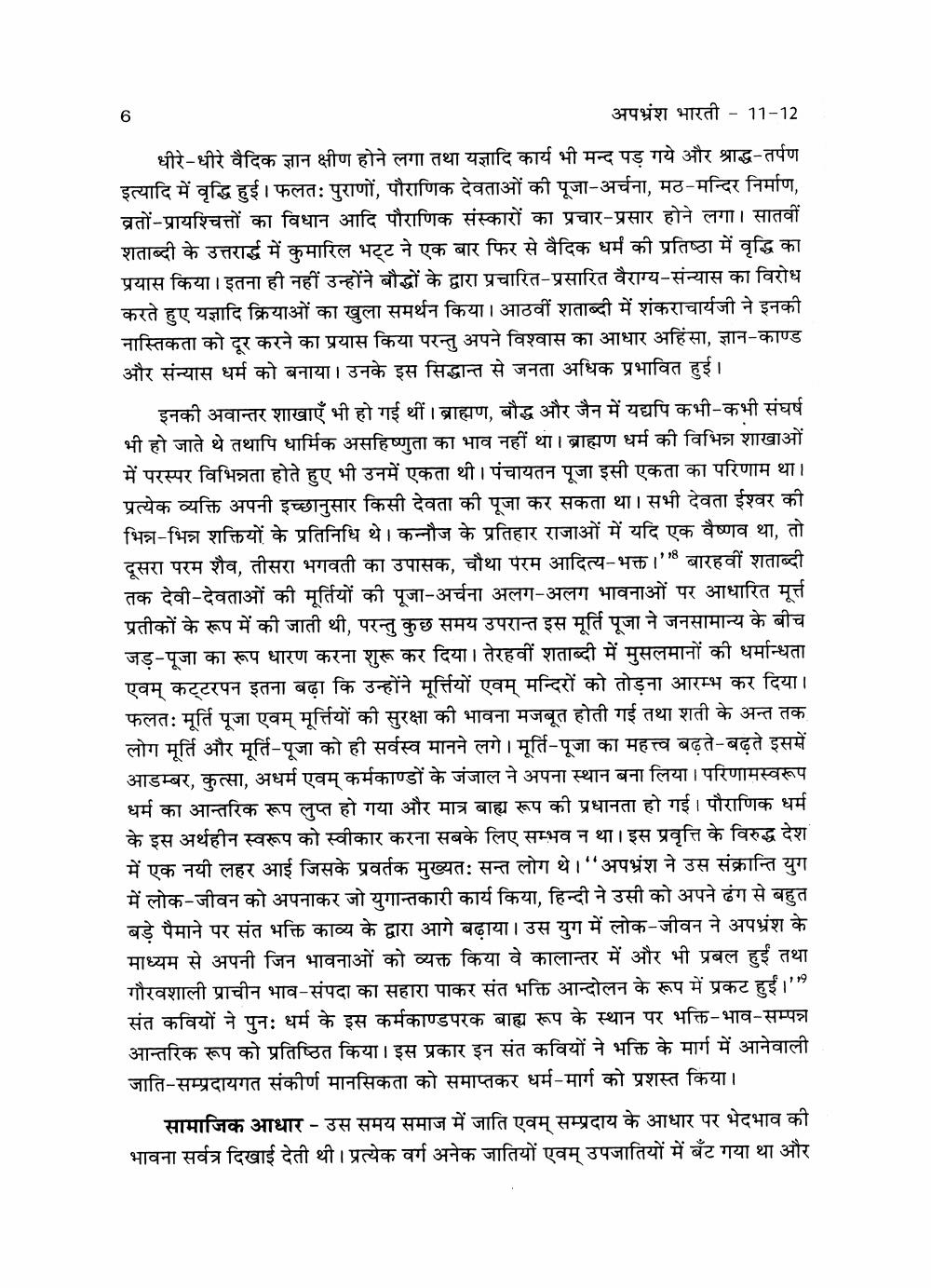________________
अपभ्रंश भारती - 11-12
धीरे-धीरे वैदिक ज्ञान क्षीण होने लगा तथा यज्ञादि कार्य भी मन्द पड़ गये और श्राद्ध-तर्पण इत्यादि में वृद्धि हुई। फलतः पुराणों, पौराणिक देवताओं की पूजा-अर्चना, मठ-मन्दिर निर्माण, व्रतों-प्रायश्चित्तों का विधान आदि पौराणिक संस्कारों का प्रचार-प्रसार होने लगा। सातवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कुमारिल भट्ट ने एक बार फिर से वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि का प्रयास किया। इतना ही नहीं उन्होंने बौद्धों के द्वारा प्रचारित-प्रसारित वैराग्य-संन्यास का विरोध करते हुए यज्ञादि क्रियाओं का खुला समर्थन किया। आठवीं शताब्दी में शंकराचार्यजी ने इनकी नास्तिकता को दूर करने का प्रयास किया परन्तु अपने विश्वास का आधार अहिंसा, ज्ञान-काण्ड और संन्यास धर्म को बनाया। उनके इस सिद्धान्त से जनता अधिक प्रभावित हई। ___ इनकी अवान्तर शाखाएँ भी हो गई थीं। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन में यद्यपि कभी-कभी संघर्ष भी हो जाते थे तथापि धार्मिक असहिष्णुता का भाव नहीं था। ब्राह्मण धर्म की विभिन्न शाखाओं में परस्पर विभिन्नता होते हुए भी उनमें एकता थी। पंचायतन पूजा इसी एकता का परिणाम था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी देवता की पूजा कर सकता था। सभी देवता ईश्वर की भिन्न-भिन्न शक्तियों के प्रतिनिधि थे। कन्नौज के प्रतिहार राजाओं में यदि एक वैष्णव था, तो दूसरा परम शैव, तीसरा भगवती का उपासक, चौथा परम आदित्य-भक्त। 18 बारहवीं शताब्दी तक देवी-देवताओं की मूर्तियों की पूजा-अर्चना अलग-अलग भावनाओं पर आधारित मूर्त प्रतीकों के रूप में की जाती थी, परन्तु कुछ समय उपरान्त इस मूर्ति पूजा ने जनसामान्य के बीच
रूप धारण करना शुरू कर दिया। तेरहवीं शताब्दी में मुसलमानों की धर्मान्धता एवम कटटरपन इतना बढा कि उन्होंने मर्तियों एवम मन्दिरों को तोडना आरम्भ कर दिया। फलतः मूर्ति पूजा एवम् मूर्तियों की सुरक्षा की भावना मजबूत होती गई तथा शती के अन्त तक लोग मूर्ति और मूर्ति-पूजा को ही सर्वस्व मानने लगे। मूर्ति-पूजा का महत्त्व बढ़ते-बढ़ते इसमें आडम्बर, कुत्सा, अधर्म एवम् कर्मकाण्डों के जंजाल ने अपना स्थान बना लिया। परिणामस्वरूप धर्म का आन्तरिक रूप लुप्त हो गया और मात्र बाह्य रूप की प्रधानता हो गई। पौराणिक धर्म के इस अर्थहीन स्वरूप को स्वीकार करना सबके लिए सम्भव न था। इस प्रवृत्ति के विरुद्ध देश में एक नयी लहर आई जिसके प्रवर्तक मुख्यतः सन्त लोग थे।"अपभ्रंश ने उस संक्रान्ति युग में लोक-जीवन को अपनाकर जो युगान्तकारी कार्य किया, हिन्दी ने उसी को अपने ढंग से बहुत बड़े पैमाने पर संत भक्ति काव्य के द्वारा आगे बढ़ाया। उस युग में लोक-जीवन ने अपभ्रंश के माध्यम से अपनी जिन भावनाओं को व्यक्त किया वे कालान्तर में और भी प्रबल हुईं तथा गौरवशाली प्राचीन भाव-संपदा का सहारा पाकर संत भक्ति आन्दोलन के रूप में प्रकट हईं।” संत कवियों ने पुनः धर्म के इस कर्मकाण्डपरक बाह्य रूप के स्थान पर भक्ति-भाव-सम्पन्न आन्तरिक रूप को प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार इन संत कवियों ने भक्ति के मार्ग में आनेवा जाति-सम्प्रदायगत संकीर्ण मानसिकता को समाप्तकर धर्म-मार्ग को प्रशस्त किया।
सामाजिक आधार - उस समय समाज में जाति एवम् सम्प्रदाय के आधार पर भेदभाव की भावना सर्वत्र दिखाई देती थी। प्रत्येक वर्ग अनेक जातियों एवम् उपजातियों में बँट गया था और