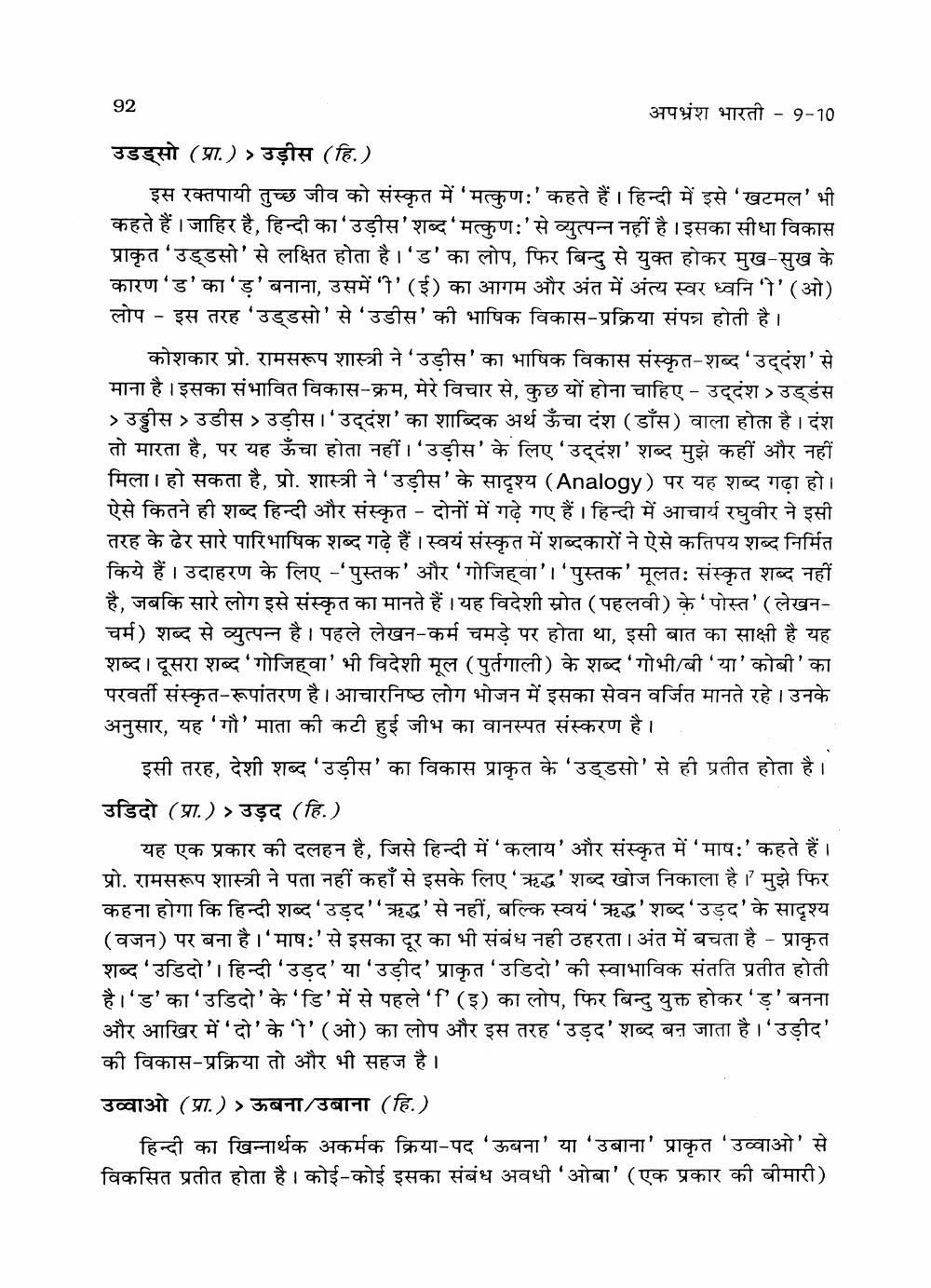________________
92
अपभ्रंश भारती - 9-10 उडड्सो (प्रा.) - उड़ीस (हि.)
इस रक्तपायी तुच्छ जीव को संस्कृत में 'मत्कुणः' कहते हैं । हिन्दी में इसे 'खटमल' भी कहते हैं । जाहिर है, हिन्दी का 'उड़ीस' शब्द 'मत्कुणः' से व्युत्पन्न नहीं है । इसका सीधा विकास प्राकृत 'उड्डसो' से लक्षित होता है। 'ड' का लोप, फिर बिन्दु से युक्त होकर मुख-सुख के कारण 'ड' का 'ड़' बनाना, उसमें "' (ई) का आगम और अंत में अंत्य स्वर ध्वनि '' (ओ) लोप - इस तरह 'उड्डसो' से 'उडीस' की भाषिक विकास-प्रक्रिया संपन्न होती है। ___ कोशकार प्रो. रामसरूप शास्त्री ने 'उड़ीस' का भाषिक विकास संस्कृत-शब्द 'उदंश' से माना है। इसका संभावित विकास-क्रम, मेरे विचार से, कुछ यों होना चाहिए - उदंश > उड्ड्स > उड्डीस > उडीस > उड़ीस । 'उदंश' का शाब्दिक अर्थ ऊँचा दंश (डाँस) वाला होता है । दंश तो मारता है, पर यह ऊँचा होता नहीं। 'उड़ीस' के लिए 'उदंश' शब्द मुझे कहीं और नहीं मिला। हो सकता है, प्रो. शास्त्री ने 'उड़ीस' के सादृश्य (Analogy) पर यह शब्द गढ़ा हो। ऐसे कितने ही शब्द हिन्दी और संस्कृत - दोनों में गढ़े गए हैं। हिन्दी में आचार्य रघुवीर ने इसी तरह के ढेर सारे पारिभाषिक शब्द गढ़े हैं । स्वयं संस्कृत में शब्दकारों ने ऐसे कतिपय शब्द निर्मित किये हैं। उदाहरण के लिए -'पुस्तक' और 'गोजिह्वा' । 'पुस्तक' मूलत: संस्कृत शब्द नहीं है, जबकि सारे लोग इसे संस्कृत का मानते हैं । यह विदेशी स्रोत (पहलवी) के 'पोस्त' (लेखनचर्म) शब्द से व्यत्पन्न है। पहले लेखन-कर्म चमडे पर होता था. इसी बात का साक्षी है यह शब्द। दूसरा शब्द 'गोजिह्वा' भी विदेशी मूल (पुर्तगाली) के शब्द 'गोभी/बी 'या' कोबी' का परवर्ती संस्कृत-रूपांतरण है। आचारनिष्ठ लोग भोजन में इसका सेवन वर्जित मानते रहे । उनके अनुसार, यह 'गौ' माता की कटी हुई जीभ का वानस्पत संस्करण है।
इसी तरह, देशी शब्द 'उड़ीस' का विकास प्राकृत के 'उड्डसो' से ही प्रतीत होता है। उडिदो (प्रा.) - उड़द (हि.) ____ यह एक प्रकार की दलहन है, जिसे हिन्दी में 'कलाय' और संस्कृत में 'माषः' कहते हैं। प्रो. रामसरूप शास्त्री ने पता नहीं कहाँ से इसके लिए 'ऋद्ध' शब्द खोज निकाला है। मुझे फिर कहना होगा कि हिन्दी शब्द 'उड़द''ऋद्ध' से नहीं, बल्कि स्वयं 'ऋद्ध' शब्द 'उड़द' के सादृश्य (वजन) पर बना है। 'माष:' से इसका दूर का भी संबंध नही ठहरता। अंत में बचता है - प्राकृत शब्द 'उडिदो'। हिन्दी 'उड़द' या 'उड़ीद' प्राकृत 'उडिदो' की स्वाभाविक संतति प्रतीत होती है। 'ड' का 'उडिदो' के 'डि' में से पहले 'f' (इ) का लोप, फिर बिन्दु युक्त होकर 'ड' बनना और आखिर में 'दो' के ी' (ओ) का लोप और इस तरह 'उड़द' शब्द बन जाता है । 'उड़ीद' की विकास-प्रक्रिया तो और भी सहज है।
उव्वाओ (प्रा.) » ऊबना/उबाना (हि.)
हिन्दी का खिन्नार्थक अकर्मक क्रिया-पद 'ऊबना' या 'उबाना' प्राकृत 'उव्वाओ' से विकसित प्रतीत होता है। कोई-कोई इसका संबंध अवधी 'ओबा' (एक प्रकार की बीमारी)