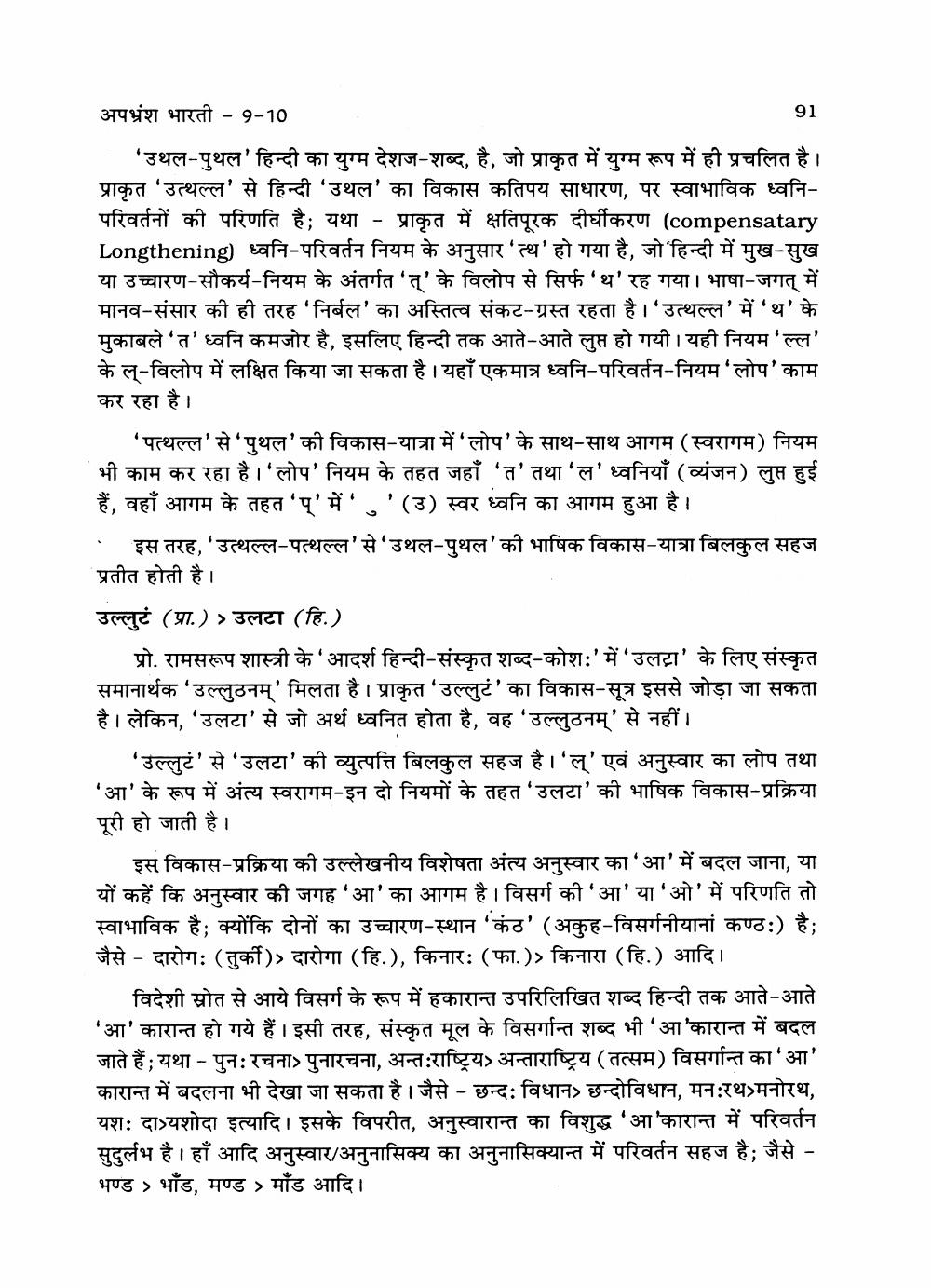________________
अपभ्रंश भारती - 9-10
91
'उथल-पुथल' हिन्दी का युग्म देशज-शब्द, है, जो प्राकृत में युग्म रूप में ही प्रचलित है। प्राकृत 'उत्थल्ल' से हिन्दी 'उथल' का विकास कतिपय साधारण, पर स्वाभाविक ध्वनिपरिवर्तनों की परिणति है; यथा - प्राकृत में क्षतिपूरक दीर्धीकरण (compensatary Longthening) ध्वनि-परिवर्तन नियम के अनुसार 'त्थ' हो गया है, जो हिन्दी में मुख-सुख या उच्चारण-सौकर्य-नियम के अंतर्गत 'त्' के विलोप से सिर्फ 'थ' रह गया। भाषा-जगत् में मानव-संसार की ही तरह 'निर्बल' का अस्तित्व संकट-ग्रस्त रहता है। 'उत्थल्ल' में 'थ' के मुकाबले 'त' ध्वनि कमजोर है, इसलिए हिन्दी तक आते-आते लुप्त हो गयी। यही नियम 'ल्ल' के ल्-विलोप में लक्षित किया जा सकता है । यहाँ एकमात्र ध्वनि-परिवर्तन-नियम 'लोप' काम कर रहा है। ___'पत्थल्ल' से 'पुथल' की विकास-यात्रा में 'लोप' के साथ-साथ आगम (स्वरागम) नियम भी काम कर रहा है। लोप' नियम के तहत जहाँ 'त' तथा 'ल' ध्वनियाँ (व्यंजन) लुप्त हुई हैं, वहाँ आगम के तहत प्' में ', ' (उ) स्वर ध्वनि का आगम हुआ है। ' इस तरह, 'उत्थल्ल-पत्थल्ल' से 'उथल-पुथल' की भाषिक विकास-यात्रा बिलकुल सहज प्रतीत होती है। उल्लुटं (प्रा.) > उलटा (हि.)
प्रो. रामसरूप शास्त्री के 'आदर्श हिन्दी-संस्कृत शब्द-कोशः' में 'उलट्रा' के लिए संस्कृत समानार्थक 'उल्लुठनम्' मिलता है। प्राकृत 'उल्लुटं' का विकास-सूत्र इससे जोड़ा जा सकता है। लेकिन, 'उलटा' से जो अर्थ ध्वनित होता है, वह 'उल्लुठनम्' से नहीं।
__'उल्लुटं' से 'उलटा' की व्युत्पत्ति बिलकुल सहज है। 'ल्' एवं अनुस्वार का लोप तथा 'आ' के रूप में अंत्य स्वरागम-इन दो नियमों के तहत 'उलटा' की भाषिक विकास-प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ___ इस विकास-प्रक्रिया की उल्लेखनीय विशेषता अंत्य अनुस्वार का 'आ' में बदल जाना, या यों कहें कि अनुस्वार की जगह 'आ' का आगम है । विसर्ग की 'आ' या 'ओ' में परिणति तो स्वाभाविक है; क्योंकि दोनों का उच्चारण-स्थान 'कंठ' (अकुह-विसर्गनीयानां कण्ठः) है; जैसे - दारोगः (तुर्की)> दारोगा (हि.), किनारः (फा.)> किनारा (हि.) आदि।
विदेशी स्रोत से आये विसर्ग के रूप में हकारान्त उपरिलिखित शब्द हिन्दी तक आते-आते 'आ' कारान्त हो गये हैं। इसी तरह, संस्कृत मूल के विसर्गान्त शब्द भी 'आ'कारान्त में बदल जाते हैं; यथा - पुनः रचना> पुनारचना, अन्त:राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय (तत्सम) विसर्गान्त का 'आ' कारान्त में बदलना भी देखा जा सकता है। जैसे - छन्दः विधान> छन्दोविधान, मन:रथ मनोरथ, यशः दा>यशोदा इत्यादि। इसके विपरीत, अनुस्वारान्त का विशुद्ध 'आ'कारान्त में परिवर्तन सुदुर्लभ है। हाँ आदि अनुस्वार/अनुनासिक्य का अनुनासिक्यान्त में परिवर्तन सहज है; जैसे - भण्ड > भाँड, मण्ड > माँड आदि।