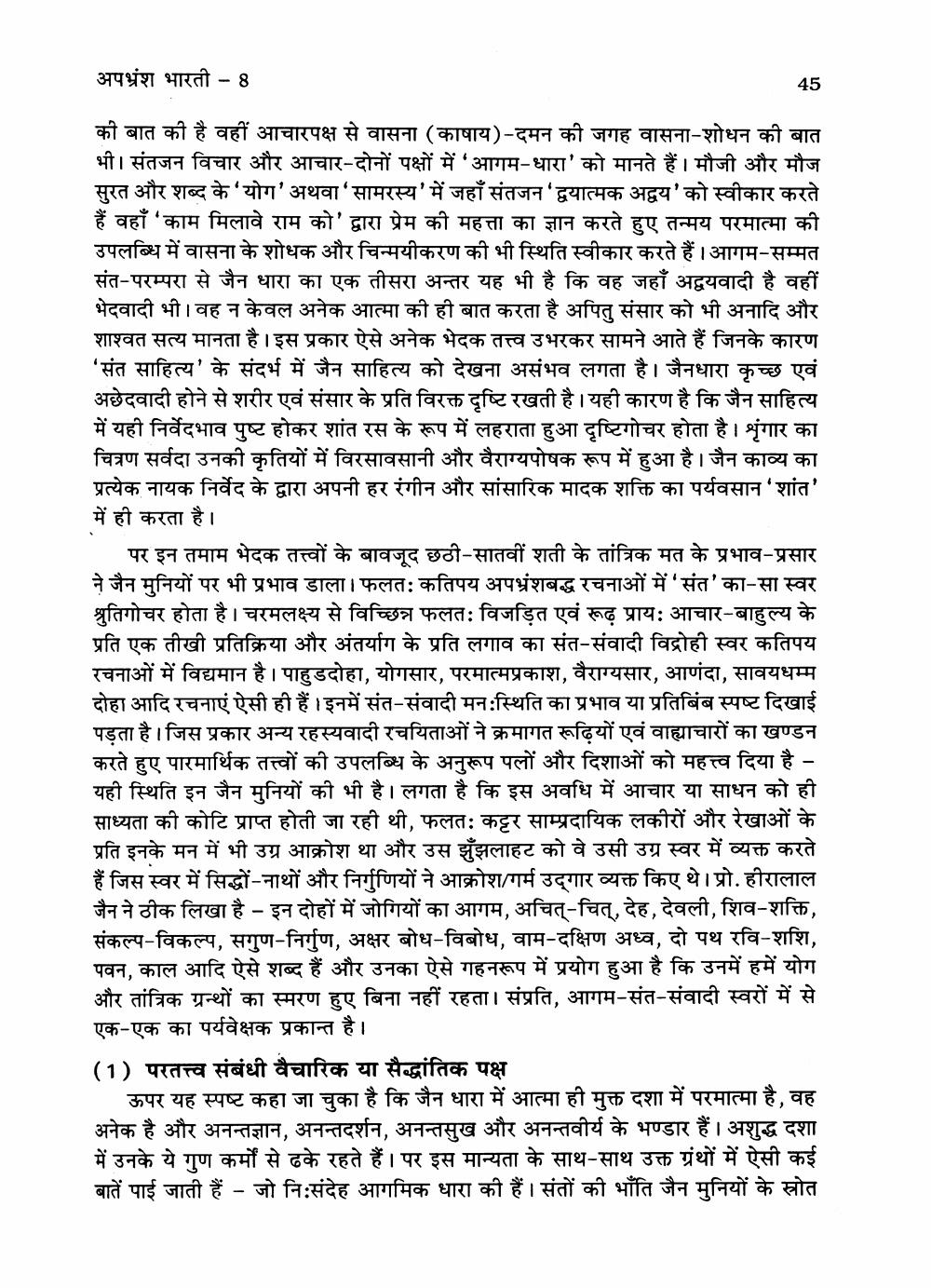________________
अपभ्रंश भारती - 8
45
की बात की है वहीं आचारपक्ष से वासना (काषाय)-दमन की जगह वासना-शोधन की बात भी। संतजन विचार और आचार-दोनों पक्षों में 'आगम-धारा' को मानते हैं। मौजी और मौज सरत और शब्द के 'योग' अथवा 'सामरस्य' में जहाँ संतजन'द्वयात्मक अद्य' को स्वीकार करते हैं वहाँ 'काम मिलावे राम को' द्वारा प्रेम की महत्ता का ज्ञान करते हुए तन्मय परमात्मा की उपलब्धि में वासना के शोधक और चिन्मयीकरण की भी स्थिति स्वीकार करते हैं। आगम-सम्मत संत-परम्परा से जैन धारा का एक तीसरा अन्तर यह भी है कि वह जहाँ अद्वयवादी है वहीं भेदवादी भी। वह न केवल अनेक आत्मा की ही बात करता है अपितु संसार को भी अनादि और शाश्वत सत्य मानता है। इस प्रकार ऐसे अनेक भेदक तत्त्व उभरकर सामने आते हैं जिनके कारण 'संत साहित्य' के संदर्भ में जैन साहित्य को देखना असंभव लगता है। जैनधारा कृच्छ एवं अछेदवादी होने से शरीर एवं संसार के प्रति विरक्त दृष्टि रखती है। यही कारण है कि जैन साहित्य में यही निर्वेदभाव पुष्ट होकर शांत रस के रूप में लहराता हुआ दृष्टिगोचर होता है। श्रृंगार का चित्रण सर्वदा उनकी कतियों में विरसावसानी और वैराग्यपोषक रूप में हआ है। जैन काव्य का प्रत्येक नायक निर्वेद के द्वारा अपनी हर रंगीन और सांसारिक मादक शक्ति का पर्यवसान 'शांत' में ही करता है।
पर इन तमाम भेदक तत्त्वों के बावजूद छठी-सातवीं शती के तांत्रिक मत के प्रभाव-प्रसार ने जैन मुनियों पर भी प्रभाव डाला। फलतः कतिपय अपभ्रंशबद्ध रचनाओं में 'संत' का-सा स्वर श्रुतिगोचर होता है। चरमलक्ष्य से विच्छिन्न फलतः विजड़ित एवं रूढ़ प्रायः आचार-बाहुल्य के प्रति एक तीखी प्रतिक्रिया और अंतर्याग के प्रति लगाव का संत-संवादी विद्रोही स्वर कतिपय रचनाओं में विद्यमान है। पाहुडदोहा, योगसार, परमात्मप्रकाश, वैराग्यसार, आणंदा, सावयधम्म दोहा आदि रचनाएं ऐसी ही हैं। इनमें संत-संवादी मन:स्थिति का प्रभाव या प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार अन्य रहस्यवादी रचयिताओं ने क्रमागत रूढ़ियों एवं वाह्याचारों का खण्डन करते हुए पारमार्थिक तत्त्वों की उपलब्धि के अनुरूप पलों और दिशाओं को महत्त्व दिया है - यही स्थिति इन जैन मुनियों की भी है। लगता है कि इस अवधि में आचार या साधन को ही साध्यता की कोटि प्राप्त होती जा रही थी, फलत: कट्टर साम्प्रदायिक लकीरों और रेखाओं के प्रति इनके मन में भी उग्र आक्रोश था और उस झुंझलाहट को वे उसी उग्र स्वर में व्यक्त करते हैं जिस स्वर में सिद्धों-नाथों और निर्गुणियों ने आक्रोश/गर्म उद्गार व्यक्त किए थे। प्रो. हीरालाल जैन ने ठीक लिखा है - इन दोहों में जोगियों का आगम, अचित्-चित्, देह, देवली, शिव-शक्ति, संकल्प-विकल्प, सगुण-निर्गुण, अक्षर बोध-विबोध, वाम-दक्षिण अध्व, दो पथ रवि-शशि, पवन, काल आदि ऐसे शब्द हैं और उनका ऐसे गहनरूप में प्रयोग हुआ है कि उनमें हमें योग
और तांत्रिक ग्रन्थों का स्मरण हुए बिना नहीं रहता। संप्रति, आगम-संत-संवादी स्वरों में से एक-एक का पर्यवेक्षक प्रकान्त है। (1) परतत्त्व संबंधी वैचारिक या सैद्धांतिक पक्ष
ऊपर यह स्पष्ट कहा जा चुका है कि जैन धारा में आत्मा ही मुक्त दशा में परमात्मा है, वह अनेक है और अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य के भण्डार हैं। अशुद्ध दशा में उनके ये गुण कर्मों से ढके रहते हैं। पर इस मान्यता के साथ-साथ उक्त ग्रंथों में ऐसी कई बातें पाई जाती हैं - जो नि:संदेह आगमिक धारा की हैं। संतों की भाँति जैन मुनियों के स्रोत