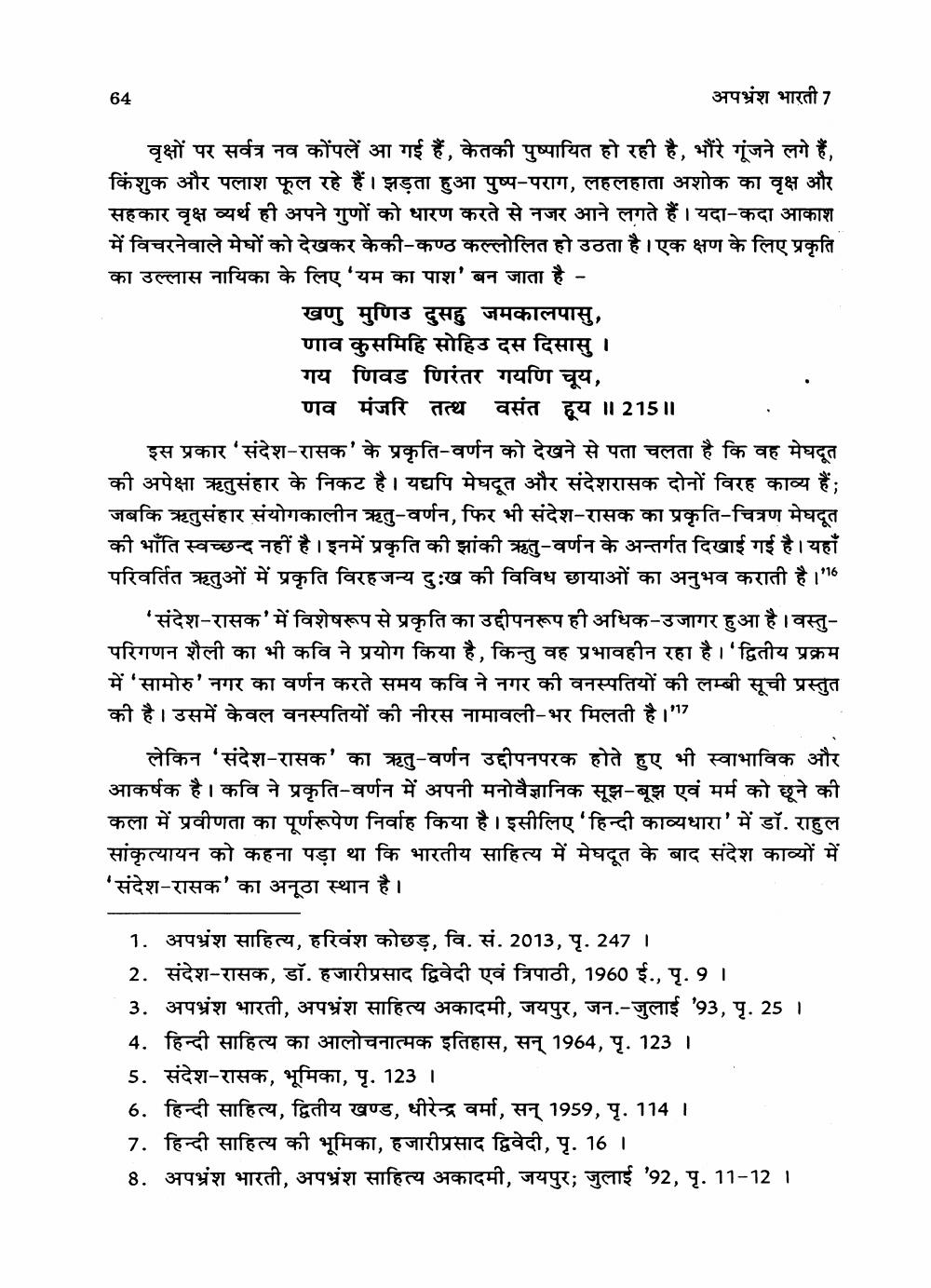________________
64
अपभ्रंश भारती7
वृक्षों पर सर्वत्र नव कोंपलें आ गई हैं, केतकी पुष्पायित हो रही है, भौंरे गूंजने लगे हैं, किंशुक और पलाश फूल रहे हैं। झड़ता हुआ पुष्प-पराग, लहलहाता अशोक का वृक्ष और सहकार वृक्ष व्यर्थ ही अपने गुणों को धारण करते से नजर आने लगते हैं । यदा-कदा आकाश में विचरनेवाले मेघों को देखकर केकी-कण्ठ कल्लोलित हो उठता है। एक क्षण के लिए प्रकृति का उल्लास नायिका के लिए 'यम का पाश' बन जाता है -
खणु मुणिउ दुसहु जमकालपासु, णाव कुसमिहि सोहिउ दस दिसासु । गय णिवड णिरंतर गयणि चूय,
णव मंजरि तत्थ वसंत हूय ॥ 215॥ इस प्रकार 'संदेश-रासक' के प्रकृति-वर्णन को देखने से पता चलता है कि वह मेघदूत की अपेक्षा ऋतुसंहार के निकट है। यद्यपि मेघदूत और संदेशरासक दोनों विरह काव्य हैं; जबकि ऋतुसंहार संयोगकालीन ऋतु-वर्णन, फिर भी संदेश-रासक का प्रकृति-चित्रण मेघदूत की भाँति स्वच्छन्द नहीं है। इनमें प्रकृति की झांकी ऋतु-वर्णन के अन्तर्गत दिखाई गई है। यहाँ परिवर्तित ऋतुओं में प्रकृति विरहजन्य दुःख की विविध छायाओं का अनुभव कराती है।
'संदेश-रासक' में विशेषरूप से प्रकृति का उद्दीपनरूप ही अधिक-उजागर हुआ है । वस्तुपरिगणन शैली का भी कवि ने प्रयोग किया है, किन्तु वह प्रभावहीन रहा है। द्वितीय प्रक्रम में 'सामोरु' नगर का वर्णन करते समय कवि ने नगर की वनस्पतियों की लम्बी सूची प्रस्तुत की है। उसमें केवल वनस्पतियों की नीरस नामावली-भर मिलती है।"
लेकिन 'संदेश-रासक' का ऋतु-वर्णन उद्दीपनपरक होते हुए भी स्वाभाविक और आकर्षक है। कवि ने प्रकृति-वर्णन में अपनी मनोवैज्ञानिक सूझ-बूझ एवं मर्म को छूने की कला में प्रवीणता का पूर्णरूपेण निर्वाह किया है। इसीलिए 'हिन्दी काव्यधारा' में डॉ. राहुल सांकृत्यायन को कहना पड़ा था कि भारतीय साहित्य में मेघदूत के बाद संदेश काव्यों में 'संदेश-रासक' का अनूठा स्थान है।
1. अपभ्रंश साहित्य, हरिवंश कोछड़, वि. सं. 2013, पृ. 247 । 2. संदेश-रासक, डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी एवं त्रिपाठी, 1960 ई., पृ. 9 । 3. अपभ्रंश भारती, अपभ्रंश साहित्य अकादमी, जयपुर, जन.-जुलाई '93, पृ. 25 । 4. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सन् 1964, पृ. 123 । 5. संदेश-रासक, भूमिका, पृ. 123 । 6. हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड, धीरेन्द्र वर्मा, सन् 1959, पृ. 114 । 7. हिन्दी साहित्य की भूमिका, हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ. 16 ।। 8. अपभ्रंश भारती, अपभ्रंश साहित्य अकादमी, जयपुर; जुलाई '92, पृ. 11-12 ।