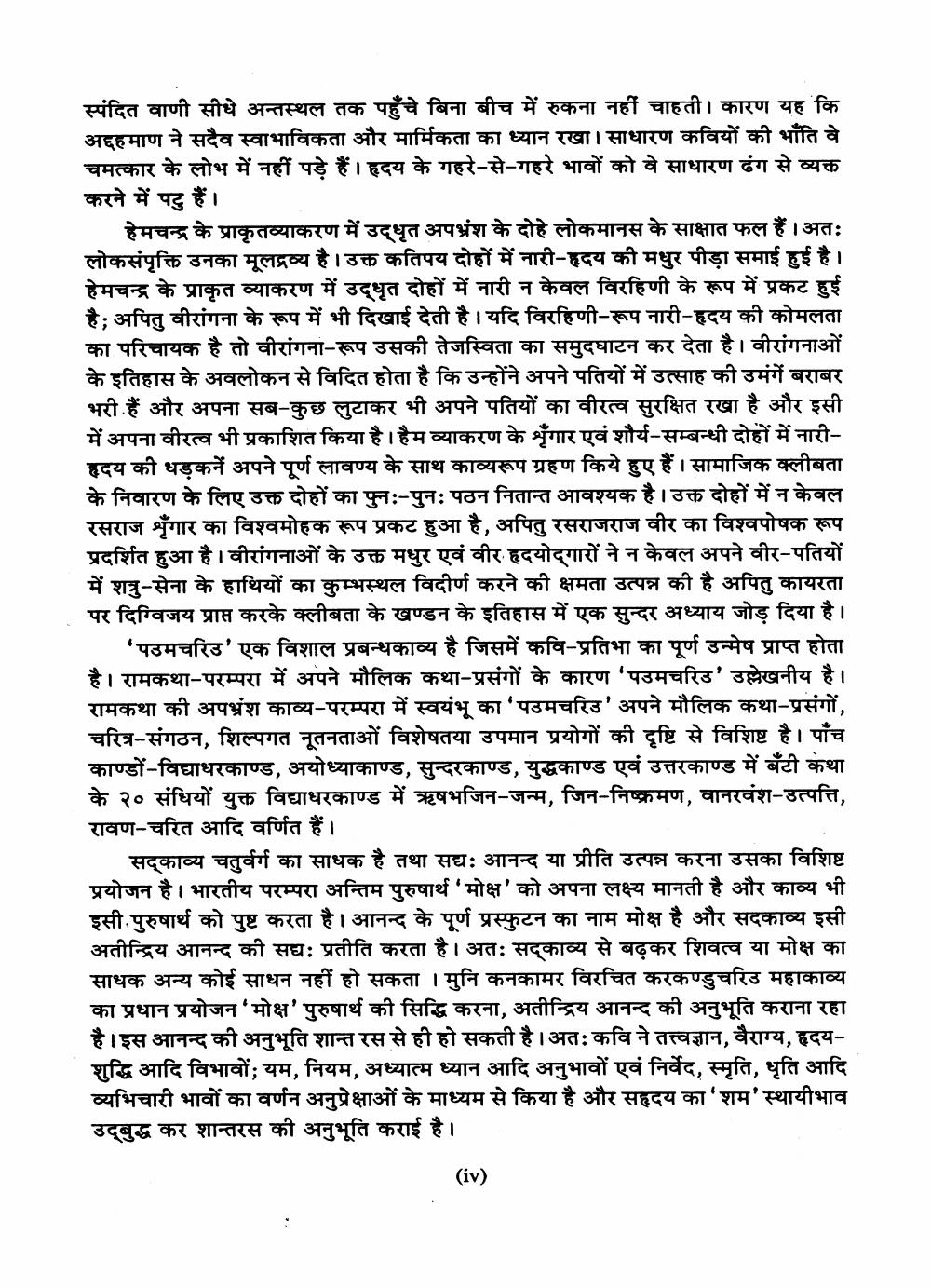________________
स्पंदित वाणी सीधे अन्तस्थल तक पहुंचे बिना बीच में रुकना नहीं चाहती। कारण यह कि अद्दहमाण ने सदैव स्वाभाविकता और मार्मिकता का ध्यान रखा। साधारण कवियों की भाँति वे चमत्कार के लोभ में नहीं पड़े हैं। हृदय के गहरे-से-गहरे भावों को वे साधारण ढंग से व्यक्त करने में पटु हैं।
हेमचन्द्र के प्राकृतव्याकरण में उद्धृत अपभ्रंश के दोहे लोकमानस के साक्षात फल हैं। अतः लोकसंपृक्ति उनका मूलद्रव्य है। उक्त कतिपय दोहों में नारी-हृदय की मधुर पीड़ा समाई हुई है। हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में उद्धृत दोहों में नारी न केवल विरहिणी के रूप में प्रकट हई है; अपितु वीरांगना के रूप में भी दिखाई देती है। यदि विरहिणी-रूप नारी-हृदय की कोमलता का परिचायक है तो वीरांगना-रूप उसकी तेजस्विता का समुदघाटन कर देता है। वीरांगनाओं के इतिहास के अवलोकन से विदित होता है कि उन्होंने अपने पतियों में उत्साह की उमंगें बराबर भरी हैं और अपना सब-कुछ लुटाकर भी अपने पतियों का वीरत्व सुरक्षित रखा है और इसी में अपना वीरत्व भी प्रकाशित किया है। हैम व्याकरण के श्रृंगार एवं शौर्य-सम्बन्धी दोहों में नारीहृदय की धड़कनें अपने पूर्ण लावण्य के साथ काव्यरूप ग्रहण किये हुए हैं। सामाजिक क्लीबता के निवारण के लिए उक्त दोहों का पुनः-पुनः पठन नितान्त आवश्यक है। उक्त दोहों में न केवल रसराज श्रृंगार का विश्वमोहक रूप प्रकट हुआ है, अपितु रसराजराज वीर का विश्वपोषक रूप प्रदर्शित हुआ है । वीरांगनाओं के उक्त मधुर एवं वीर हृदयोद्गारों ने न केवल अपने वीर-पतियों में शत्रु-सेना के हाथियों का कुम्भस्थल विदीर्ण करने की क्षमता उत्पन्न की है अपितु कायरता पर दिग्विजय प्राप्त करके क्लीबता के खण्डन के इतिहास में एक सुन्दर अध्याय जोड़ दिया है। ___'पउमचरिउ' एक विशाल प्रबन्धकाव्य है जिसमें कवि-प्रतिभा का पूर्ण उन्मेष प्राप्त होता
-परम्परा में अपने मौलिक कथा-प्रसंगों के कारण 'पउमचरिउ' उल्लेखनीय है। रामकथा की अपभ्रंश काव्य-परम्परा में स्वयंभू का 'पउमचरिउ' अपने मौलिक कथा-प्रसंगों, चरित्र-संगठन, शिल्पगत नूतनताओं विशेषतया उपमान प्रयोगों की दृष्टि से विशिष्ट है। पाँच काण्डों-विद्याधरकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड में बँटी कथा के २० संधियों युक्त विद्याधरकाण्ड में ऋषभजिन-जन्म, जिन-निष्क्रमण, वानरवंश-उत्पत्ति, रावण-चरित आदि वर्णित हैं।
सद्काव्य चतुर्वर्ग का साधक है तथा सद्यः आनन्द या प्रीति उत्पन्न करना उसका विशिष्ट प्रयोजन है। भारतीय परम्परा अन्तिम पुरुषार्थ 'मोक्ष' को अपना लक्ष्य मानती है और काव्य भी इसी पुरुषार्थ को पुष्ट करता है। आनन्द के पूर्ण प्रस्फुटन का नाम मोक्ष है और सदकाव्य इसी अतीन्द्रिय आनन्द की सद्यः प्रतीति करता है। अतः सद्काव्य से बढ़कर शिवत्व या मोक्ष का साधक अन्य कोई साधन नहीं हो सकता । मुनि कनकामर विरचित करकण्डुचरिउ महाकाव्य का प्रधान प्रयोजन 'मोक्ष' पुरुषार्थ की सिद्धि करना, अतीन्द्रिय आनन्द की अनुभूति कराना रहा है। इस आनन्द की अनुभूति शान्त रस से ही हो सकती है। अतः कवि ने तत्त्वज्ञान, वैराग्य, हृदयशुद्धि आदि विभावों; यम, नियम, अध्यात्म ध्यान आदि अनुभावों एवं निर्वेद, स्मृति, धृति आदि व्यभिचारी भावों का वर्णन अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से किया है और सहृदय का 'शम' स्थायीभाव उद्बुद्ध कर शान्तरस की अनुभूति कराई है।
(iv)