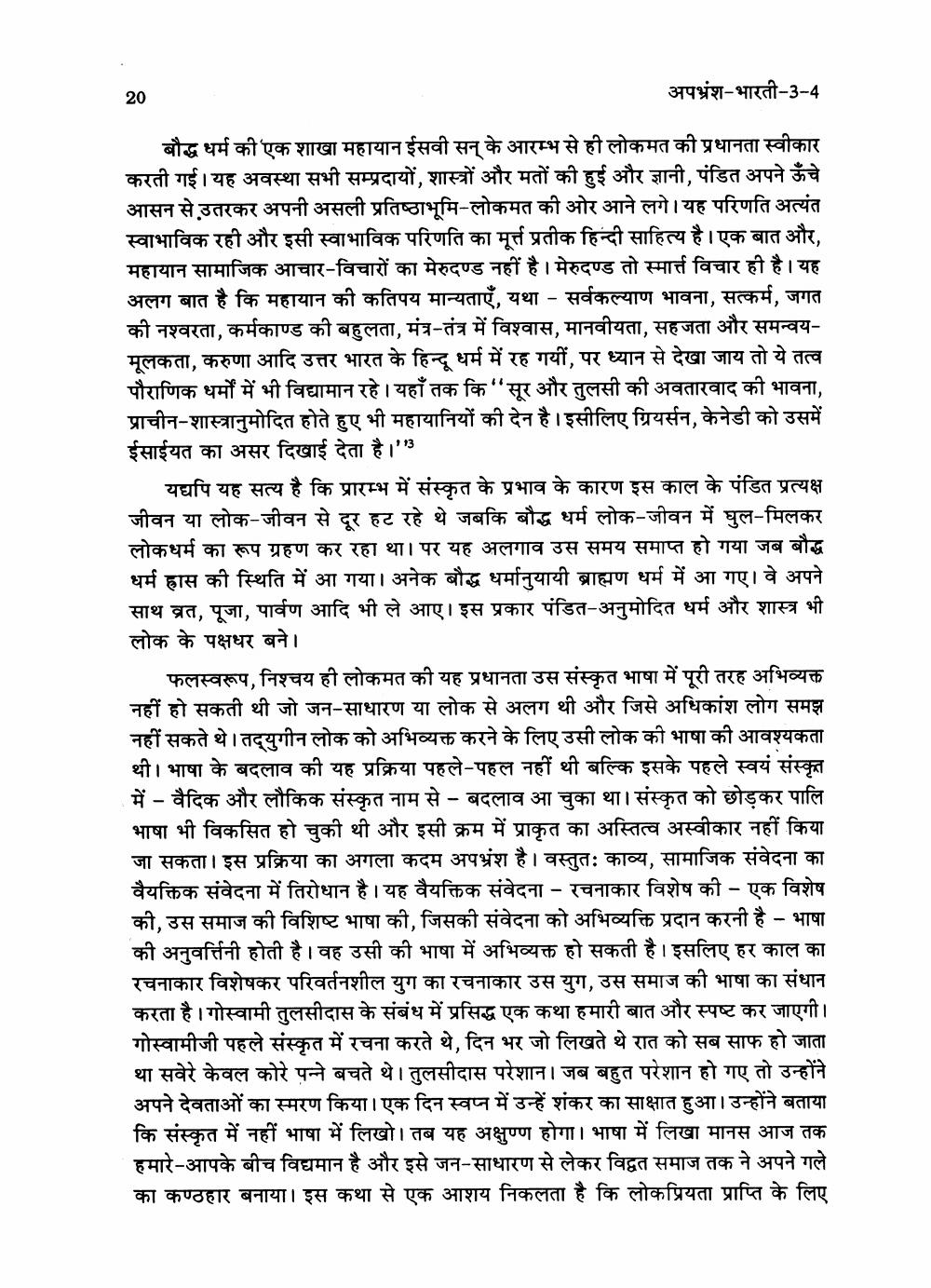________________
अपभ्रंश - भारती - 3-4
द्ध धर्म की एक शाखा महायान ईसवी सन् के आरम्भ से ही लोकमत की प्रधानता स्वीकार करती गई। यह अवस्था सभी सम्प्रदायों, शास्त्रों और मतों की हुई और ज्ञानी, पंडित अपने ऊँचे आसन से उतरकर अपनी असली प्रतिष्ठाभूमि-लोकमत की ओर आने लगे। यह परिणति अत्यंत स्वाभाविक रही और इसी स्वाभाविक परिणति का मूर्त प्रतीक हिन्दी साहित्य है । एक बात और, महायान सामाजिक आचार-विचारों का मेरुदण्ड नहीं है । मेरुदण्ड तो स्मार्त्त विचार ही है। यह अलग बात है कि महायान की कतिपय मान्यताएँ, यथा सर्वकल्याण भावना, सत्कर्म, जगत की नश्वरता, कर्मकाण्ड की बहुलता, मंत्र-तंत्र में विश्वास, मानवीयता, सहजता और समन्वयमूलकता, करुणा आदि उत्तर भारत के हिन्दू धर्म में रह गयीं, पर ध्यान से देखा जाय तो ये तत्व पौराणिक धर्मों में भी विद्यामान रहे । यहाँ तक कि "सूर और तुलसी की अवतारवाद की भावना, प्राचीन शास्त्रानुमोदित होते हुए भी महायानियों की देन है। इसीलिए ग्रियर्सन, केनेडी को उसमें ईसाईयत का असर दिखाई देता है।'
13
20
-
यद्यपि यह सत्य है कि प्रारम्भ में संस्कृत के प्रभाव के कारण इस काल के पंडित प्रत्यक्ष जीवन या लोक-जीवन से दूर हट रहे थे जबकि बौद्ध धर्म लोक-जीवन में घुल मिलकर लोकधर्म का रूप ग्रहण कर रहा था। पर यह अलगाव उस समय समाप्त हो गया जब बौद्ध धर्म ह्रास की स्थिति में आ गया। अनेक बौद्ध धर्मानुयायी ब्राह्मण धर्म में आ गए। वे अपने साथ व्रत, पूजा, पार्वण आदि भी ले आए। इस प्रकार पंडित - अनुमोदित धर्म और शास्त्र भी लोक के पक्षधर बने ।
-
--
फलस्वरूप, निश्चय ही लोकमत की यह प्रधानता उस संस्कृत भाषा में पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं हो सकती थी जो जन साधारण या लोक से अलग थी और जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं सकते थे। तद्युगीन लोक को अभिव्यक्त करने के लिए उसी लोक की भाषा की आवश्यकता थी । भाषा के बदलाव की यह प्रक्रिया पहले-पहल नहीं थी बल्कि इसके पहले स्वयं संस्कृत में - वैदिक और लौकिक संस्कृत नाम से बदलाव आ चुका था । संस्कृत को छोड़कर पालि भाषा भी विकसित हो चुकी थी और इसी क्रम में प्राकृत का अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया का अगला कदम अपभ्रंश है। वस्तुतः काव्य, सामाजिक संवेदना का वैयक्तिक संवेदना में तिरोधान है। यह वैयक्तिक संवेदना - रचनाकार विशेष की एक विशेष की, उस समाज की विशिष्ट भाषा की, जिसकी संवेदना को अभिव्यक्ति प्रदान करनी है - भाषा की अनुवर्त्तिनी होती है । वह उसी की भाषा में अभिव्यक्त हो सकती है। इसलिए हर काल का रचनाकार विशेषकर परिवर्तनशील युग का रचनाकार उस युग, उस समाज की भाषा का संधान करता है । गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में प्रसिद्ध एक कथा हमारी बात और स्पष्ट कर जाएगी । गोस्वामीजी पहले संस्कृत में रचना करते थे, दिन भर जो लिखते थे रात को सब साफ हो जाता था सवेरे केवल कोरे पन्ने बचते थे । तुलसीदास परेशान । जब बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने देवताओं का स्मरण किया। एक दिन स्वप्न में उन्हें शंकर का साक्षात हुआ। उन्होंने बताया कि संस्कृत में नहीं भाषा में लिखो । तब यह अक्षुण्ण होगा। भाषा में लिखा मानस आज तक हमारे-आपके बीच विद्यमान है और इसे जन-साधारण से लेकर विद्वत समाज तक ने अपने गले का कण्ठहार बनाया। इस कथा से एक आशय निकलता है कि लोकप्रियता प्राप्ति के लिए