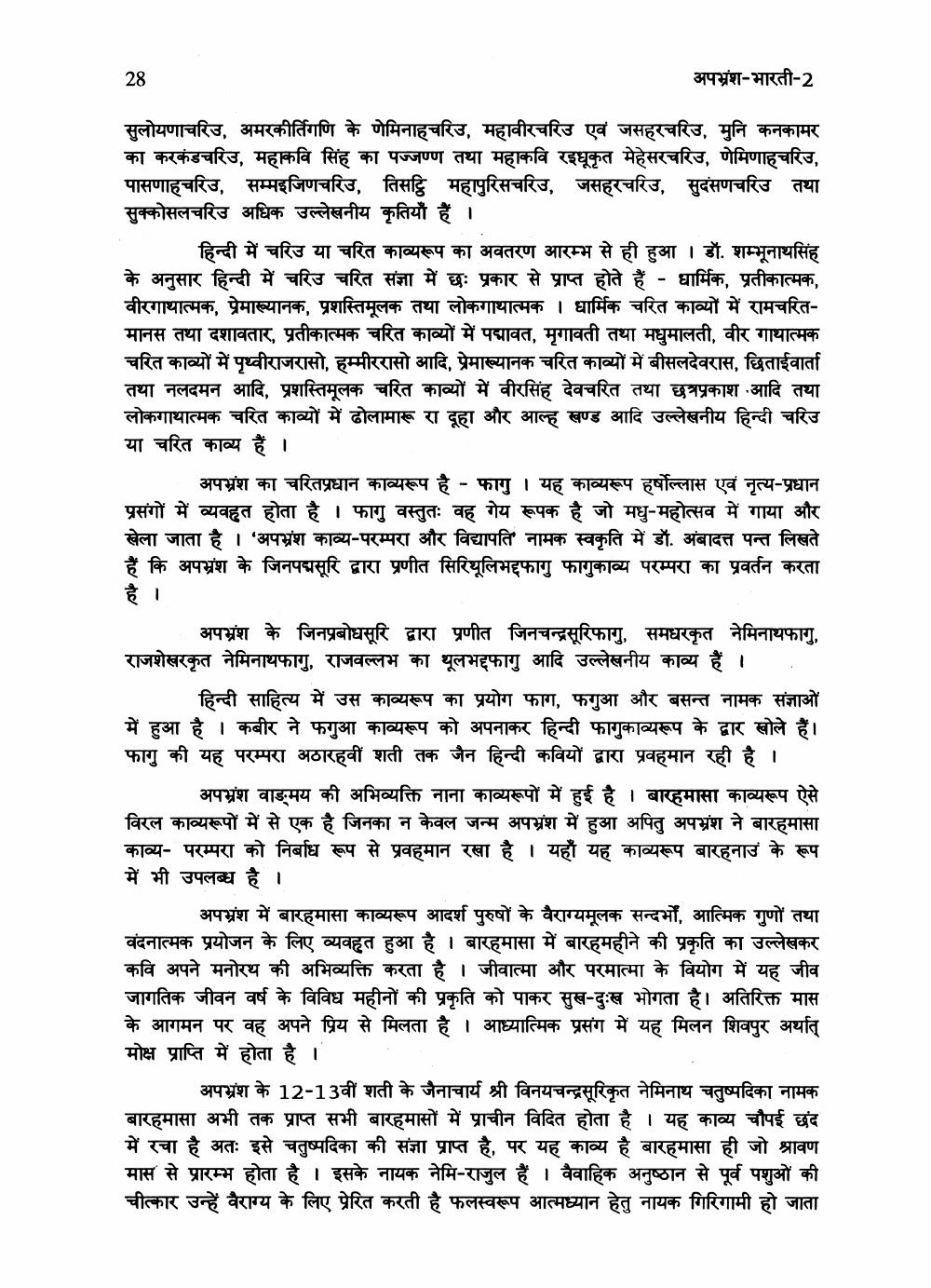________________
अपभ्रंश - भारती-2
सुलोयणाचरिउ, अमरकीर्तिगणि के णेमिनाहचरिउ, महावीरचरिउ एवं जसहरचरिउ, मुनि कनकामर का करकंडचरिउ, महाकवि सिंह का पज्जण्ण तथा महाकवि रइधूकृत मेहेसरचरिउ, णेमिणाहचरिउ, पासणाहचरिउ, सम्मइजिणचरिउ, तिसट्ठि महापुरिसचरिउ, जसहरचरिउ, सुदंसणचरिउ तथा सुक्कोसलचरिउ अधिक उल्लेखनीय कृतियाँ हैं ।
28
हिन्दी में चरिउ या चरित काव्यरूप का अवतरण आरम्भ से ही हुआ । डॉ. शम्भूनाथसिंह के अनुसार हिन्दी में चरिउ चरित संज्ञा में छः प्रकार से प्राप्त होते हैं धार्मिक, प्रतीकात्मक, वीरगाथात्मक, प्रेमाख्यानक, प्रशस्तिमूलक तथा लोकगाथात्मक । धार्मिक चरित काव्यों में रामचरित - मानस तथा दशावतार, प्रतीकात्मक चरित काव्यों में पद्मावत, मृगावती तथा मधुमालती, वीर गाथात्मक चरित काव्यों में पृथ्वीराजरासो, हम्मीररासो आदि, प्रेमाख्यानक चरित काव्यों में बीसलदेवरास, छिताईवार्ता तथा नलदमन आदि, प्रशस्तिमूलक चरित काव्यों में वीरसिंह देवचरित तथा छत्रप्रकाश आदि तथा लोकगाथात्मक चरित काव्यों में ढोलामारू रा दूहा और आल्ह खण्ड आदि उल्लेखनीय हिन्दी चरिउ या चरित काव्य हैं ।
-
अपभ्रंश का चरितप्रधान काव्यरूप है - फागु । यह काव्यरूप हर्षोल्लास एवं नृत्य - प्रधान प्रसंगों में व्यवहृत होता है । फागु वस्तुतः वह गेय रूपक है जो मधु-महोत्सव में गाया और खेला जाता है । 'अपभ्रंश काव्य-परम्परा और विद्यापति नामक स्वकृति में डॉ. अंबादत्त पन्त लिखते हैं कि अपभ्रंश के जिनपद्मसूरि द्वारा प्रणीत सिरिथूलिभद्दफागु फागुकाव्य परम्परा का प्रवर्तन करता है ।
अपभ्रंश के जिनप्रबोधसूरि द्वारा प्रणीत जिनचन्द्रसूरिफागु, समधरकृत नेमिनाथफागु, राजशेखरकृत नेमिनाथफागु, राजवल्लभ का थूलभद्दफागु आदि उल्लेखनीय काव्य हैं ।
हिन्दी साहित्य में उस काव्यरूप का प्रयोग फाग, फगुआ और बसन्त नामक संज्ञाओं में हुआ है । कबीर ने फगुआ काव्यरूप को अपनाकर हिन्दी फागुकाव्यरूप के द्वार खोले हैं। फागु की यह परम्परा अठारहवीं शती तक जैन हिन्दी कवियों द्वारा प्रवहमान रही है ।
अपभ्रंश वाङ्मय की अभिव्यक्ति नाना काव्यरूपों में हुई है । बारहमासा काव्यरूप ऐसे विरल काव्यरूपों में से एक है जिनका न केवल जन्म अपभ्रंश में हुआ अपितु अपभ्रंश ने बारहमासा काव्य- परम्परा को निर्बाध रूप से प्रवहमान रखा है । यहाँ यह काव्यरूप बारहनाउं के रूप में भी उपलब्ध है ।
अपभ्रंश में बारहमासा काव्यरूप आदर्श पुरुषों के वैराग्यमूलक सन्दर्भों, आत्मिक गुणों तथा वंदनात्मक प्रयोजन के लिए व्यवहुत हुआ है । बारहमासा में बारहमहीने की प्रकृति का उल्लेखकर कवि अपने मनोरथ की अभिव्यक्ति करता है । जीवात्मा और परमात्मा के वियोग में यह जीव जागतिक जीवन वर्ष के विविध महीनों की प्रकृति को पाकर सुख - दुःख भोगता है। अतिरिक्त मास के आगमन पर वह अपने प्रिय से मिलता है । आध्यात्मिक प्रसंग में यह मिलन शिवपुर अर्थात् मोक्ष प्राप्ति में होता है ।"
अपभ्रंश के 12-13वीं शती के जैनाचार्य श्री विनयचन्द्रसूरिकृत नेमिनाथ चतुष्पदिका नामक बारहमासा अभी तक प्राप्त सभी बारहमासों में प्राचीन विदित होता है । यह काव्य चौपई छंद में रचा है अतः इसे चतुष्पदिका की संज्ञा प्राप्त है, पर यह काव्य है बारहमासा ही जो श्रावण मास से प्रारम्भ होता है । इसके नायक नेमि - राजुल हैं । वैवाहिक अनुष्ठान से पूर्व पशुओं की चीत्कार उन्हें वैराग्य के लिए प्रेरित करती है फलस्वरूप आत्मध्यान हेतु नायक गिरिगामी हो जाता