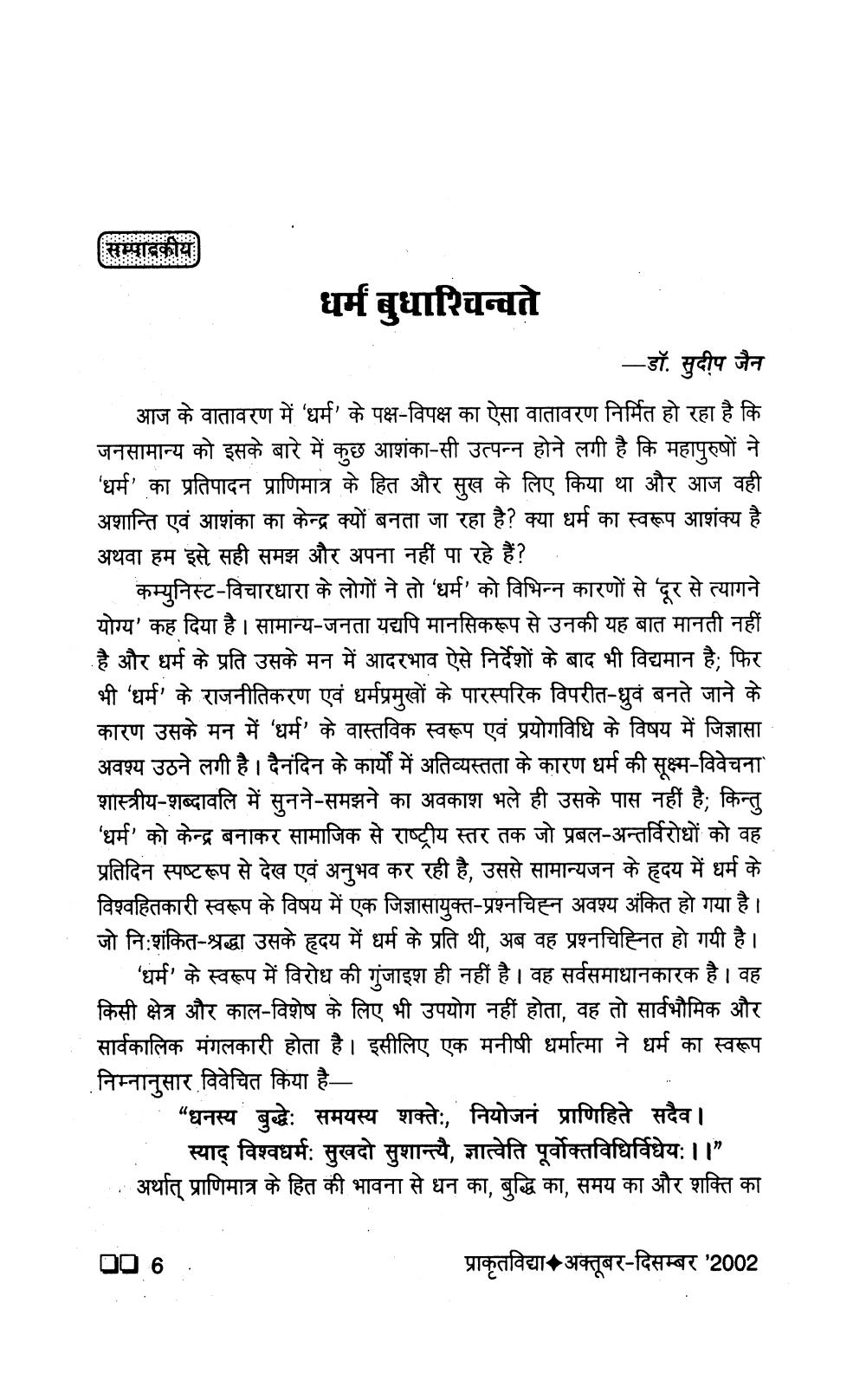________________
धर्मं बुधाश्चिन्वते
-डॉ. सुदीप जैन आज के वातावरण में 'धर्म' के पक्ष-विपक्ष का ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा है कि जनसामान्य को इसके बारे में कुछ आशंका-सी उत्पन्न होने लगी है कि महापुरुषों ने 'धर्म' का प्रतिपादन प्राणिमात्र के हित और सुख के लिए किया था और आज वही अशान्ति एवं आशंका का केन्द्र क्यों बनता जा रहा है? क्या धर्म का स्वरूप आशंक्य है अथवा हम इसे सही समझ और अपना नहीं पा रहे हैं?
कम्युनिस्ट-विचारधारा के लोगों ने तो 'धर्म' को विभिन्न कारणों से 'दूर से त्यागने योग्य' कह दिया है। सामान्य-जनता यद्यपि मानसिकरूप से उनकी यह बात मानती नहीं है और धर्म के प्रति उसके मन में आदरभाव ऐसे निर्देशों के बाद भी विद्यमान है; फिर भी 'धर्म' के राजनीतिकरण एवं धर्मप्रमुखों के पारस्परिक विपरीत-ध्रुवं बनते जाने के कारण उसके मन में 'धर्म' के वास्तविक स्वरूप एवं प्रयोगविधि के विषय में जिज्ञासा अवश्य उठने लगी है। दैनंदिन के कार्यों में अतिव्यस्तता के कारण धर्म की सूक्ष्म-विवेचना शास्त्रीय-शब्दावलि में सुनने-समझने का अवकाश भले ही उसके पास नहीं है; किन्तु 'धर्म' को केन्द्र बनाकर सामाजिक से राष्ट्रीय स्तर तक जो प्रबल-अन्तर्विरोधों को वह प्रतिदिन स्पष्टरूप से देख एवं अनुभव कर रही है, उससे सामान्यजन के हृदय में धर्म के विश्वहितकारी स्वरूप के विषय में एक जिज्ञासायुक्त-प्रश्नचिह्न अवश्य अंकित हो गया है। जो नि:शंकित-श्रद्धा उसके हृदय में धर्म के प्रति थी, अब वह प्रश्नचिह्नित हो गयी है।
'धर्म' के स्वरूप में विरोध की गुंजाइश ही नहीं है। वह सर्वसमाधानकारक है। वह किसी क्षेत्र और काल-विशेष के लिए भी उपयोग नहीं होता, वह तो सार्वभौमिक और सार्वकालिक मंगलकारी होता है। इसीलिए एक मनीषी धर्मात्मा ने धर्म का स्वरूप निम्नानुसार विवेचित किया है."धनस्य बुद्धेः समयस्य शक्ते:, नियोजनं प्राणिहिते सदैव ।
स्याद् विश्वधर्म: सुखदो सुशान्त्यै, ज्ञात्वेति पूर्वोक्तविधिविधेय: ।।” अर्थात् प्राणिमात्र के हित की भावना से धन का, बुद्धि का, समय का और शक्ति का
006 .
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2002