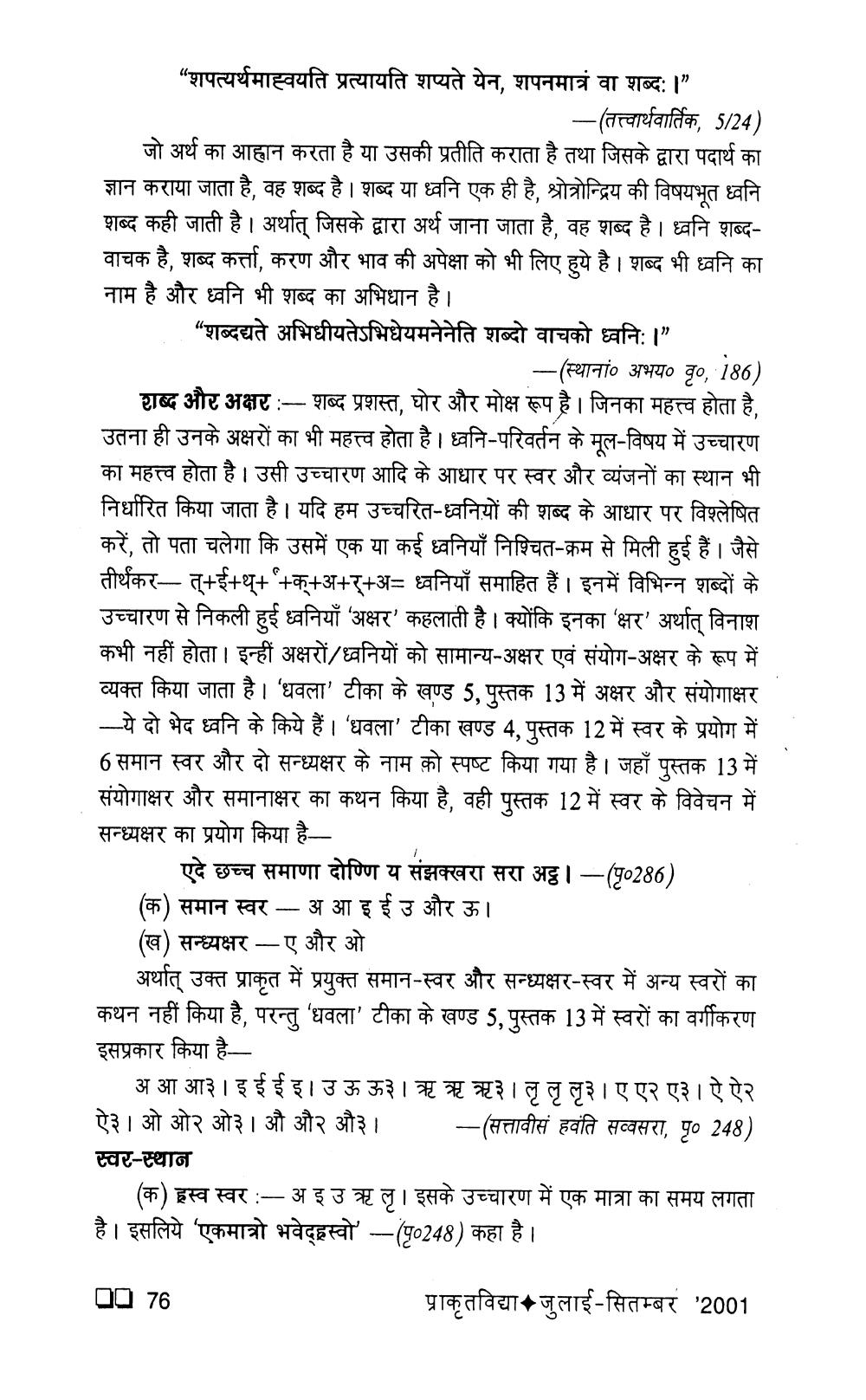________________
“शपत्यर्थमाह्वयति प्रत्यायति शप्यते येन, शपनमात्रं वा शब्द: । ”
- ( तत्त्वार्थवार्तिक, 5/24 ) अर्थ का आह्वान करता है या उसकी प्रतीति कराता है तथा जिसके द्वारा पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है, वह शब्द है । शब्द या ध्वनि एक ही है, श्रोत्रोन्द्रिय की विषयभूत ध्वनि शब्द कही जाती है। अर्थात् जिसके द्वारा अर्थ जाना जाता है, वह शब्द है । ध्वनि शब्दवाचक है, शब्द कर्ता, करण और भाव की अपेक्षा को भी लिए हुये है । शब्द भी ध्वनि का नाम है और ध्वनि भी शब्द का अभिधान है 1
“शब्दद्यते अभिधीयतेऽभिधेयमनेनेति शब्दो वाचको ध्वनिः । "
1
— (स्थानां० अभय० वृ०, 186 ) शब्द और अक्षर • शब्द प्रशस्त, घोर और मोक्ष रूप है। जिनका महत्त्व होता है, उतना ही उनके अक्षरों का भी महत्त्व होता है। ध्वनि - परिवर्तन के मूल विषय में उच्चारण का महत्त्व होता है । उसी उच्चारण आदि के आधार पर स्वर और व्यंजनों का स्थान भी निर्धारित किया जाता है । यदि हम उच्चरित - ध्वनियों की शब्द के आधार पर विश्लेषित करें, तो पता चलेगा कि उसमें एक या कई ध्वनियाँ निश्चित - क्रम से मिली हुई हैं । जैसे तीर्थंकर – त् + ई + थ् + + क् + अ + र् + अ = ध्वनियाँ समाहित हैं । इनमें विभिन्न शब्दों के उच्चारण से निकली हुई ध्वनियाँ 'अक्षर' कहलाती है। क्योंकि इनका 'क्षर' अर्थात् विनाश कभी नहीं होता। इन्हीं अक्षरों / ध्वनियों को सामान्य - अक्षर एवं संयोग - अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है । 'धवला' टीका के खण्ड 5, पुस्तक 13 में अक्षर और संयोगाक्षर — ये दो भेद ध्वनि के किये हैं। 'धवला' टीका खण्ड 4, पुस्तक 12 में स्वर के प्रयोग में 6 समान स्वर और दो सन्ध्यक्षर के नाम को स्पष्ट किया गया है। जहाँ पुस्तक 13 में संयोगाक्षर और समानाक्षर का कथन किया है, वही पुस्तक 12 में स्वर के विवेचन में सन्ध्यक्षर का प्रयोग किया है
एदे छच्च समाणा दोण्णि य संझक्खरा सरा अट्ठ। – ( पृ०286)
(क) समान स्वर अ आ इ ई उ और ऊ ।
(ख) सन्ध्यक्षर
अर्थात् उक्त प्राकृत में प्रयुक्त समान - स्वर और सन्ध्यक्षर -स्वर में अन्य स्वरों का कथन नहीं किया है, परन्तु 'धवला' टीका के खण्ड 5, पुस्तक 13 में स्वरों का वर्गीकरण इसप्रकार किया है
―
0076
- ए और ओ
अ आ आ३ । इ ई ई इ । उ ऊ ऊ३। ऋ ऋ ऋ३। लृ लृ लृ३ । ए ए२ ए३ । ऐ ऐ२ ऐ३ । ओ ओर ओ३ । औ और औ३ । - ( सत्तावीसं हवंति सव्वसरा, पृ० 248 )
I
स्वर - स्थान
(क) ह्रस्व स्वर :- अ इ उ ऋ लृ । इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसलिये ‘एकमात्रो भवेद्वस्वो' – ( पृ०248) कहा है
1
प्राकृतविद्या• जुलाई-सितम्बर 2001