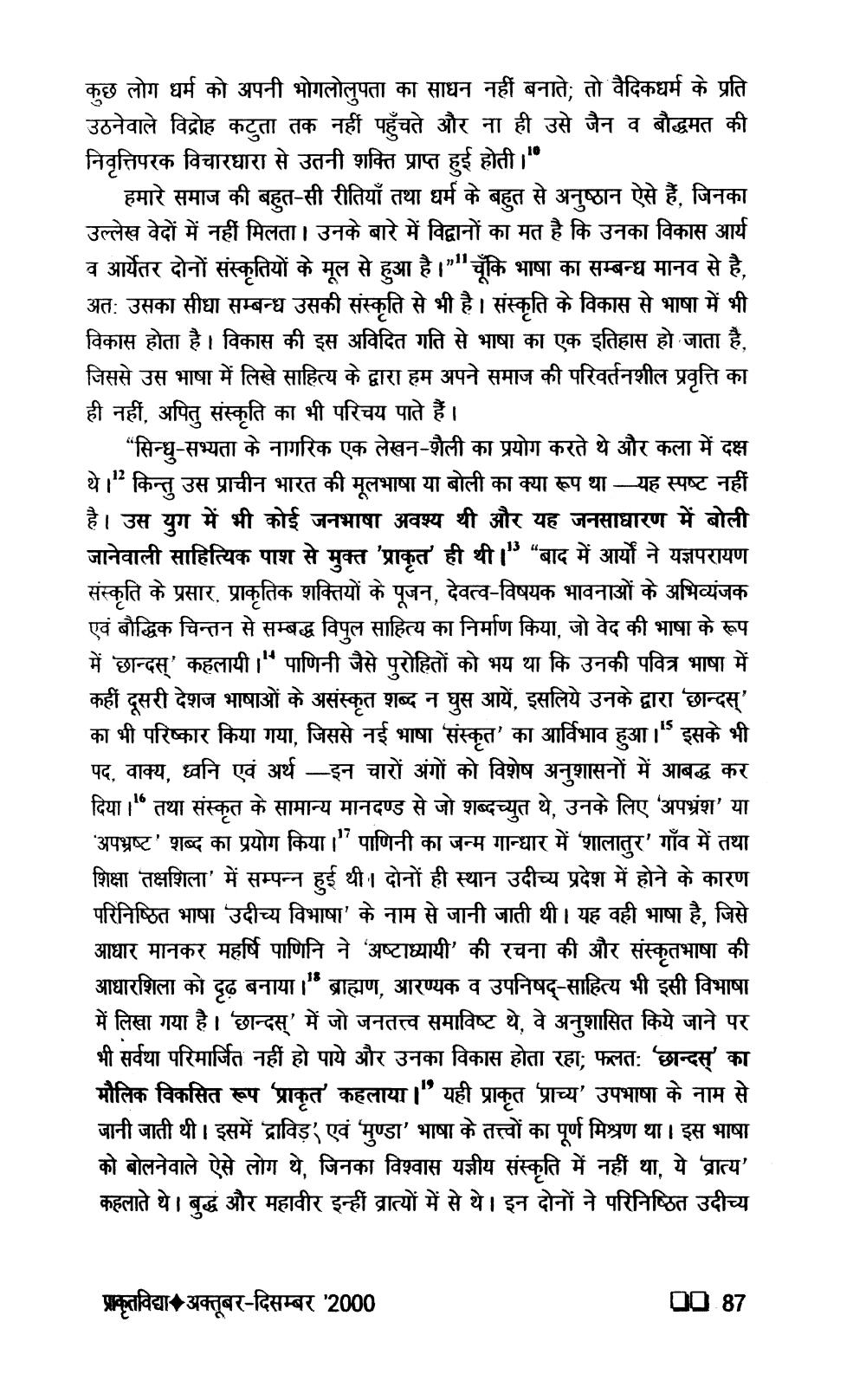________________
कुछ लोग धर्म को अपनी भोगलोलुपता का साधन नहीं बनाते; तो वैदिकधर्म के प्रति उठनेवाले विद्रोह कटुता तक नहीं पहुँचते और ना ही उसे जैन व बौद्धमत की निवृत्तिपरक विचारधारा से उतनी शक्ति प्राप्त हुई होती।"
हमारे समाज की बहुत-सी रीतियाँ तथा धर्म के बहुत से अनुष्ठान ऐसे हैं, जिनका उल्लेख वेदों में नहीं मिलता। उनके बारे में विद्वानों का मत है कि उनका विकास आर्य व आर्येतर दोनों संस्कृतियों के मूल से हुआ है।"" चूँकि भाषा का सम्बन्ध मानव से है, अत: उसका सीधा सम्बन्ध उसकी संस्कृति से भी है । संस्कृति के विकास से भाषा में भी विकास होता है । विकास की इस अविदित गति से भाषा का एक इतिहास हो जाता है, जिससे उस भाषा में लिखे साहित्य के द्वारा हम अपने समाज की परिवर्तनशील प्रवृत्ति का ही नहीं, अपितु संस्कृति का भी परिचय पाते हैं।
1
“सिन्धु सभ्यता के नागरिक एक लेखन - शैली का प्रयोग करते थे और कला में दक्ष थे।” किन्तु उस प्राचीन भारत की मूलभाषा या बोली का क्या रूप था —यह स्पष्ट नहीं है । उस युग में भी कोई जनभाषा अवश्य थी और यह जनसाधारण में बोली जानेवाली साहित्यिक पाश से मुक्त 'प्राकृत' ही थी ।" “बाद में आर्यों ने यज्ञपरायण संस्कृति के प्रसार, प्राकृतिक शक्तियों के पूजन, देवत्व - विषयक भावनाओं के अभिव्यंजक एवं बौद्धिक चिन्तन से सम्बद्ध विपुल साहित्य का निर्माण किया, जो वेद की भाषा के रूप में 'छान्दस्' कहलायी।" पाणिनी जैसे पुरोहितों को भय था कि उनकी पवित्र भाषा में कहीं दूसरी देशज भाषाओं के असंस्कृत शब्द न घुस आयें, इसलिये उनके द्वारा 'छान्दस्’ का भी परिष्कार किया गया, जिससे नई भाषा 'संस्कृत' का आर्विभाव हुआ ।" इसके भी पद, वाक्य, ध्वनि एवं अर्थ – इन चारों अंगों को विशेष अनुशासनों में आबद्ध कर दिया । " तथा संस्कृत के सामान्य मानदण्ड से जो शब्दच्युत थे, उनके लिए 'अपभ्रंश' या 'अपभ्रष्ट' शब्द का प्रयोग किया ।” पाणिनी का जन्म गान्धार में 'शालातुर' गाँव में तथा शिक्षा 'तक्षशिला' में सम्पन्न हुई थी । दोनों ही स्थान उदीच्य प्रदेश में होने के कारण परिनिष्ठित भाषा 'उदीच्य विभाषा' के नाम से जानी जाती थी । यह वही भाषा है, जिसे आधार मानकर महर्षि पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' की रचना की और संस्कृतभाषा की आधारशिला को दृढ़ बनाया। " ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद् - साहित्य भी इसी विभाषा में लिखा गया है। ‘छान्दस्' में जो जनतत्त्व समाविष्ट थे, वे अनुशासित किये जाने पर भी सर्वथा परिमार्जित नहीं हो पाये और उनका विकास होता रहा; फलत: 'छान्दस्' का मौलिक विकसित रूप 'प्राकृत' कहलाया ।" यही प्राकृत 'प्राच्य' उपभाषा के नाम से जानी जाती थी। इसमें 'द्राविड़' एवं 'मुण्डा' भाषा के तत्त्वों का पूर्ण मिश्रण था । इस भाषा को बोलनेवाले ऐसे लोग थे, जिनका विश्वास यज्ञीय संस्कृति में नहीं था, ये 'व्रात्य' कहलाते थे। बुद्ध और महावीर इन्हीं व्रात्यों में से थे । इन दोनों ने परिनिष्ठित उदीच्य
प्राकृतविद्या + अक्तूबर-दिसम्बर 2000
00 87