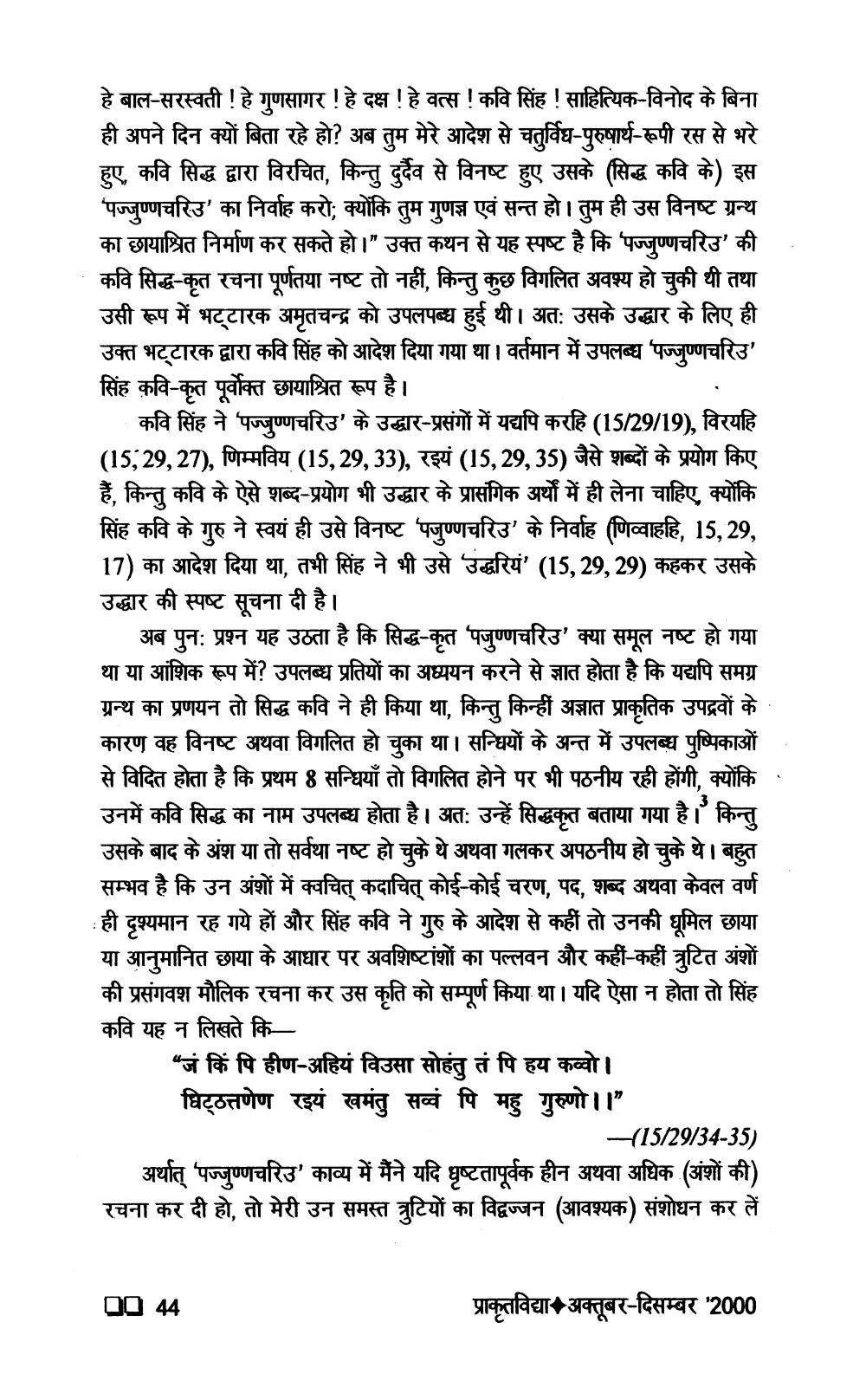________________
हे बाल-सरस्वती ! हे गुणसागर ! हे दक्ष ! हे वत्स ! कवि सिंह ! साहित्यिक-विनोद के बिना ही अपने दिन क्यों बिता रहे हो? अब तुम मेरे आदेश से चतुर्विध-पुरुषार्थ-रूपी रस से भरे हुए, कवि सिद्ध द्वारा विरचित, किन्तु दुर्दैव से विनष्ट हुए उसके (सिद्ध कवि के) इस 'पज्जुण्णचरिउ' का निर्वाह करो; क्योंकि तुम गुणज्ञ एवं सन्त हो। तुम ही उस विनष्ट ग्रन्थ का छायाश्रित निर्माण कर सकते हो।” उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि 'पज्जुण्णचरिउ' की कवि सिद्ध-कृत रचना पूर्णतया नष्ट तो नहीं, किन्तु कुछ विगलित अवश्य हो चुकी थी तथा उसी रूप में भट्टारक अमृतचन्द्र को उपलपब्ध हुई थी। अत: उसके उद्धार के लिए ही उक्त भट्टारक द्वारा कवि सिंह को आदेश दिया गया था। वर्तमान में उपलब्ध पज्जुण्णचरिउ' सिंह कवि-कृत पूर्वोक्त छायाश्रित रूप है।
कवि सिंह ने 'पज्जुण्णचरिउ' के उद्धार-प्रसंगों में यद्यपि करहि (15729/19), विरयहि (15,29,27), णिम्मविय (15,29,33), रइयं (15,29,35) जैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं, किन्तु कवि के ऐसे शब्द-प्रयोग भी उद्धार के प्रासंगिक अर्थों में ही लेना चाहिए. क्योंकि सिंह कवि के गुरु ने स्वयं ही उसे विनष्ट पजुण्णचरिउ' के निर्वाह (णिव्वाहहि, 15,29, 17) का आदेश दिया था, तभी सिंह ने भी उसे उद्धरियं' (15,29,29) कहकर उसके उद्धार की स्पष्ट सूचना दी है। __ अब पुन: प्रश्न यह उठता है कि सिद्ध-कृत 'पजुण्णचरिउ' क्या समूल नष्ट हो गया था या आंशिक रूप में? उपलब्ध प्रतियों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यद्यपि समग्र ग्रन्थ का प्रणयन तो सिद्ध कवि ने ही किया था, किन्तु किन्हीं अज्ञात प्राकृतिक उपद्रवों के कारण वह विनष्ट अथवा विगलित हो चुका था। सन्धियों के अन्त में उपलब्ध पुष्पिकाओं से विदित होता है कि प्रथम 8 सन्धियाँ तो विगलित होने पर भी पठनीय रही होंगी, क्योंकि । उनमें कवि सिद्ध का नाम उपलब्ध होता है। अत: उन्हें सिद्धकृत बताया गया है। किन्तु उसके बाद के अंश या तो सर्वथा नष्ट हो चुके थे अथवा गलकर अपठनीय हो चुके थे। बहुत सम्भव है कि उन अंशों में क्वचित् कदाचित् कोई-कोई चरण, पद, शब्द अथवा केवल वर्ण ही दृश्यमान रह गये हों और सिंह कवि ने गुरु के आदेश से कहीं तो उनकी धूमिल छाया या आनुमानित छाया के आधार पर अवशिष्टांशों का पल्लवन और कहीं-कहीं त्रुटित अंशों की प्रसंगवश मौलिक रचना कर उस कृति को सम्पूर्ण किया था। यदि ऐसा न होता तो सिंह कवि यह न लिखते कि
“जं किं पि हीण-अहियं विउसा सोहंतु तं पि हय कव्वो। घिट्टत्तणेण रइयं खमंतु सव्वं पि महु गुरुणो।।"
–(15/29/34-35) अर्थात् 'पज्जुण्णचरिउ' काव्य में मैंने यदि धृष्टतापूर्वक हीन अथवा अधिक (अंशों की) रचना कर दी हो, तो मेरी उन समस्त त्रुटियों का विद्वज्जन (आवश्यक) संशोधन कर लें
0044
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2000