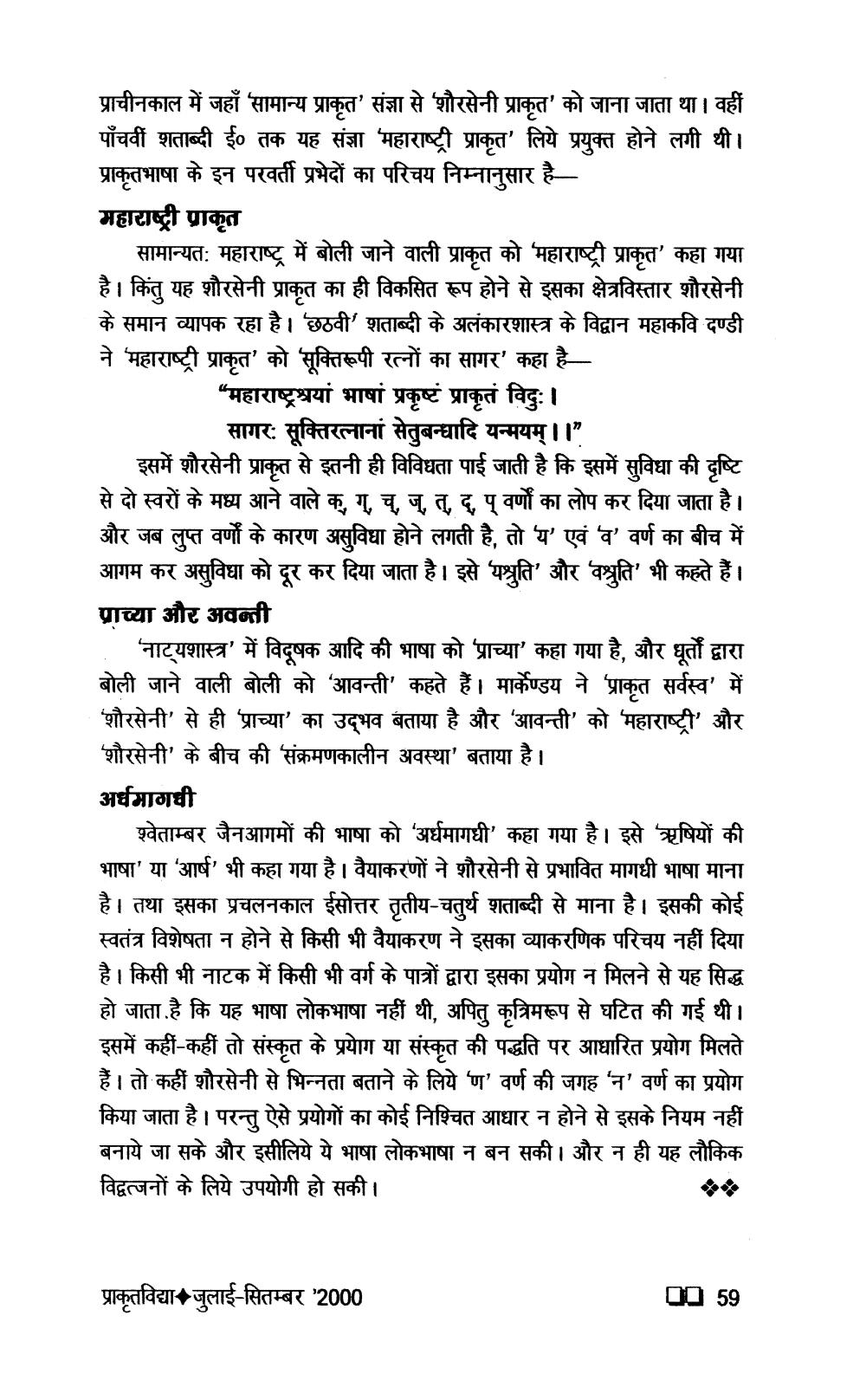________________
प्राचीनकाल में जहाँ 'सामान्य प्राकृत' संज्ञा से 'शौरसेनी प्राकृत' को जाना जाता था। वहीं पाँचवीं शताब्दी ई० तक यह संज्ञा 'महाराष्ट्री प्राकृत' लिये प्रयुक्त होने लगी थी। प्राकृतभाषा के इन परवर्ती प्रभेदों का परिचय निम्नानुसार हैमहाराष्ट्री प्राकृत
सामान्यत: महाराष्ट्र में बोली जाने वाली प्राकृत को 'महाराष्ट्री प्राकृत' कहा गया है। किंतु यह शौरसेनी प्राकृत का ही विकसित रूप होने से इसका क्षेत्रविस्तार शौरसेनी के समान व्यापक रहा है। 'छठवी' शताब्दी के अलंकारशास्त्र के विद्वान महाकवि दण्डी ने महाराष्ट्री प्राकृत' को 'सूक्तिरूपी रत्नों का सागर' कहा है—
"महाराष्ट्रश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः ।
सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम् ।।" इसमें शौरसेनी प्राकृत से इतनी ही विविधता पाई जाती है कि इसमें सुविधा की दृष्टि से दो स्वरों के मध्य आने वाले क्, ग, च्, ज्, त्, द, प् वर्णों का लोप कर दिया जाता है। और जब लुप्त वर्णों के कारण असुविधा होने लगती है, तो 'य' एवं 'व' वर्ण का बीच में आगम कर असुविधा को दूर कर दिया जाता है। इसे 'यश्रुति' और 'वश्रुति' भी कहते हैं। प्राच्या और अवन्ती
'नाट्यशास्त्र' में विदूषक आदि की भाषा को 'प्राच्या' कहा गया है, और धूर्तों द्वारा बोली जाने वाली बोली को 'आवन्ती' कहते हैं। मार्केण्डय ने 'प्राकृत सर्वस्व' में 'शौरसेनी' से ही प्राच्या' का उद्भव बताया है और 'आवन्ती' को 'महाराष्ट्री' और 'शौरसेनी' के बीच की संक्रमणकालीन अवस्था' बताया है। अर्धमागधी
श्वेताम्बर जैनआगमों की भाषा को 'अर्धमागधी' कहा गया है। इसे 'ऋषियों की भाषा' या 'आर्ष' भी कहा गया है। वैयाकरणों ने शौरसेनी से प्रभावित मागधी भाषा माना है। तथा इसका प्रचलनकाल ईसोत्तर तृतीय-चतुर्थ शताब्दी से माना है। इसकी कोई स्वतंत्र विशेषता न होने से किसी भी वैयाकरण ने इसका व्याकरणिक परिचय नहीं दिया है। किसी भी नाटक में किसी भी वर्ग के पात्रों द्वारा इसका प्रयोग न मिलने से यह सिद्ध हो जाता है कि यह भाषा लोकभाषा नहीं थी, अपितु कृत्रिमरूप से घटित की गई थी। इसमें कहीं-कहीं तो संस्कृत के प्रयोग या संस्कृत की पद्धति पर आधारित प्रयोग मिलते हैं। तो कहीं शौरसेनी से भिन्नता बताने के लिये 'ण' वर्ण की जगह 'न' वर्ण का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ऐसे प्रयोगों का कोई निश्चित आधार न होने से इसके नियम नहीं बनाये जा सके और इसीलिये ये भाषा लोकभाषा न बन सकी। और न ही यह लौकिक विद्वत्जनों के लिये उपयोगी हो सकी।
प्राकृतविद्या जुलाई-सितम्बर '2000
1059