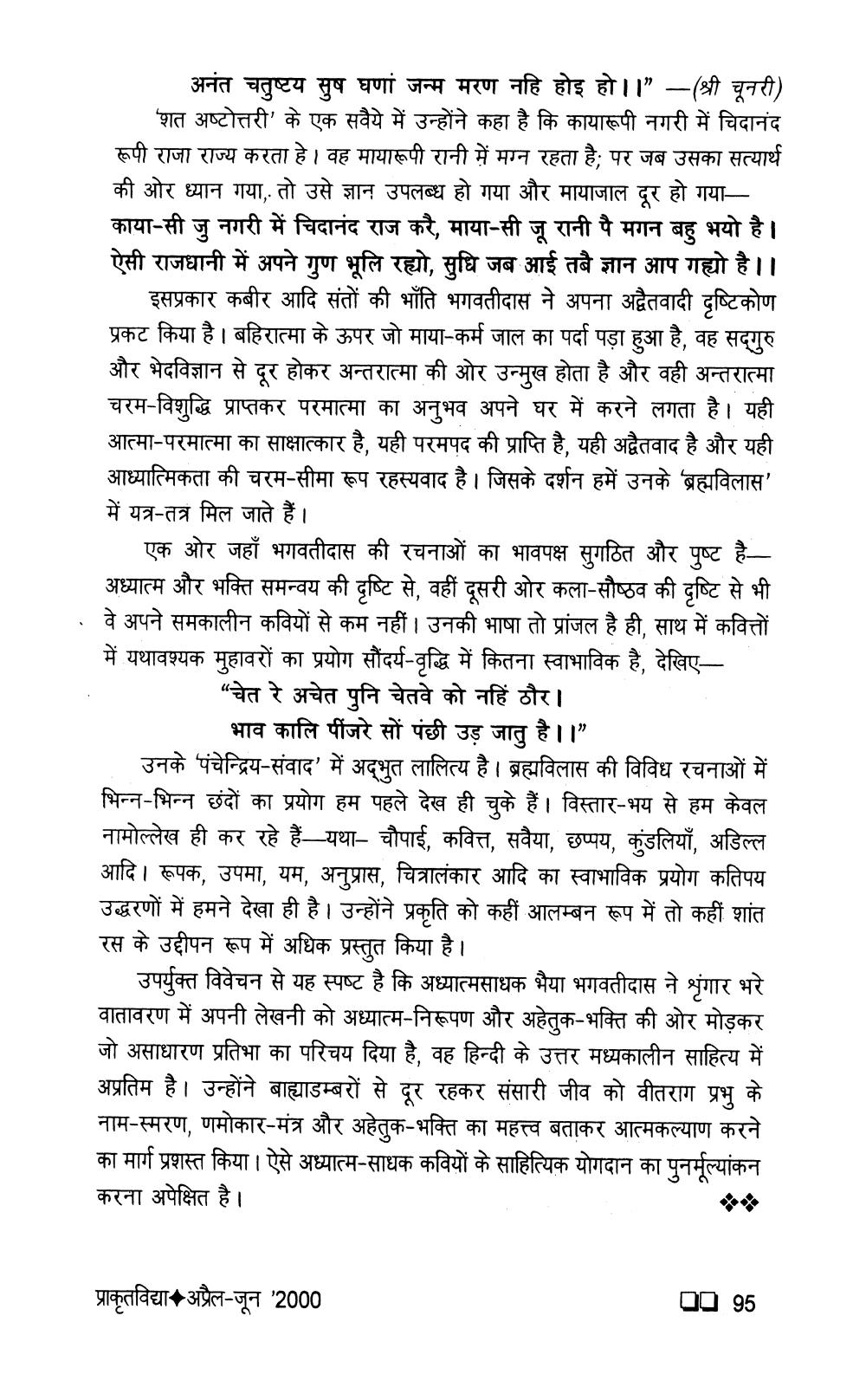________________
अनंत चतुष्टय सुष घणां जन्म मरण नहि होइ हो।।" – (श्री चूनरी) ‘शत अष्टोत्तरी' के एक सवैये में उन्होंने कहा है कि कायारूपी नगरी में चिदानंद रूपी राजा राज्य करता है। वह मायारूपी रानी में मग्न रहता है; पर जब उसका सत्यार्थ की ओर ध्यान गया, तो उसे ज्ञान उपलब्ध हो गया और मायाजाल दूर हो गयाकाया-सी जु नगरी में चिदानंद राज करै, माया-सी जू रानी पै मगन बहु भयो है। ऐसी राजधानी में अपने गुण भूलि रह्यो, सुधि जब आई तबै ज्ञान आप गह्यो है।।
इसप्रकार कबीर आदि संतों की भाँति भगवतीदास ने अपना अद्वैतवादी दृष्टिकोण प्रकट किया है। बहिरात्मा के ऊपर जो माया-कर्म जाल का पर्दा पड़ा हुआ है, वह सद्गुरु और भेदविज्ञान से दूर होकर अन्तरात्मा की ओर उन्मुख होता है और वही अन्तरात्मा चरम-विशुद्धि प्राप्तकर परमात्मा का अनुभव अपने घर में करने लगता है। यही आत्मा-परमात्मा का साक्षात्कार है, यही परमपद की प्राप्ति है, यही अद्वैतवाद है और यही आध्यात्मिकता की चरम-सीमा रूप रहस्यवाद है। जिसके दर्शन हमें उनके ब्रह्मविलास' में यत्र-तत्र मिल जाते हैं।
एक ओर जहाँ भगवतीदास की रचनाओं का भावपक्ष सुगठित और पुष्ट हैअध्यात्म और भक्ति समन्वय की दृष्टि से, वहीं दूसरी ओर कला-सौष्ठव की दृष्टि से भी वे अपने समकालीन कवियों से कम नहीं। उनकी भाषा तो प्रांजल है ही, साथ में कवित्तों में यथावश्यक मुहावरों का प्रयोग सौंदर्य-वृद्धि में कितना स्वाभाविक है, देखिए
“चेत रे अचेत पुनि चेतवे को नहिं ठौर ।
भाव कालि पींजरे सों पंछी उड़ जातु है।।" उनके पंचेन्द्रिय-संवाद' में अद्भुत लालित्य है। ब्रह्मविलास की विविध रचनाओं में भिन्न-भिन्न छंदों का प्रयोग हम पहले देख ही चुके हैं। विस्तार-भय से हम केवल नामोल्लेख ही कर रहे हैं—यथा- चौपाई, कवित्त, सवैया, छप्पय, कुंडलियाँ, अडिल्ल आदि। रूपक, उपमा, यम, अनुप्रास, चित्रालंकार आदि का स्वाभाविक प्रयोग कतिपय उद्धरणों में हमने देखा ही है। उन्होंने प्रकृति को कहीं आलम्बन रूप में तो कहीं शांत रस के उद्दीपन रूप में अधिक प्रस्तुत किया है। __ उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अध्यात्मसाधक भैया भगवतीदास ने शृंगार भरे वातावरण में अपनी लेखनी को अध्यात्म-निरूपण और अहेतुक-भक्ति की ओर मोड़कर जो असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है, वह हिन्दी के उत्तर मध्यकालीन साहित्य में अप्रतिम है। उन्होंने बाह्याडम्बरों से दूर रहकर संसारी जीव को वीतराग प्रभु के नाम-स्मरण, णमोकार-मंत्र और अहेतुक-भक्ति का महत्त्व बताकर आत्मकल्याण करने का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे अध्यात्म-साधक कवियों के साहित्यिक योगदान का पुनर्मूल्यांकन करना अपेक्षित है।
प्राकृतविद्या अप्रैल-जून '2000
00 95