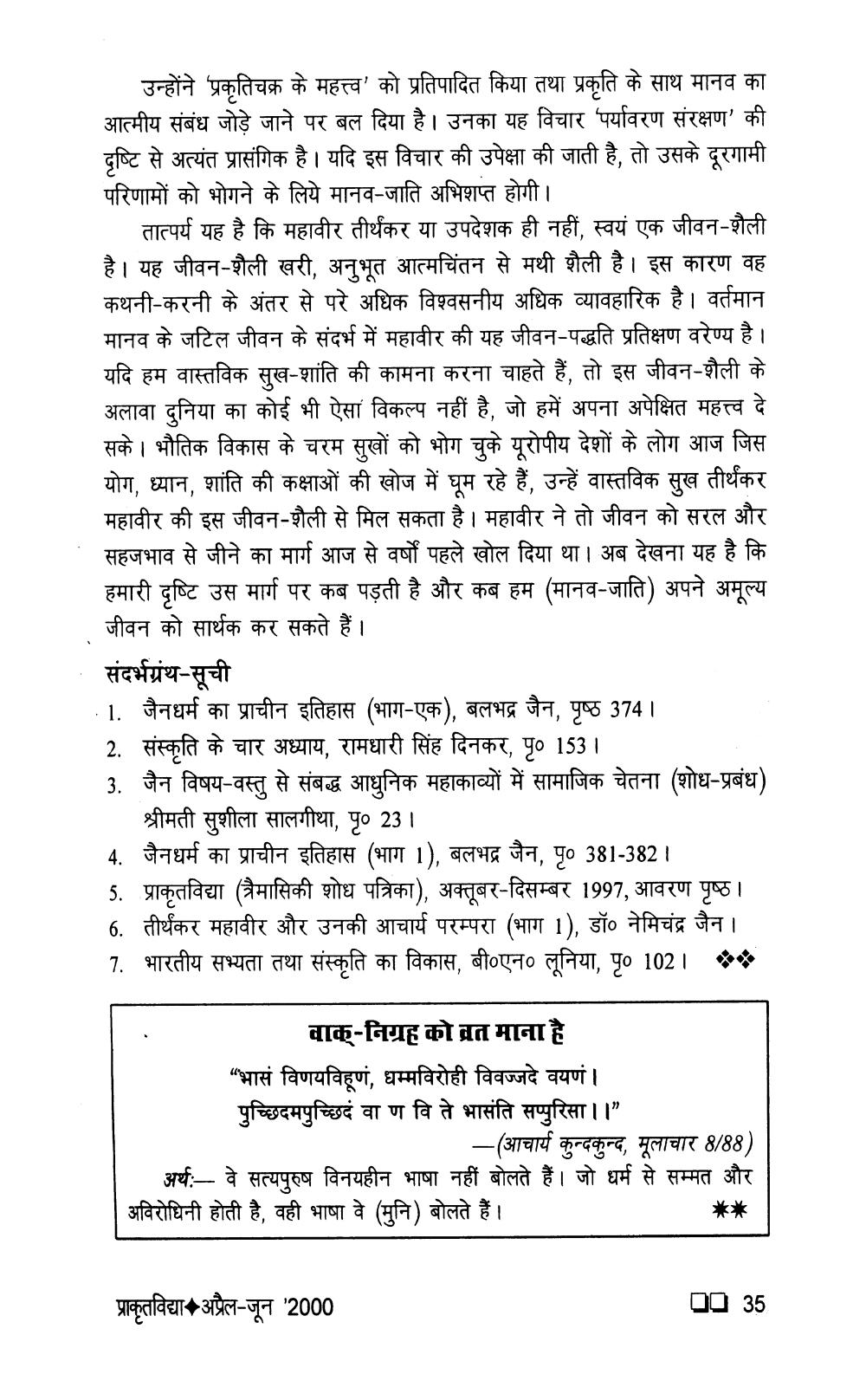________________
उन्होंने 'प्रकृतिचक्र के महत्त्व' को प्रतिपादित किया तथा प्रकृति के साथ मानव का आत्मीय संबंध जोड़े जाने पर बल दिया है। उनका यह विचार 'पर्यावरण संरक्षण' की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है । यदि इस विचार की उपेक्षा की जाती है, तो उसके दूरगामी परिणामों को भोगने के लिये मानव-जाति अभिशप्त होगी ।
तात्पर्य यह है कि महावीर तीर्थंकर या उपदेशक ही नहीं, स्वयं एक जीवन-शैली है। यह जीवन-शैली खरी, अनुभूत आत्मचिंतन से मथी शैली है । इस कारण वह कथनी-करनी के अंतर से परे अधिक विश्वसनीय अधिक व्यावहारिक है । वर्तमान मानव के जटिल जीवन के संदर्भ में महावीर की यह जीवन-पद्धति प्रतिक्षण वरेण्य है। यदि हम वास्तविक सुख-शांति की कामना करना चाहते हैं, तो इस जीवन-शैली के अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है, जो हमें अपना अपेक्षित महत्त्व दे सके। भौतिक विकास के चरम सुखों को भोग चुके यूरोपीय देशों के लोग आज जिस योग, ध्यान, शांति की कक्षाओं की खोज में घूम रहे हैं, उन्हें वास्तविक सुख तीर्थंकर महावीर की इस जीवन-शैली से मिल सकता है। महावीर ने तो जीवन को सरल और सहजभाव से जीने का मार्ग आज से वर्षों पहले खोल दिया था । अब देखना यह है कि हमारी दृष्टि उस मार्ग पर कब पड़ती है और कब हम (मानव-जाति) अपने अमूल्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं ।
संदर्भग्रंथ सूची
1. जैन धर्म का प्राचीन इतिहास (भाग - एक ), बलभद्र जैन, पृष्ठ 374।
2. संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, पृ० 153 ।
3. जैन विषय-वस्तु से संबद्ध आधुनिक महाकाव्यों में सामाजिक चेतना (शोध-प्रबंध) श्रीमती सुशीला सालगीथा, पृ० 23 1
4. जैनधर्म का प्राचीन इतिहास ( भाग 1 ), बलभद्र जैन, पृ० 381-382।
5. प्राकृतविद्या (त्रैमासिकी शोध पत्रिका), अक्तूबर-दिसम्बर 1997, आवरण पृष्ठ। 6. तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा ( भाग 1 ), डॉ० नेमिचंद्र जैन । 7. भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, बी०एन० लूनिया, पृ० 102 |
वाक्-निग्रह को व्रत माना है
“भासं विणयविहूणं, धम्मविरोही विवज्जदे वयणं । पुच्छिदमपुच्छिदं वा ण वि ते भासति सप्पुरिसा । ।"
- ( आचार्य कुन्दकुन्द, मूलाचार 8/88 ) अर्थ:- वे सत्यपुरुष विनयहीन भाषा नहीं बोलते हैं । जो धर्म से सम्मत और अविरोधिनी होती है, वही भाषा वे (मुनि) बोलते हैं।
**
प्राकृतविद्या + अप्रैल-जून 2000
35