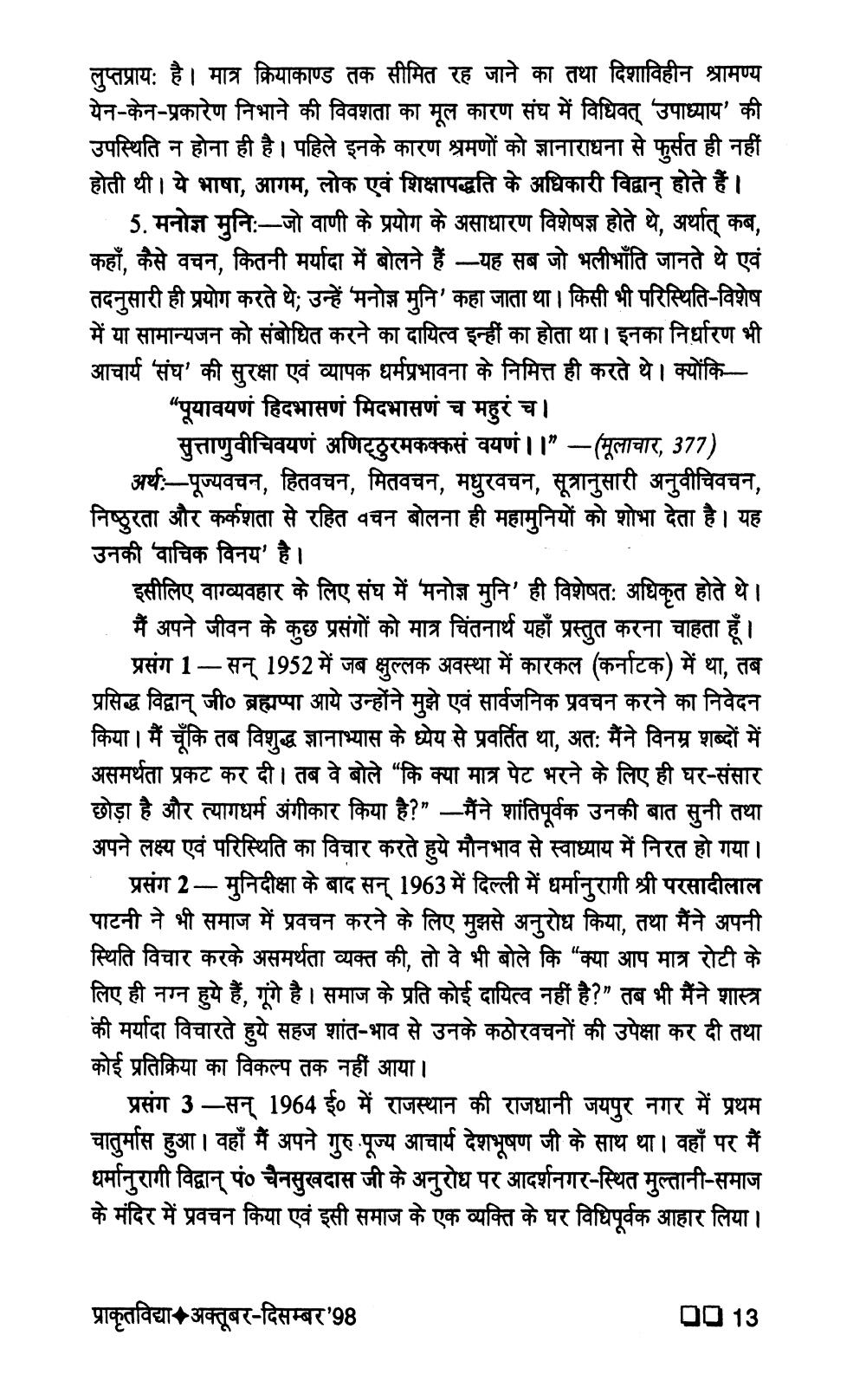________________
लुप्तप्राय: है। मात्र क्रियाकाण्ड तक सीमित रह जाने का तथा दिशाविहीन श्रामण्य येन-केन-प्रकारेण निभाने की विवशता का मूल कारण संघ में विधिवत् उपाध्याय' की उपस्थिति न होना ही है। पहिले इनके कारण श्रमणों को ज्ञानाराधना से फुर्सत ही नहीं होती थी। ये भाषा, आगम, लोक एवं शिक्षापद्धति के अधिकारी विद्वान् होते हैं।
5. मनोज्ञ मुनि:-जो वाणी के प्रयोग के असाधारण विशेषज्ञ होते थे, अर्थात् कब, कहाँ, कैसे वचन, कितनी मर्यादा में बोलने हैं - यह सब जो भलीभाँति जानते थे एवं तदनुसारी ही प्रयोग करते थे; उन्हें मनोज्ञ मुनि' कहा जाता था। किसी भी परिस्थिति-विशेष में या सामान्यजन को संबोधित करने का दायित्व इन्हीं का होता था। इनका निर्धारण भी आचार्य 'संघ' की सुरक्षा एवं व्यापक धर्मप्रभावना के निमित्त ही करते थे। क्योंकि
"पूयावयणं हिदभासणं मिदभासणं च महुरं च।
सुत्ताणुवीचिवयणं अणिठुरमकक्कसं वयणं ।।" - (मूलाचार, 377) अर्थ:-पूज्यवचन, हितवचन, मितवचन, मधुरवचन, सूत्रानुसारी अनुवीचिवचन, निष्ठुरता और कर्कशता से रहित वचन बोलना ही महामुनियों को शोभा देता है। यह उनकी वाचिक विनय' है।
इसीलिए वाग्व्यवहार के लिए संघ में 'मनोज्ञ मुनि' ही विशेषत: अधिकृत होते थे। मैं अपने जीवन के कुछ प्रसंगों को मात्र चिंतनार्थ यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
प्रसंग 1- सन् 1952 में जब क्षुल्लक अवस्था में कारकल (कर्नाटक) में था, तब प्रसिद्ध विद्वान् जी० ब्रह्मप्पा आये उन्होंने मुझे एवं सार्वजनिक प्रवचन करने का निवेदन किया। मैं चूँकि तब विशुद्ध ज्ञानाभ्यास के ध्येय से प्रवर्तित था, अत: मैंने विनम्र शब्दों में असमर्थता प्रकट कर दी। तब वे बोले “कि क्या मात्र पेट भरने के लिए ही घर-संसार छोड़ा है और त्यागधर्म अंगीकार किया है?" -मैंने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी तथा अपने लक्ष्य एवं परिस्थिति का विचार करते हुये मौनभाव से स्वाध्याय में निरत हो गया।
प्रसंग 2- मुनिदीक्षा के बाद सन् 1963 में दिल्ली में धर्मानुरागी श्री परसादीलाल पाटनी ने भी समाज में प्रवचन करने के लिए मुझसे अनुरोध किया, तथा मैंने अपनी स्थिति विचार करके असमर्थता व्यक्त की, तो वे भी बोले कि "क्या आप मात्र रोटी के लिए ही नग्न हुये हैं, गूंगे है। समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं है?" तब भी मैंने शास्त्र की मर्यादा विचारते हुये सहज शांत-भाव से उनके कठोरवचनों की उपेक्षा कर दी तथा कोई प्रतिक्रिया का विकल्प तक नहीं आया।
प्रसंग 3–सन् 1964 ई० में राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर में प्रथम चातुर्मास हुआ। वहाँ मैं अपने गुरु पूज्य आचार्य देशभूषण जी के साथ था। वहाँ पर मैं धर्मानुरागी विद्वान् पं० चैनसुखदास जी के अनुरोध पर आदर्शनगर-स्थित मुल्तानी-समाज के मंदिर में प्रवचन किया एवं इसी समाज के एक व्यक्ति के घर विधिपूर्वक आहार लिया।
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर'98
बर'98
0013