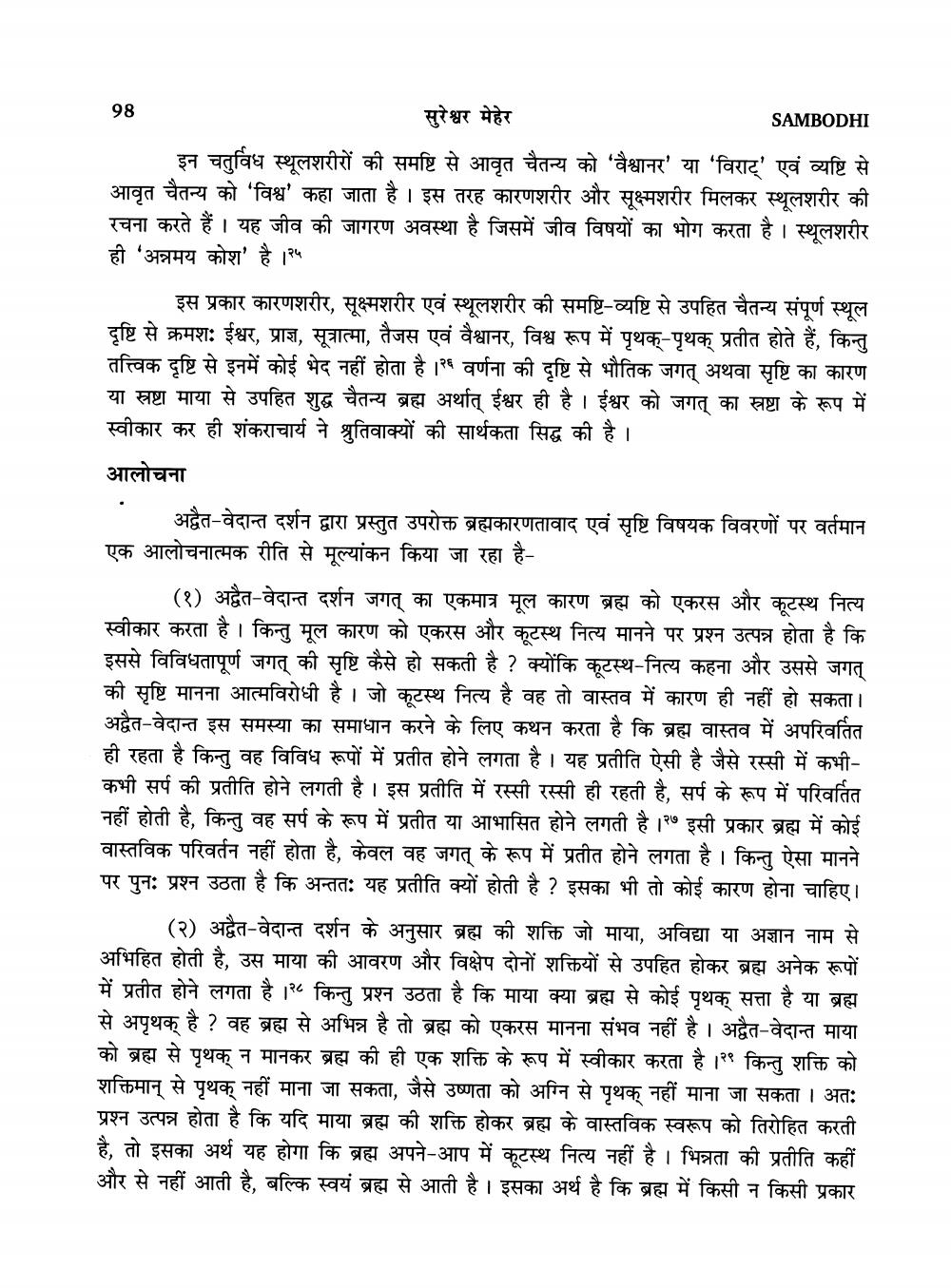________________
98
सुरेश्वर मेहेर
SAMBODHI इन चतुर्विध स्थूलशरीरों की समष्टि से आवृत चैतन्य को 'वैश्वानर' या 'विराट' एवं व्यष्टि से आवृत चैतन्य को 'विश्व' कहा जाता है । इस तरह कारणशरीर और सूक्ष्मशरीर मिलकर स्थूलशरीर की रचना करते हैं । यह जीव की जागरण अवस्था है जिसमें जीव विषयों का भोग करता है । स्थूलशरीर ही 'अन्नमय कोश' है ।२५
इस प्रकार कारणशरीर, सूक्ष्मशरीर एवं स्थूलशरीर की समष्टि-व्यष्टि से उपहित चैतन्य संपूर्ण स्थूल दृष्टि से क्रमशः ईश्वर, प्राज्ञ, सूत्रात्मा, तैजस एवं वैश्वानर, विश्व रूप में पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हैं, किन्तु तत्त्विक दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं होता है ।२६ वर्णना की दृष्टि से भौतिक जगत् अथवा सृष्टि का कारण या स्रष्टा माया से उपहित शुद्ध चैतन्य ब्रह्म अर्थात् ईश्वर ही है । ईश्वर को जगत् का स्रष्टा के रूप में स्वीकार कर ही शंकराचार्य ने श्रुतिवाक्यों की सार्थकता सिद्ध की है। आलोचना
अद्वैत-वेदान्त दर्शन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त ब्रह्मकारणतावाद एवं सृष्टि विषयक विवरणों पर वर्तमान एक आलोचनात्मक रीति से मूल्यांकन किया जा रहा है
(१) अद्वैत-वेदान्त दर्शन जगत् का एकमात्र मूल कारण ब्रह्म को एकरस और कूटस्थ नित्य स्वीकार करता है। किन्तु मूल कारण को एकरस और कूटस्थ नित्य मानने पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि इससे विविधतापूर्ण जगत् की सृष्टि कैसे हो सकती है ? क्योंकि कूटस्थ-नित्य कहना और उससे जगत् की सृष्टि मानना आत्मविरोधी है। जो कूटस्थ नित्य है वह तो वास्तव में कारण ही नहीं हो सकता। अद्वैत-वेदान्त इस समस्या का समाधान करने के लिए कथन करता है कि ब्रह्म वास्तव में अपरिवर्तित ही रहता है किन्तु वह विविध रूपों में प्रतीत होने लगता है। यह प्रतीति ऐसी है जैसे रस्सी में कभीकभी सर्प की प्रतीति होने लगती है। इस प्रतीति में रस्सी रस्सी ही रहती है, सर्प के रूप में परिवर्तित नहीं होती है, किन्तु वह सर्प के रूप में प्रतीत या आभासित होने लगती है ।२७ इसी प्रकार ब्रह्म में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है, केवल वह जगत् के रूप में प्रतीत होने लगता है । किन्तु ऐसा मानने पर पुनः प्रश्न उठता है कि अन्ततः यह प्रतीति क्यों होती है ? इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए।
(२) अद्वैत-वेदान्त दर्शन के अनुसार ब्रह्म की शक्ति जो माया, अविद्या या अज्ञान नाम से अभिहित होती है, उस माया की आवरण और विक्षेप दोनों शक्तियों से उपहित होकर ब्रह्म अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है ।२८ किन्तु प्रश्न उठता है कि माया क्या ब्रह्म से कोई पृथक् सत्ता है या ब्रह्म से अपृथक् है ? वह ब्रह्म से अभिन्न है तो ब्रह्म को एकरस मानना संभव नहीं है । अद्वैत-वेदान्त माया को ब्रह्म से पृथक् न मानकर ब्रह्म की ही एक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है ।२९ किन्तु शक्ति को शक्तिमान् से पृथक् नहीं माना जा सकता, जैसे उष्णता को अग्नि से पृथक् नहीं माना जा सकता । अत: प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि माया ब्रह्म की शक्ति होकर ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को तिरोहित करती है, तो इसका अर्थ यह होगा कि ब्रह्म अपने-आप में कूटस्थ नित्य नहीं है । भिन्नता की प्रतीति कहीं और से नहीं आती है, बल्कि स्वयं ब्रह्म से आती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म में किसी न किसी प्रकार