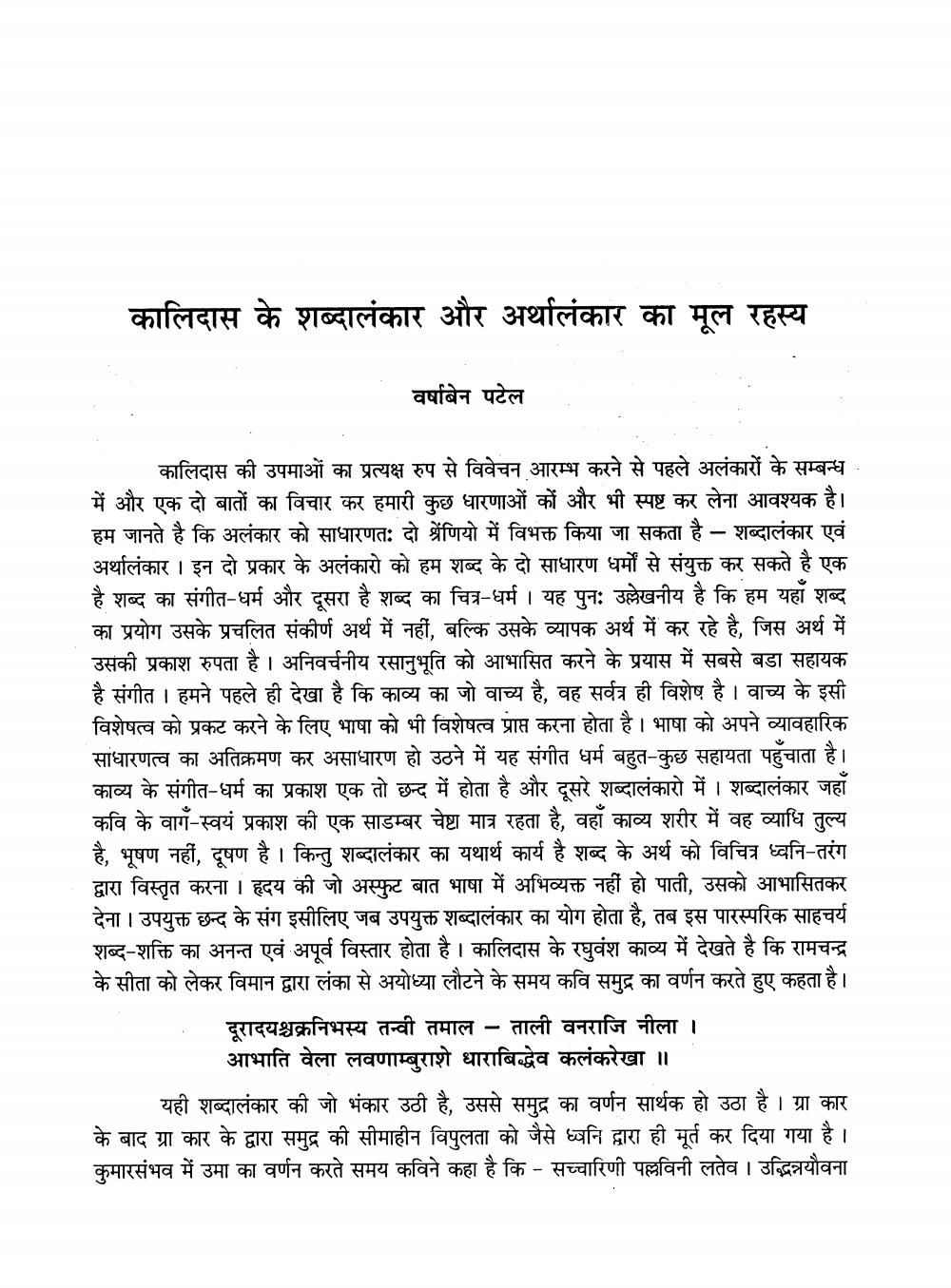________________
कालिदास के शब्दालंकार और अर्थालंकार का मूल रहस्य
वर्षाबेन पटेल
कालिदास की उपमाओं का प्रत्यक्ष रुप से विवेचन आरम्भ करने से पहले अलंकारों के सम्बन्ध . में और एक दो बातों का विचार कर हमारी कुछ धारणाओं कों और भी स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। हम जानते है कि अलंकार को साधारणतः दो श्रेणियो में विभक्त किया जा सकता है - शब्दालंकार एवं अर्थालंकार । इन दो प्रकार के अलंकारो को हम शब्द के दो साधारण धर्मों से संयुक्त कर सकते है एक है शब्द का संगीत-धर्म और दूसरा है शब्द का चित्र-धर्म । यह पनः उल्लेखनीय है कि हम यहाँ शब्द का प्रयोग उसके प्रचलित संकीर्ण अर्थ में नहीं, बल्कि उसके व्यापक अर्थ में कर रहे है, जिस अर्थ में उसकी प्रकाश रुपता है। अनिवर्चनीय रसानभति को आभासित करने के प्रयास में सबसे बडा सहायक है संगीत । हमने पहले ही देखा है कि काव्य का जो वाच्य है, वह सर्वत्र ही विशेष है। वाच्य के इसी विशेषत्व को प्रकट करने के लिए भाषा को भी विशेषत्व प्राप्त करना होता है। भाषा को अपने व्यावहारिक साधारणत्व का अतिक्रमण कर असाधारण हो उठने में यह संगीत धर्म बहुत-कुछ सहायता पहुँचाता है। काव्य के संगीत-धर्म का प्रकाश एक तो छन्द में होता है और दूसरे शब्दालंकारो में । शब्दालंकार जहाँ कवि के वाग-स्वयं प्रकाश की एक साडम्बर चेष्टा मात्र रहता है, वहाँ काव्य शरीर में वह व्याधि तुल्य है, भूषण नहीं, दूषण है। किन्तु शब्दालंकार का यथार्थ कार्य है शब्द के अर्थ को विचित्र ध्वनि-तरंग द्वारा विस्तृत करना । हृदय की जो अस्फुट बात भाषा में अभिव्यक्त नहीं हो पाती, उसको आभासितकर देना । उपयुक्त छन्द के संग इसीलिए जब उपयुक्त शब्दालंकार का योग होता है, तब इस पारस्परिक साहचर्य शब्द-शक्ति का अनन्त एवं अपूर्व विस्तार होता है । कालिदास के रघुवंश काव्य में देखते है कि रामचन्द्र के सीता को लेकर विमान द्वारा लंका से अयोध्या लौटने के समय कवि समुद्र का वर्णन करते हुए कहता है।
. दूरादयश्चक्रनिभस्य तन्वी तमाल - ताली वनराजि नीला ।
आभाति वेला लवणाम्बुराशे धाराबिद्धेव कलंकरेखा ॥ यही शब्दालंकार की जो भंकार उठी है, उससे समुद्र का वर्णन सार्थक हो उठा है । ग्रा कार के बाद ग्रा कार के द्वारा समुद्र की सीमाहीन विपुलता को जैसे ध्वनि द्वारा ही मूर्त कर दिया गया है। कुमारसंभव में उमा का वर्णन करते समय कविने कहा है कि - सच्चारिणी पल्लविनी लतेव । उद्भिनयौवना