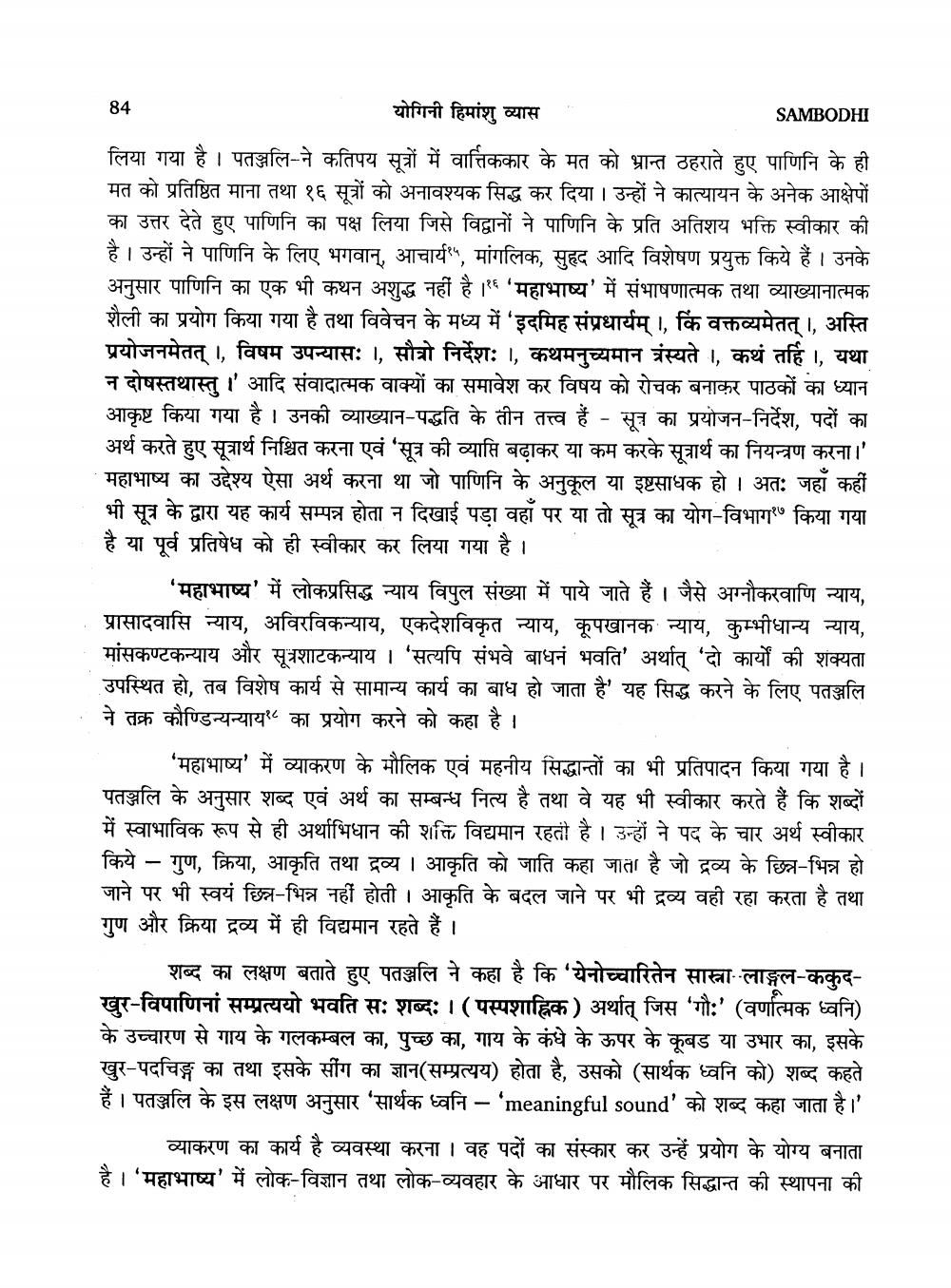________________ 84 योगिनी हिमांशु व्यास SAMBODHI लिया गया है / पतञ्जलि-ने कतिपय सूत्रों में वार्तिककार के मत को भ्रान्त ठहराते हुए पाणिनि के ही मत को प्रतिष्ठित माना तथा 16 सूत्रों को अनावश्यक सिद्ध कर दिया। उन्हों ने कात्यायन के अनेक आक्षेपों का उत्तर देते हुए पाणिनि का पक्ष लिया जिसे विद्वानों ने पाणिनि के प्रति अतिशय भक्ति स्वीकार की है। उन्हों ने पाणिनि के लिए भगवान्, आचार्य१५, मांगलिक, सुहृद आदि विशेषण प्रयुक्त किये हैं। उनके अनुसार पाणिनि का एक भी कथन अशुद्ध नहीं है / 16 'महाभाष्य' में संभाषणात्मक तथा व्याख्यानात्मक शैली का प्रयोग किया गया है तथा विवेचन के मध्य में 'इदमिह संप्रधार्यम् / , किं वक्तव्यमेतत् / , अस्ति प्रयोजनमेतत् / , विषम उपन्यासः / , सौत्रो निर्देशः / , कथमनुच्यमान –स्यते / , कथं तर्हि / , यथा न दोषस्तथास्तु / ' आदि संवादात्मक वाक्यों का समावेश कर विषय को रोचक बनाकर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। उनकी व्याख्यान-पद्धति के तीन तत्त्व हैं - सूत्र का प्रयोजन-निर्देश, पदों का अर्थ करते हुए सूत्रार्थ निश्चित करना एवं 'सूत्र की व्याप्ति बढ़ाकर या कम करके सूत्रार्थ का नियन्त्रण करना।' महाभाष्य का उद्देश्य ऐसा अर्थ करना था जो पाणिनि के अनुकूल या इष्टसाधक हो / अतः जहाँ कहीं भी सूत्र के द्वारा यह कार्य सम्पन्न होता न दिखाई पड़ा वहाँ पर या तो सूत्र का योग-विभाग किया गया है या पूर्व प्रतिषेध को ही स्वीकार कर लिया गया है। - 'महाभाष्य' में लोकप्रसिद्ध न्याय विपुल संख्या में पाये जाते हैं / जैसे अग्नौकरवाणि न्याय, . प्रासादवासि न्याय, अविरविकन्याय, एकदेशविकृत न्याय, कूपखानक न्याय, कुम्भीधान्य न्याय, मांसकण्टकन्याय और सूत्रशाटकन्याय / 'सत्यपि संभवे बाधनं भवति' अर्थात् 'दो कार्यों की शक्यता उपस्थित हो, तब विशेष कार्य से सामान्य कार्य का बाध हो जाता है' यह सिद्ध करने के लिए पतञ्जलि ने तक्र कौण्डिन्यन्याय८ का प्रयोग करने को कहा है। 'महाभाष्य' में व्याकरण के मौलिक एवं महनीय सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया है / पतञ्जलि के अनुसार शब्द एवं अर्थ का सम्बन्ध नित्य है तथा वे यह भी स्वीकार करते हैं कि शब्दों में स्वाभाविक रूप से ही अर्थाभिधान की शक्ति विद्यमान रहती है। उन्हों ने पद के चार अर्थ स्वीकार किये - गुण, क्रिया, आकृति तथा द्रव्य / आकृति को जाति कहा जाता है जो द्रव्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर भी स्वयं छिन्न-भिन्न नहीं होती / आकृति के बदल जाने पर भी द्रव्य वही रहा करता है तथा गुण और क्रिया द्रव्य में ही विद्यमान रहते हैं। शब्द का लक्षण बताते हुए पतञ्जलि ने कहा है कि 'येनोच्चारितेन सास्ना--लाङ्गल-ककुदखुर-विपाणिनां सम्प्रत्ययो भवति सः शब्दः / (पस्पशाह्निक) अर्थात् जिस 'गौः' (वर्णात्मक ध्वनि) के उच्चारण से गाय के गलकम्बल का, पुच्छ का, गाय के कंधे के ऊपर के कूबड या उभार का, इसके खुर-पदचिङ्ग का तथा इसके सींग का ज्ञान(सम्प्रत्यय) होता है, उसको (सार्थक ध्वनि को) शब्द कहते हैं / पतञ्जलि के इस लक्षण अनुसार 'सार्थक ध्वनि - 'meaningful sound' को शब्द कहा जाता है।' व्याकरण का कार्य है व्यवस्था करना / वह पदों का संस्कार कर उन्हें प्रयोग के योग्य बनाता है / 'महाभाष्य' में लोक-विज्ञान तथा लोक-व्यवहार के आधार पर मौलिक सिद्धान्त की स्थापना की