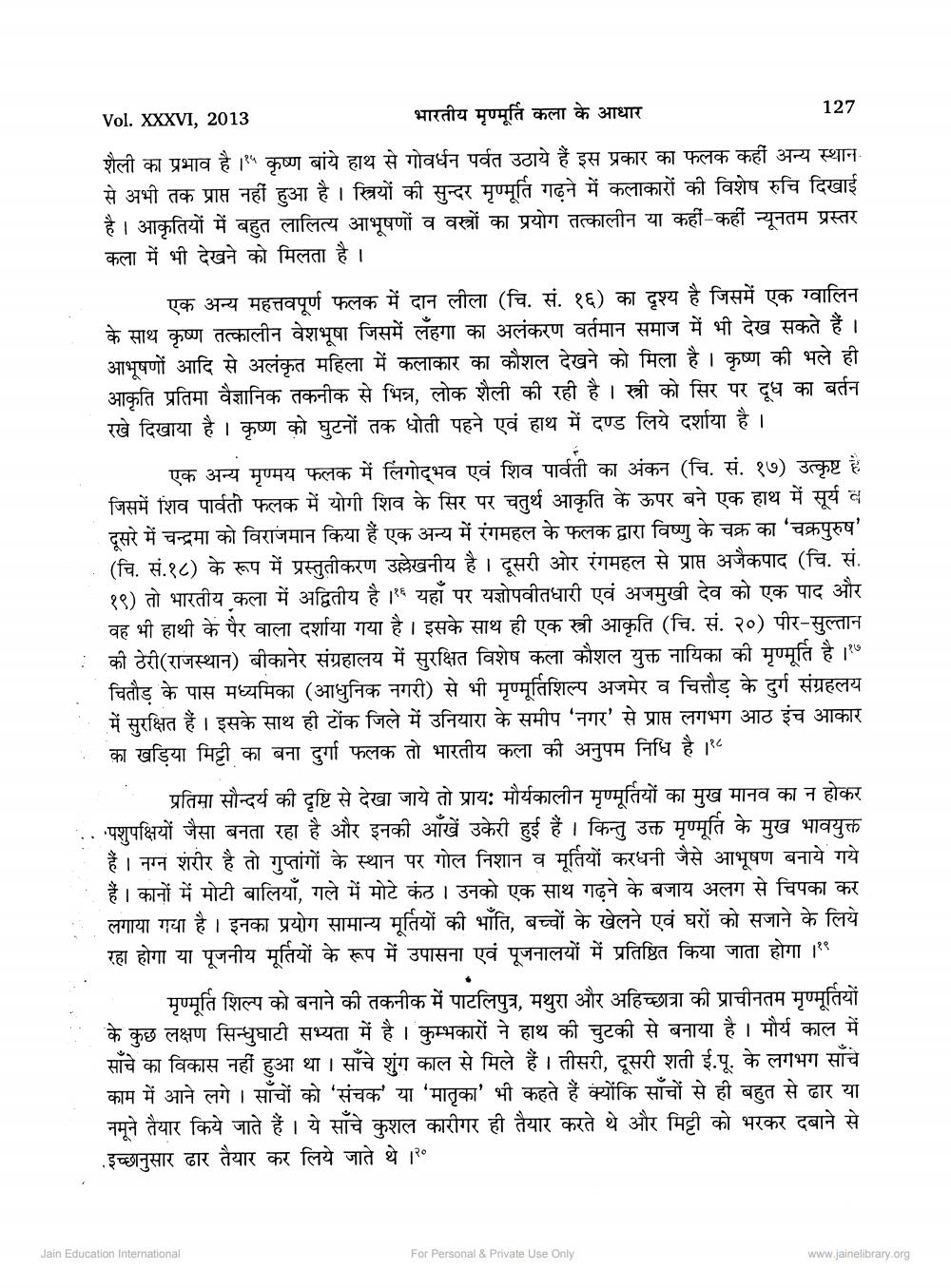________________
Vol. XXXVI, 2013 भारतीय मृणमूर्ति कला के आधार
127 शैली का प्रभाव है ।१५ कृष्ण बांये हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाये हैं इस प्रकार का फलक कहीं अन्य स्थान से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। स्त्रियों की सुन्दर मृणमूर्ति गढ़ने में कलाकारों की विशेष रुचि दिखाई है। आकृतियों में बहुत लालित्य आभूषणों व वस्त्रों का प्रयोग तत्कालीन या कहीं-कहीं न्यूनतम प्रस्तर कला में भी देखने को मिलता है।
__एक अन्य महत्तवपूर्ण फलक में दान लीला (चि. सं. १६) का दृश्य है जिसमें एक ग्वालिन के साथ कृष्ण तत्कालीन वेशभूषा जिसमें लँहगा का अलंकरण वर्तमान समाज में भी देख सकते हैं। आभूषणों आदि से अलंकृत महिला में कलाकार का कौशल देखने को मिला है । कृष्ण की भले ही आकृति प्रतिमा वैज्ञानिक तकनीक से भिन्न, लोक शैली की रही है । स्त्री को सिर पर दूध का बर्तन रखे दिखाया है । कृष्ण को घुटनों तक धोती पहने एवं हाथ में दण्ड लिये दर्शाया है ।
___एक अन्य मृण्मय फलक में लिंगोद्भव एवं शिव पार्वती का अंकन (चि. सं. १७) उत्कृष्ट है जिसमें शिव पार्वती फलक में योगी शिव के सिर पर चतुर्थ आकृति के ऊपर बने एक हाथ में सूर्य व दूसरे में चन्द्रमा को विराजमान किया हैं एक अन्य में रंगमहल के फलक द्वारा विष्णु के चक्र का 'चक्रपुरुष' (चि. सं.१८) के रूप में प्रस्तुतीकरण उल्लेखनीय है। दूसरी ओर रंगमहल से प्राप्त अजैकपाद (चि. सं. १९) तो भारतीय कला में अद्वितीय है ।१६ यहाँ पर यज्ञोपवीतधारी एवं अजमुखी देव को एक पाद और वह भी हाथी के पैर वाला दर्शाया गया है। इसके साथ ही एक स्त्री आकृति (चि. सं. २०) पीर-सुल्तान की ठेरी(राजस्थान) बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित विशेष कला कौशल युक्त नायिका की मृण्मूर्ति है ।१७ चितौड़ के पास मध्यमिका (आधुनिक नगरी) से भी मृणमूर्तिशिल्प अजमेर व चित्तौड़ के दुर्ग संग्रहलय में सुरक्षित हैं। इसके साथ ही टोंक जिले में उनियारा के समीप 'नगर' से प्राप्त लगभग आठ इंच आकार का खड़िया मिट्टी का बना दुर्गा फलक तो भारतीय कला की अनुपम निधि है ।१८
प्रतिमा सौन्दर्य की दृष्टि से देखा जाये तो प्राय: मौर्यकालीन मृण्मूर्तियों का मुख मानव का न होकर .. पशुपक्षियों जैसा बनता रहा है और इनकी आँखें उकेरी हुई हैं । किन्तु उक्त मृण्मूर्ति के मुख भावयुक्त - हैं। नग्न शरीर है तो गुप्तांगों के स्थान पर गोल निशान व मूर्तियों करधनी जैसे आभूषण बनाये गये हैं। कानों में मोटी बालिया, गले में मोटे कंठ । उनको एक साथ गढ़ने के बजाय अलग से चिपका कर लगाया गया है। इनका प्रयोग सामान्य मूर्तियों की भाति, बच्चों के खेलने एवं घरों को सजाने के लिये रहा होगा या पूजनीय मूर्तियों के रूप में उपासना एवं पूजनालयों में प्रतिष्ठित किया जाता होगा ।१९
मृण्मूर्ति शिल्प को बनाने की तकनीक में पाटलिपुत्र, मथुरा और अहिच्छात्रा की प्राचीनतम मृण्मूर्तियों के कुछ लक्षण सिन्धुघाटी सभ्यता में है। कुम्भकारों ने हाथ की चुटकी से बनाया है। मौर्य काल में साँचे का विकास नहीं हुआ था । साँचे शुंग काल से मिले हैं। तीसरी, दूसरी शती ई.पू. के लगभग साँचे काम में आने लगे । साँचों को 'संचक' या 'मातृका' भी कहते हैं क्योंकि साचों से ही बहुत से ढार या नमूने तैयार किये जाते हैं । ये साँचे कुशल कारीगर ही तैयार करते थे और मिट्टी को भरकर दबाने से इच्छानुसार ढार तैयार कर लिये जाते थे ।२०
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org