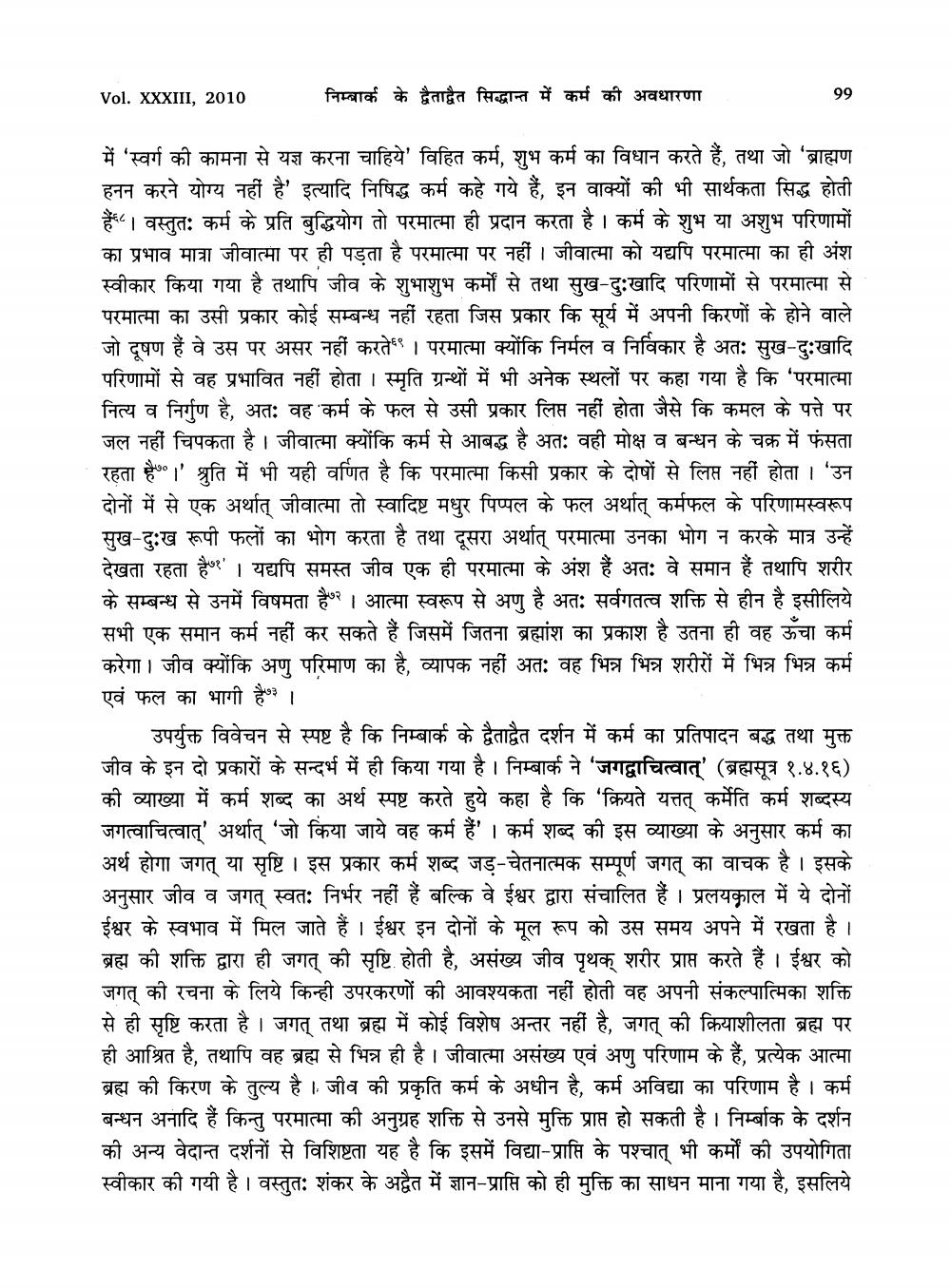________________
Vol. XXXIII, 2010
निम्बार्क के द्वैताद्वैत सिद्धान्त में कर्म की अवधारणा
99
में 'स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिये' विहित कर्म, शुभ कर्म का विधान करते हैं, तथा जो 'ब्राह्मण हनन करने योग्य नहीं है' इत्यादि निषिद्ध कर्म कहे गये हैं, इन वाक्यों की भी सार्थकता सिद्ध होती हैं । वस्तुतः कर्म के प्रति बुद्धियोग तो परमात्मा ही प्रदान करता है । कर्म के शुभ या अशुभ परिणामों का प्रभाव मात्रा जीवात्मा पर ही पड़ता है परमात्मा पर नहीं । जीवात्मा को यद्यपि परमात्मा का ही अंश स्वीकार किया गया है तथापि जीव के शुभाशुभ कर्मों से तथा सुख-दुःखादि परिणामों से परमात्मा से परमात्मा का उसी प्रकार कोई सम्बन्ध नहीं रहता जिस प्रकार कि सूर्य में अपनी किरणों के होने वाले जो दूषण हैं वे उस पर असर नहीं करते६९ । परमात्मा क्योंकि निर्मल व निर्विकार है अतः सुख-दुःखादि परिणामों से वह प्रभावित नहीं होता । स्मृति ग्रन्थों में भी अनेक स्थलों पर कहा गया है कि 'परमात्मा नित्य व निर्गुण है, अतः वह कर्म के फल से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल के पत्ते पर जल नहीं चिपकता है। जीवात्मा क्योंकि कर्म से आबद्ध है अतः वही मोक्ष व बन्धन के चक्र में फंसता रहता है।' श्रुति में भी यही वर्णित है कि परमात्मा किसी प्रकार के दोषों से लिप्त नहीं होता । 'उन दोनों में से एक अर्थात् जीवात्मा तो स्वादिष्ट मधुर पिप्पल के फल अर्थात् कर्मफल के परिणामस्वरूप सुख-दुःख रूपी फलों का भोग करता है तथा दूसरा अर्थात् परमात्मा उनका भोग न करके मात्र उन्हें देखता रहता है । यद्यपि समस्त जीव एक ही परमात्मा के अंश हैं अतः वे समान हैं तथापि शरीर के सम्बन्ध से उनमें विषमता है७२ । आत्मा स्वरूप से अण है अतः सर्वगतत्व शक्ति से हीन है इसीलिये सभी एक समान कर्म नहीं कर सकते हैं जिसमें जितना ब्रह्मांश का प्रकाश है उतना ही वह ऊंचा कर्म करेगा। जीव क्योंकि अणु परिमाण का है, व्यापक नहीं अत: वह भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न कर्म एवं फल का भागी है ।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निम्बार्क के द्वैताद्वैत दर्शन में कर्म का प्रतिपादन बद्ध तथा मुक्त जीव के इन दो प्रकारों के सन्दर्भ में ही किया गया है। निम्बार्क ने 'जगद्वाचित्वात्' (ब्रह्मसूत्र १.४.१६) की व्याख्या में कर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुये कहा है कि 'क्रियते यत्तत् कर्मेति कर्म शब्दस्य जगत्वाचित्वात्' अर्थात् 'जो किया जाये वह कर्म हैं' । कर्म शब्द की इस व्याख्या के अनुसार कर्म का अर्थ होगा जगत् या सृष्टि । इस प्रकार कर्म शब्द जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत् का वाचक है । इसके अनुसार जीव व जगत् स्वतः निर्भर नहीं हैं बल्कि वे ईश्वर द्वारा संचालित हैं । प्रलयकाल में ये दोनों ईश्वर के स्वभाव में मिल जाते हैं । ईश्वर इन दोनों के मूल रूप को उस समय अपने में रखता है। ब्रह्म की शक्ति द्वारा ही जगत् की सृष्टि होती है, असंख्य जीव पृथक् शरीर प्राप्त करते हैं । ईश्वर को जगत् की रचना के लिये किन्ही उपरकरणों की आवश्यकता नहीं होती वह अपनी संकल्पात्मिका शक्ति से ही सृष्टि करता है । जगत् तथा ब्रह्म में कोई विशेष अन्तर नहीं है, जगत् की क्रियाशीलता ब्रह्म पर ही आश्रित है, तथापि वह ब्रह्म से भिन्न ही है । जीवात्मा असंख्य एवं अणु परिणाम के हैं, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म की किरण के तुल्य है। जीव की प्रकृति कर्म के अधीन है, कर्म अविद्या का परिणाम है । कर्म बन्धन अनादि हैं किन्तु परमात्मा की अनुग्रह शक्ति से उनसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। निर्बाक के दर्शन की अन्य वेदान्त दर्शनों से विशिष्टता यह है कि इसमें विद्या-प्राप्ति के पश्चात् भी कर्मों की उपयोगिता स्वीकार की गयी है। वस्तुत: शंकर के अद्वैत में ज्ञान-प्राप्ति को ही मुक्ति का साधन माना गया है, इसलिये