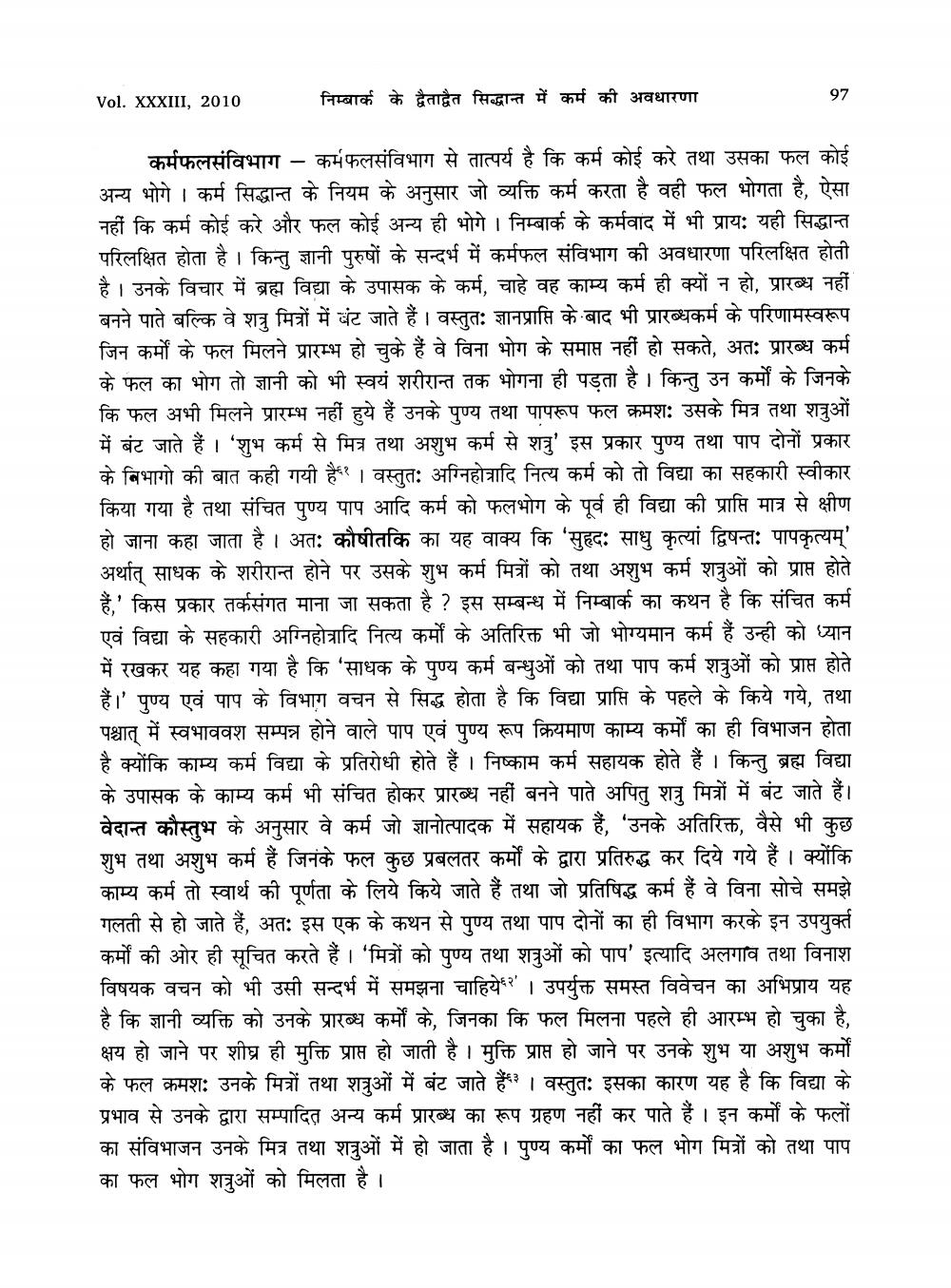________________
Vol. XXXIII, 2010
निम्बार्क के द्वैताद्वैत सिद्धान्त में कर्म की अवधारणा
कर्मफलसंविभाग - कर्मफलसंविभाग से तात्पर्य है कि कर्म कोई करे तथा उसका फल कोई अन्य भोगे । कर्म सिद्धान्त के नियम के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है वही फल भोगता है, ऐसा नहीं कि कर्म कोई करे और फल कोई अन्य ही भोगे । निम्बार्क के कर्मवाद में भी प्रायः यही सिद्धान्त परिलक्षित होता है । किन्तु ज्ञानी पुरुषों के सन्दर्भ में कर्मफल संविभाग की अवधारणा परिलक्षित होती है । उनके विचार में ब्रह्म विद्या के उपासक के कर्म, चाहे वह काम्य कर्म ही क्यों न हो, प्रारब्ध नहीं बनने पाते बल्कि वे शत्रु मित्रों में बंट जाते हैं । वस्तुतः ज्ञानप्राप्ति के बाद भी प्रारब्धकर्म के परिणामस्वरूप जिन कर्मों के फल मिलने प्रारम्भ हो चुके हैं वे विना भोग के समाप्त नहीं हो सकते, अतः प्रारब्ध कर्म के फल का भोग तो ज्ञानी को भी स्वयं शरीरान्त तक भोगना ही पड़ता है। किन्तु उन कर्मों के जिनके कि फल अभी मिलने प्रारम्भ नहीं हुये हैं उनके पुण्य तथा पापरूप फल क्रमशः उसके मित्र तथा शत्रुओं में बंट जाते हैं । ‘शुभ कर्म से मित्र तथा अशुभ कर्म से शत्रु' इस प्रकार पुण्य तथा पाप दोनों प्रकार के विभागो की बात कही गयी है । वस्तुतः अग्निहोत्रादि नित्य कर्म को तो विद्या का सहकारी स्वीकार किया गया है तथा संचित पुण्य पाप आदि कर्म को फलभोग के पूर्व ही विद्या की प्राप्ति मात्र से क्षीण हो जाना कहा जाता है। अतः कौषीतकि का यह वाक्य कि 'सुहृदः साधु कृत्यां द्विषन्तः पापकृत्यम्' अर्थात् साधक के शरीरान्त होने पर उसके शुभ कर्म मित्रों को तथा अशुभ कर्म शत्रुओं को प्राप्त होते हैं,' किस प्रकार तर्कसंगत माना जा सकता है ? इस सम्बन्ध में निम्बार्क का कथन है कि संचित कर्म एवं विद्या के सहकारी अग्निहोत्रादि नित्य कर्मों के अतिरिक्त भी जो भोग्यमान कर्म हैं उन्ही को ध्यान में रखकर यह कहा गया है कि 'साधक के पुण्य कर्म बन्धुओं को तथा पाप कर्म शत्रुओं को प्राप्त होते हैं।' पुण्य एवं पाप के विभाग वचन से सिद्ध होता है कि विद्या प्राप्ति के पहले के किये गये, तथा पश्चात् में स्वभाववश सम्पन्न होने वाले पाप एवं पुण्य रूप क्रियमाण काम्य कर्मों का ही विभाजन होता है क्योंकि काम्य कर्म विद्या के प्रतिरोधी होते हैं । निष्काम कर्म सहायक होते हैं । किन्तु ब्रह्म विद्या के उपासक के काम्य कर्म भी संचित होकर प्रारब्ध नहीं बनने पाते अपितु शत्रु मित्रों में बंट जाते हैं। वेदान्त कौस्तुभ के अनुसार वे कर्म जो ज्ञानोत्पादक में सहायक हैं, 'उनके अतिरिक्त, वैसे भी कुछ शुभ तथा अशुभ कर्म हैं जिनके फल कुछ प्रबलतर कर्मों के द्वारा प्रतिरुद्ध कर दिये गये हैं। क्योंकि काम्य कर्म तो स्वार्थ की पूर्णता के लिये किये जाते हैं तथा जो प्रतिषिद्ध कर्म हैं वे विना सोचे समझे गलती से हो जाते हैं, अतः इस एक के कथन से पुण्य तथा पाप दोनों का ही विभाग करके इन उपयुक्त कर्मों की ओर ही सूचित करते हैं । 'मित्रों को पुण्य तथा शत्रुओं को पाप' इत्यादि अलगाव तथा विनाश विषयक वचन को भी उसी सन्दर्भ में समझना चाहिये२' । उपर्युक्त समस्त विवेचन का अभिप्राय यह है कि ज्ञानी व्यक्ति को उनके प्रारब्ध कर्मों के, जिनका कि फल मिलना पहले ही आरम्भ हो चुका है, क्षय हो जाने पर शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति प्राप्त हो जाने पर उनके शुभ या अशुभ कर्मों के फल क्रमशः उनके मित्रों तथा शत्रुओं में बंट जाते हैं । वस्तुतः इसका कारण यह है कि विद्या के प्रभाव से उनके द्वारा सम्पादित अन्य कर्म प्रारब्ध का रूप ग्रहण नहीं कर पाते हैं । इन कर्मों के फलों का संविभाजन उनके मित्र तथा शत्रुओं में हो जाता है । पुण्य कर्मों का फल भोग मित्रों को तथा पाप का फल भोग शत्रुओं को मिलता है।