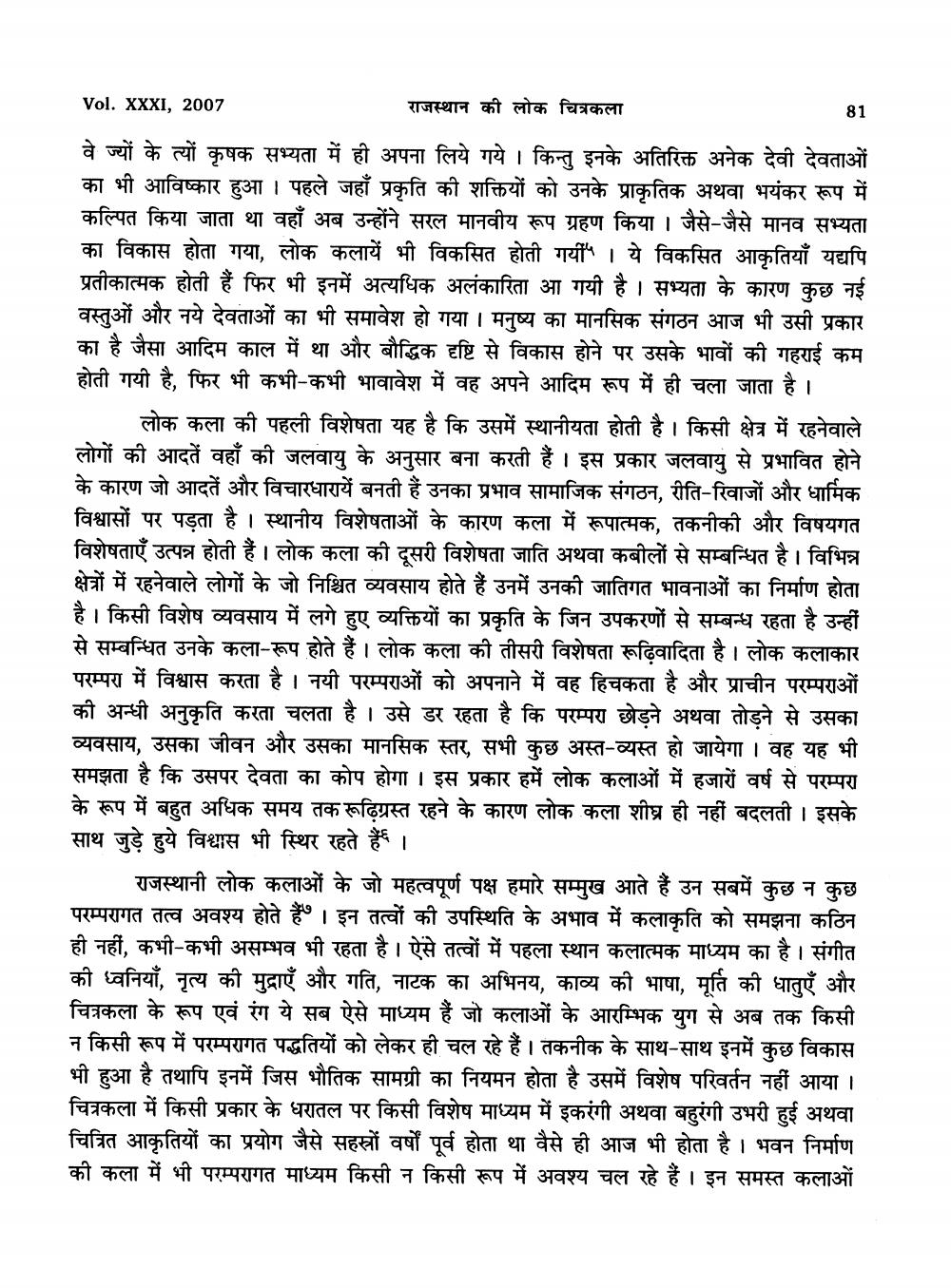________________
Vol. xxxI, 2007
राजस्थान की लोक चित्रकला
81
वे ज्यों के त्यों कृषक सभ्यता में ही अपना लिये गये । किन्तु इनके अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं का भी आविष्कार हुआ। पहले जहाँ प्रकृति की शक्तियों को उनके प्राकृतिक अथवा भयंकर रूप में कल्पित किया जाता था वहाँ अब उन्होंने सरल मानवीय रूप ग्रहण किया । जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, लोक कलायें भी विकसित होती गयीं । ये विकसित आकृतियाँ यद्यपि प्रतीकात्मक होती हैं फिर भी इनमें अत्यधिक अलंकारिता आ गयी है । सभ्यता के कारण कुछ नई वस्तुओं और नये देवताओं का भी समावेश हो गया । मनुष्य का मानसिक संगठन आज भी उसी प्रकार का है जैसा आदिम काल में था और बौद्धिक दृष्टि से विकास होने पर उसके भावों की गहराई कम होती गयी है, फिर भी कभी-कभी भावावेश में वह अपने आदिम रूप में ही चला जाता है ।
लोक कला की पहली विशेषता यह है कि उसमें स्थानीयता होती है। किसी क्षेत्र में रहनेवाले लोगों की आदतें वहाँ की जलवायु के अनुसार बना करती हैं । इस प्रकार जलवायु से प्रभावित होने के कारण जो आदतें और विचारधारायें बनती हैं उनका प्रभाव सामाजिक संगठन, रीति-रिवाजों और धार्मिक विश्वासों पर पड़ता है। स्थानीय विशेषताओं के कारण कला में रूपात्मक, तकनीकी और विषयगत विशेषताएँ उत्पन्न होती हैं । लोक कला की दूसरी विशेषता जाति अथवा कबीलों से सम्बन्धित है। विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों के जो निश्चित व्यवसाय होते हैं उनमें उनकी जातिगत भावनाओं का निर्माण होता है। किसी विशेष व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का प्रकृति के जिन उपकरणों से सम्बन्ध रहता है उन्हीं से सम्बन्धित उनके कला-रूप होते हैं । लोक कला की तीसरी विशेषता रूढ़िवादिता है। लोक कलाकार परम्परा में विश्वास करता है । नयी परम्पराओं को अपनाने में वह हिचकता है और प्राचीन परम्पराओं की अन्धी अनुकृति करता चलता है। उसे डर रहता है कि परम्परा छोड़ने अथवा तोड़ने से उसका व्यवसाय, उसका जीवन और उसका मानसिक स्तर, सभी कुछ अस्त-व्यस्त हो जायेगा । वह यह भी समझता है कि उसपर देवता का कोप होगा । इस प्रकार हमें लोक कलाओं में हजारों वर्ष से परम्परा के रूप में बहुत अधिक समय तक रूढ़िग्रस्त रहने के कारण लोक कला शीघ्र ही नहीं बदलती। इसके साथ जुड़े हुये विश्वास भी स्थिर रहते हैं ।
राजस्थानी लोक कलाओं के जो महत्वपूर्ण पक्ष हमारे सम्मुख आते हैं उन सबमें कुछ न कुछ परम्परागत तत्व अवश्य होते हैं । इन तत्वों की उपस्थिति के अभाव में कलाकृति को समझना कठिन ही नहीं, कभी-कभी असम्भव भी रहता है। ऐसे तत्वों में पहला स्थान कलात्मक माध्यम का है। संगीत की ध्वनियाँ, नृत्य की मुद्राएँ और गति, नाटक का अभिनय, काव्य की भाषा, मूर्ति की धातुएँ और चित्रकला के रूप एवं रंग ये सब ऐसे माध्यम हैं जो कलाओं के आरम्भिक युग से अब तक किसी न किसी रूप में परम्परागत पद्धतियों को लेकर ही चल रहे हैं। तकनीक के साथ-साथ इनमें कुछ विकास भी हुआ है तथापि इनमें जिस भौतिक सामग्री का नियमन होता है उसमें विशेष परिवर्तन नहीं आया । चित्रकला में किसी प्रकार के धरातल पर किसी विशेष माध्यम में इकरंगी अथवा बहुरंगी उभरी हुई अथवा चित्रित आकृतियों का प्रयोग जैसे सहस्रों वर्षों पूर्व होता था वैसे ही आज भी होता है । भवन निर्माण की कला में भी परम्परागत माध्यम किसी न किसी रूप में अवश्य चल रहे हैं । इन समस्त कलाओं