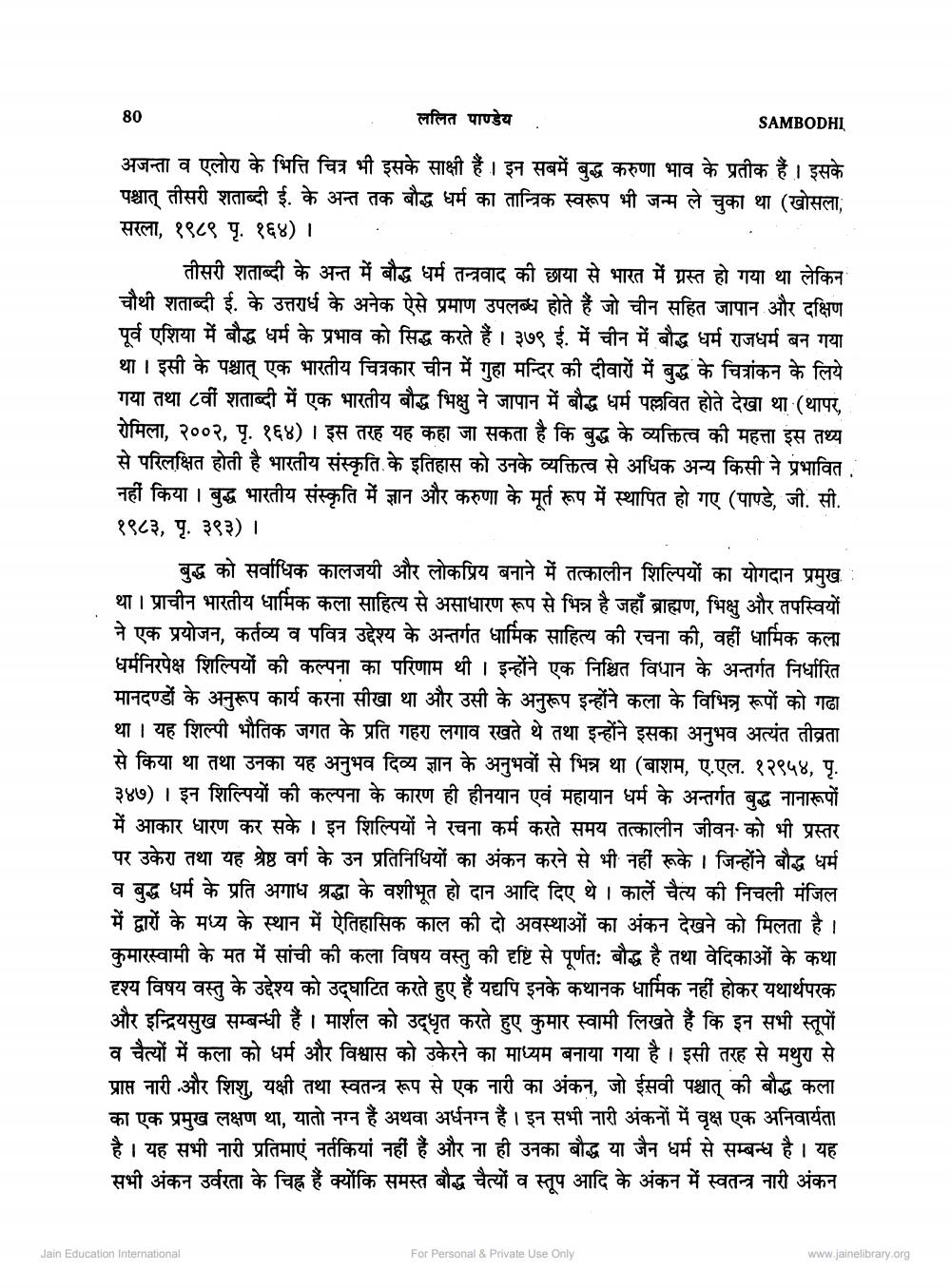________________
ललित पाण्डेय
SAMBODHI
अजन्ता व एलोरा के भित्ति चित्र भी इसके साक्षी हैं । इन सबमें बुद्ध करुणा भाव के प्रतीक हैं। इसके पश्चात् तीसरी शताब्दी ई. के अन्त तक बौद्ध धर्म का तान्त्रिक स्वरूप भी जन्म ले चुका था (खोसला, सरला, १९८९ पृ. १६४) ।
80
तीसरी शताब्दी के अन्त में बौद्ध धर्म तन्त्रवाद की छाया से भारत में ग्रस्त हो गया था लेकिन चौथी शताब्दी ई. के उत्तरार्ध के अनेक ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं। चीन सहित जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रभाव को सिद्ध करते हैं । ३७९ ई. में चीन में बौद्ध धर्म राजधर्म बन गया था । इसी के पश्चात् एक भारतीय चित्रकार चीन में गुहा मन्दिर की दीवारों में बुद्ध के चित्रांकन के लिये गया तथा ८वीं शताब्दी में एक भारतीय बौद्ध भिक्षु ने जापान में बौद्ध धर्म पल्लवित होते देखा था ( थापर, रोमिला, २००२, पृ. १६४) । इस तरह यह कहा जा सकता है कि बुद्ध के व्यक्तित्व की महत्ता इस तथ्य से परिलक्षित होती है भारतीय संस्कृति के इतिहास को उनके व्यक्तित्व से अधिक अन्य किसी ने प्रभावित . नहीं किया । बुद्ध भारतीय संस्कृति में ज्ञान और करुणा के मूर्त रूप में स्थापित हो गए (पाण्डे, जी. सी. १९८३, पृ. ३९३) ।
बुद्ध को सर्वाधिक कालजयी और लोकप्रिय बनाने में तत्कालीन शिल्पियों का योगदान प्रमुख था। प्राचीन भारतीय धार्मिक कला साहित्य से असाधारण रूप से भिन्न है जहाँ ब्राह्मण, भिक्षु और तपस्वियों ने एक प्रयोजन, कर्तव्य व पवित्र उद्देश्य के अन्तर्गत धार्मिक साहित्य की रचना की, वहीं धार्मिक कला धर्मनिरपेक्ष शिल्पियों की कल्पना का परिणाम थी । इन्होंने एक निश्चित विधान के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप कार्य करना सीखा था और उसी के अनुरूप इन्होंने कला के विभिन्न रूपों को गढा था । यह शिल्पी भौतिक जगत के प्रति गहरा लगाव रखते थे तथा इन्होंने इसका अनुभव अत्यंत तीव्रता से किया था तथा उनका यह अनुभव दिव्य ज्ञान के अनुभवों से भिन्न था (बाशम, ए. एल. १२९५४, पृ. ३४७) । इन शिल्पियों की कल्पना के कारण ही हीनयान एवं महायान धर्म के अन्तर्गत बुद्ध नानारूपों में आकार धारण कर सके। इन शिल्पियों ने रचना कर्म करते समय तत्कालीन जीवन को भी प्रस्तर पर उकेरा तथा यह श्रेष्ठ वर्ग के उन प्रतिनिधियों का अंकन करने से भी नहीं रूके । जिन्होंने बौद्ध धर्म बुद्ध धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा के वशीभूत हो दान आदि दिए थे। कार्ले चैत्य की निचली मंजिल में द्वारों के मध्य के स्थान में ऐतिहासिक काल की दो अवस्थाओं का अंकन देखने को मिलता है । कुमारस्वामी के मत में सांची की कला विषय वस्तु की दृष्टि से पूर्णतः बौद्ध है तथा वेदिकाओं के कथा दृश्य विषय वस्तु के उद्देश्य को उद्घाटित करते हुए हैं यद्यपि इनके कथानक धार्मिक नहीं होकर यथार्थपरक और इन्द्रियसुख सम्बन्धी हैं । मार्शल को उद्धृत करते हुए कुमार स्वामी लिखते हैं कि इन सभी स्तूपों व चैत्यों में कला को धर्म और विश्वास को उकेरने का माध्यम बनाया गया है। इसी तरह मथुरा से प्राप्त नारी और शिशु, यक्षी तथा स्वतन्त्र रूप से एक नारी का अंकन, जो ईसवी पश्चात् की बौद्ध कला का एक प्रमुख लक्षण था, यातो नग्न हैं अथवा अर्धनग्न हैं। इन सभी नारी अंकनों में वृक्ष एक अनिवार्यता है । यह सभी नारी प्रतिमाएं नर्तकियां नहीं हैं और ना उनका बौद्ध या जैन धर्म से सम्बन्ध है । यह सभी अंकन उर्वरता के चिह्न हैं क्योंकि समस्त बौद्ध चैत्यों व स्तूप आदि के अंकन
स्वतन्त्र नारी अंकन
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org