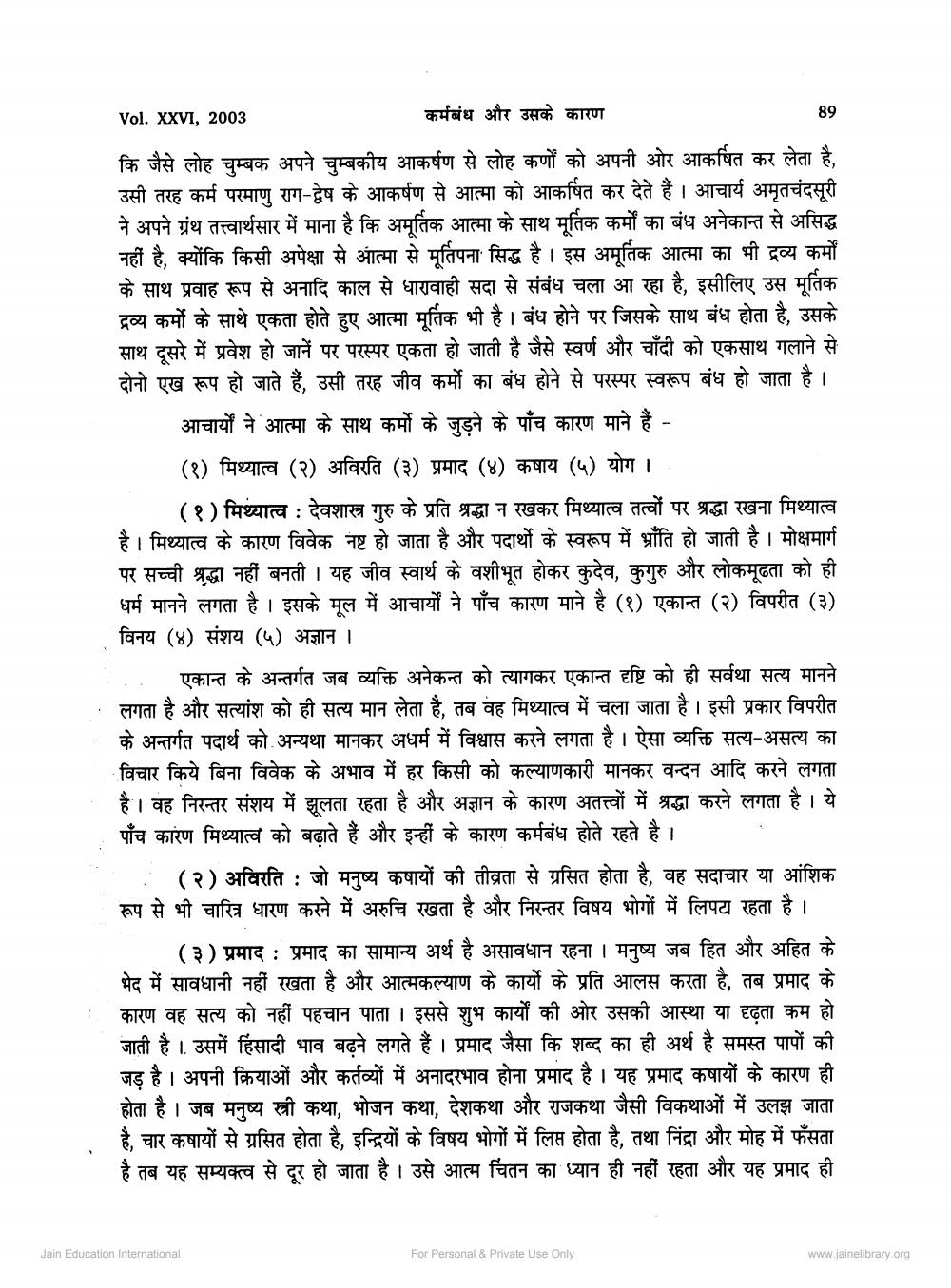________________
Vol. XXVI, 2003
कर्मबंध और उसके कारण
कि जैसे लोह चुम्बक अपने चुम्बकीय आकर्षण से लोह कर्णों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी तरह कर्म परमाणु राग-द्वेष के आकर्षण से आत्मा को आकर्षित कर देते हैं । आचार्य अमृतचंदसूरी ने अपने ग्रंथ तत्त्वार्थसार में माना है कि अमूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्मों का बंध अनेकान्त से असिद्ध नहीं है, क्योंकि किसी अपेक्षा से आत्मा से मूर्तिपना सिद्ध है । इस अमूर्तिक आत्मा का भी द्रव्य कर्मों के साथ प्रवाह रूप से अनादि काल से धारावाही सदा से संबंध चला आ रहा है, इसीलिए उस मूर्तिक द्रव्य कर्मो के साथे एकता होते हुए आत्मा मूर्तिक भी है। बंध होने पर जिसके साथ बंध होता है, उसके साथ दूसरे में प्रवेश हो जानें पर परस्पर एकता हो जाती है जैसे स्वर्ण और चाँदी को एकसाथ गलाने से दोनो एख रूप हो जाते हैं, उसी तरह जीव कर्मों का बंध होने से परस्पर स्वरूप बंध हो जाता है 1
आचार्यों ने आत्मा के साथ कर्मों के जुड़ने के पाँच कारण माने हैं.
-
(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कषाय (५) योग ।
(१) मिथ्यात्व : देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा न रखकर मिथ्यात्व तत्वों पर श्रद्धा रखना मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व के कारण विवेक नष्ट हो जाता है और पदार्थो के स्वरूप में भ्रांति हो जाती है । मोक्षमार्ग पर सच्ची श्रद्धा नहीं बनती। यह जीव स्वार्थ के वशीभूत होकर कुदेव, कुगुरु और लोकमूढता को ही धर्म मानने लगता है । इसके मूल में आचार्यों ने पाँच कारण माने है (१) एकान्त (२) विपरीत (३) विनय ( ४ ) संशय (५) अज्ञान ।
89
एकान्त के अन्तर्गत जब व्यक्ति अनेकन्त को त्यागकर एकान्त दृष्टि को ही सर्वथा सत्य मानने लगता है और सत्यांश को ही सत्य मान लेता है, तब वह मिथ्यात्व में चला जाता है। इसी प्रकार विपरीत के अन्तर्गत पदार्थ को अन्यथा मानकर अधर्म में विश्वास करने लगता है । ऐसा व्यक्ति सत्य-असत्य का विचार किये बिना विवेक के अभाव में हर किसी को कल्याणकारी मानकर वन्दन आदि करने लगता है । वह निरन्तर संशय में झूलता रहता है और अज्ञान के कारण अतत्त्वों में श्रद्धा करने लगता है। ये पाँच कारण मिथ्यात्व को बढ़ाते हैं और इन्हीं के कारण कर्मबंध होते रहते है ।
(२) अविरति : जो मनुष्य कषायों की तीव्रता से ग्रसित होता है, वह सदाचार या आंशिक रूप से भी चारित्र धारण करने में अरुचि रखता है और निरन्तर विषय भोगों में लिपटा रहता है ।
(३) प्रमाद : प्रमाद का सामान्य अर्थ है असावधान रहना । मनुष्य जब हित और अहित के भेद में सावधानी नहीं रखता है और आत्मकल्याण के कार्यो के प्रति आलस करता है, तब प्रमाद के कारण वह सत्य को नहीं पहचान पाता । इससे शुभ कार्यों की ओर उसकी आस्था या दृढ़ता कम हो जाती है । उसमें हिंसादी भाव बढ़ने लगते हैं। प्रमाद जैसा कि शब्द का ही अर्थ है समस्त पापों की जड़ है । अपनी क्रियाओं और कर्तव्यों में अनादरभाव होना प्रमाद है । यह प्रमाद कषायों के कारण ही होता है । जब मनुष्य स्त्री कथा, भोजन कथा, देशकथा और राजकथा जैसी विकथाओं में उलझ जाता है, चार कषायों से ग्रसित होता है, इन्द्रियों के विषय भोगों में लिप्त होता है, तथा निंद्रा और मोह में फँसता है तब यह सम्यक्त्व से दूर हो जाता है। उसे आत्म चिंतन का ध्यान ही नहीं रहता और यह प्रमाद ही
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org