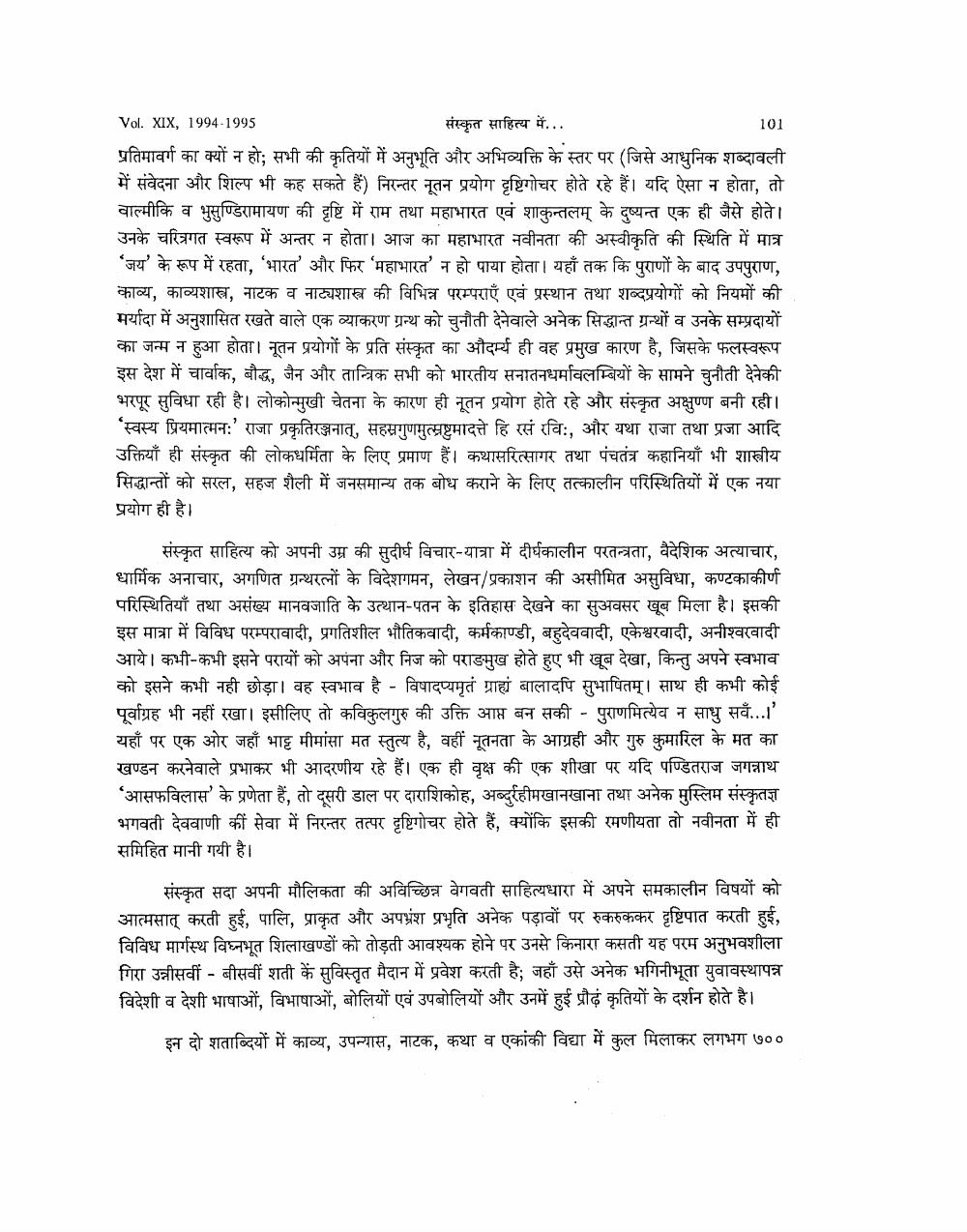________________
Vol. XIX, 1994-1995 संस्कृत साहित्य में...
101 प्रतिमावर्ग का क्यों न हो; सभी की कृतियों में अनुभूति और अभिव्यक्ति के स्तर पर (जिसे आधुनिक शब्दावली में संवेदना और शिल्प भी कह सकते हैं) निरन्तर नूतन प्रयोग दृष्टिगोचर होते रहे हैं। यदि ऐसा न होता, तो वाल्मीकि व भुसुण्डिरामायण की दृष्टि में राम तथा महाभारत एवं शाकुन्तलम् के दुष्यन्त एक ही जैसे होते। उनके चरित्रगत स्वरूप में अन्तर न होता। आज का महाभारत नवीनता की अस्वीकृति की स्थिति में मात्र 'जय' के रूप में रहता, 'भारत' और फिर 'महाभारत' न हो पाया होता। यहाँ तक कि पुराणों के बाद उपपुराण, काव्य, काव्यशास्त्र, नाटक व नाट्यशास्त्र की विभिन्न परम्पराएँ एवं प्रस्थान तथा शब्दप्रयोगों को नियमों की मर्यादा में अनुशासित रखते वाले एक व्याकरण ग्रन्थ को चुनौती देनेवाले अनेक सिद्धान्त ग्रन्थों व उनके सम्प्रदायों का जन्म न हुआ होता। नूतन प्रयोगों के प्रति संस्कृत का औदर्य ही वह प्रमुख कारण है, जिसके फलस्वरूप इस देश में चार्वाक, बौद्ध, जैन और तान्त्रिक सभी को भारतीय सनातनधर्मावलम्बियों के सामने चुनौती देनेकी भरपूर सुविधा रही है। लोकोन्मुखी चेतना के कारण ही नूतन प्रयोग होते रहे और संस्कृत अक्षुण्ण बनी रही। 'स्वस्य प्रियमात्मन:' राजा प्रकृतिरञ्जनात्, सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रवि:, और यथा राजा तथा प्रजा आदि उक्तियाँ ही संस्कृत की लोकधर्मिता के लिए प्रमाण हैं। कथासरित्सागर तथा पंचतंत्र कहानियाँ भी शास्त्रीय सिद्धान्तों को सरल, सहज शैली में जनसमान्य तक बोध कराने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में एक नया प्रयोग ही है।
संस्कृत साहित्य को अपनी उम्र की सुदीर्घ विचार-यात्रा में दीर्घकालीन परतन्त्रता, वैदेशिक अत्याचार, धार्मिक अनाचार, अगणित ग्रन्थरत्नों के विदेशगमन, लेखन/प्रकाशन की असीमित असुविधा, कण्टकाकीर्ण परिस्थितियाँ तथा असंख्य मानवजाति के उत्थान-पतन के इतिहास देखने का सुअवसर खूब मिला है। इसकी इस मात्रा में विविध परम्परावादी, प्रगतिशील भौतिकवादी, कर्मकाण्डी, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अनीश्वरवादी आये। कभी-कभी इसने परायों को अपना और निज को पराङमुख होते हुए भी खूब देखा, किन्तु अपने स्वभाव को इसने कभी नही छोड़ा। वह स्वभाव है - विषादप्यमृतं ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्। साथ ही कभी कोई पूर्वाग्रह भी नहीं रखा। इसीलिए तो कविकुलगुरु की उक्ति आप्त बन सकी - पुराणमित्येव न साधु सर्वं....' यहाँ पर एक ओर जहाँ भाट्ट मीमांसा मत स्तुत्य है, वहीं नूतनता के आग्रही और गुरु कुमारिल के मत का खण्डन करनेवाले प्रभाकर भी आदरणीय रहे हैं। एक ही वृक्ष की एक शीखा पर यदि पण्डितराज जगन्नाथ 'आसफविलास' के प्रणेता , तो दूसरी डाल पर दाराशिकोह, अब्दुर्रहीमखानखाना तथा अनेक मुस्लिम संस्कृतज्ञ भगवती देववाणी की सेवा में निरन्तर तत्पर दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि इसकी रमणीयता तो नवीनता में ही समिहित मानी गयी है।
संस्कृत सदा अपनी मौलिकता की अविच्छिन्न वेगवती साहित्यधारा में अपने समकालीन विषयों को आत्मसात् करती हुई, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश प्रभृति अनेक पड़ावों पर रुकरुककर दृष्टिपात करती हुई, विविध मार्गस्थ विघ्नभूत शिलाखण्डों को तोड़ती आवश्यक होने पर उनसे किनारा कसती यह परम अनुभवशीला गिरा उन्नीसवीं - बीसवीं शती के सुविस्तृत मैदान में प्रवेश करती है; जहाँ उसे अनेक भगिनीभूता युवावस्थापन्न विदेशी व देशी भाषाओं, विभाषाओं, बोलियों एवं उपबोलियों और उनमें हुई प्रौद्रं कृतियों के दर्शन होते है।
इन दो शताब्दियों में काव्य, उपन्यास, नाटक, कथा व एकांकी विद्या में कुल मिलाकर लगभग ७००