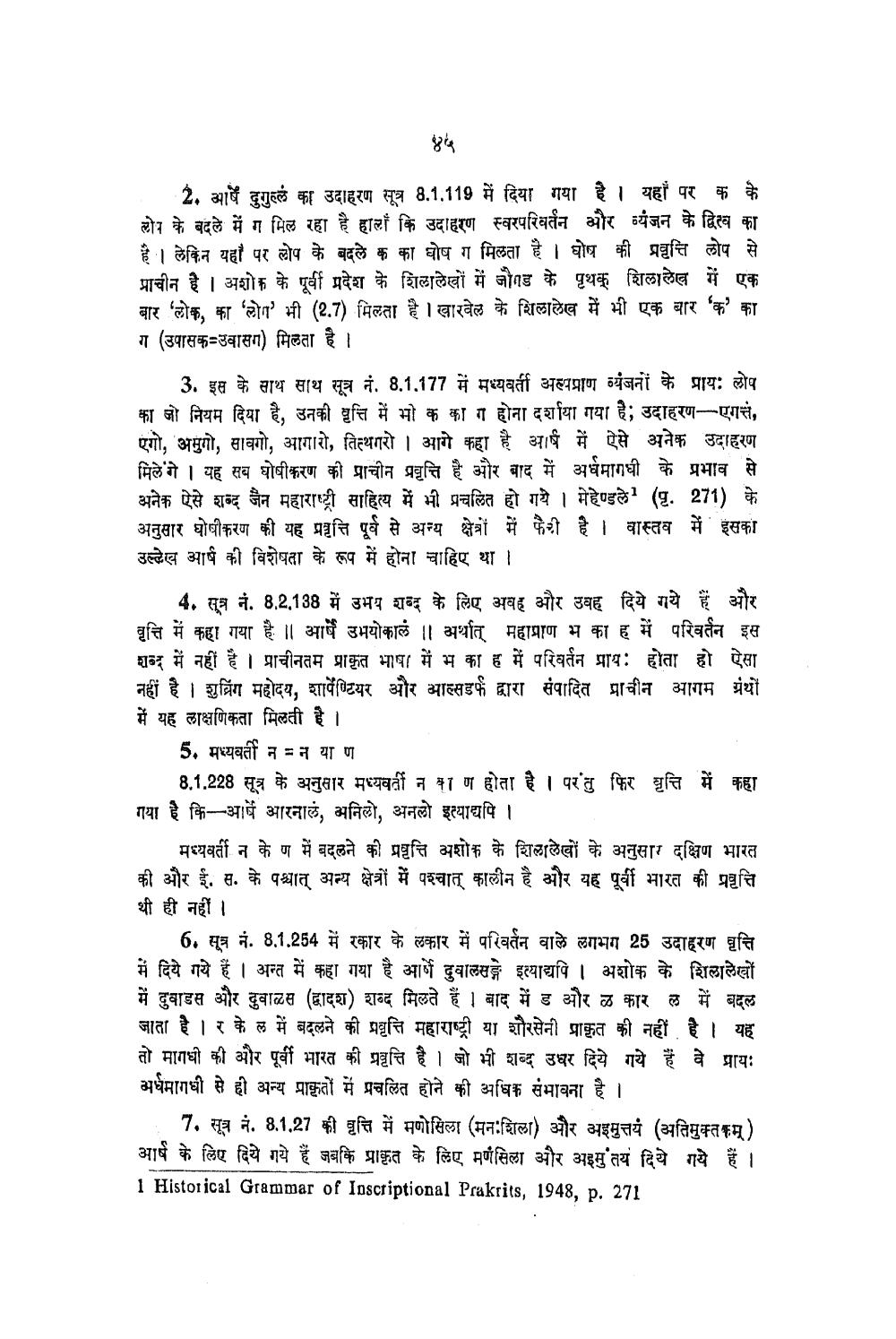________________
४५
2. आषै दुगुल्लं का उदाहरण सूत्र 8.1.119 में दिया गया है । यहाँ पर क के लोन के बदले में ग मिल रहा है हालों कि उदाहरण स्वरपरिवर्तन और व्यंजन के द्विख का है । लेकिन यहाँ पर लोप के बदले क का घोष ग मिलता है । घोष की प्रवृत्ति लोप से प्राचीन है । अशोक के पूर्वी प्रदेश के शिलालेखों में जौड के पृथक् शिलालेख में एक बार 'लोक, का 'लोग' भी ( 27 ) मिलता है । खारवेल के शिलालेख में भी एक बार 'क' का ग ( उपासक = उवास ) मिलता है ।
3. इस के साथ साथ सूत्र नं. 8.1.177 में मध्यवर्ती अल्पप्राण व्यंजनों के प्रायः लोप का जो नियम दिया है, उनकी वृत्ति में भोक का ग होना दर्शाया गया है; उदाहरण - एमत्तं, एंगो, अमुगो, सावगो, आगारो, तिथगरो । आगे कहा है अर्ष में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे । यह सब घोषीकरण की प्राचीन प्रवृत्ति है और बाद में अनेक ऐसे शब्द जैन महाराष्ट्री साहित्य में भी प्रचलित हो गये अनुसार घोषीकरण की यह प्रवृत्ति पूर्व से अन्य क्षेत्रों में फैी है । वास्तव उल्लेख आर्ष की विशेषता के रूप में होना चाहिए था ।
अर्धमागधी के प्रभाव से
।
मेहेण्डले ' (पृ. 271) के
1
इसका
4. सूत्र नं. 8,2,138 में उभय शब्द के लिए अवह और उवह दिये गये हैं और वृत्ति में कहा गया है || आफैँ उभयोकालं | अर्थात् महाप्राण भ का ह में परिवर्तन इस शब्द में नहीं है । प्राचीनतम प्राकृत भाषा में भ का ह में परिवर्तन प्रायः होता हो ऐसा नहीं है । शुक्रिंग महोदय, शार्पेण्टियर और आल्सडर्फ द्वारा संपादित प्राचीन आगम ग्रंथों में यह लाक्षणिकता मिलती है ।
5. मध्यवर्ती न न या ण
8.1.228 सूत्र
के अनुसार मध्यवर्ती नाण होता है । परंतु फिर वृत्ति में कहा आरनालं, अनिलो, अनलो इत्याद्यपि ।
गया है कि
मध्यवर्ती न के ण में बदलने की प्रवृत्ति अशोक के शिलालेखों के अनुसार दक्षिण भारत की और ई. स. के पश्चात् अन्य क्षेत्रों में पश्चात् कालीन है और यह पूर्वी भारत की प्रवृत्ति थी ही नहीं ।
6. सूत्र नं. 8.1.254 में रकार के लकार में परिवर्तन वाले लगभग 25 उदाहरण वृत्ति में दिये गये हैं । अन्त में कहा गया है आर्जे दुवालसङ्गे इत्याद्यपि । अशोक के शिलालेखों में दुवास और दुवास (द्वादश) शब्द मिलते हैं । बाद में ड और ळ कार ल में बदल जाता है । र के ल में बदलने की प्रवृत्ति महाराष्ट्री या शौरसेनी प्राकृत की नहीं है । यह तो मागधी की और पूर्वी भारत की प्रवृत्ति है । जो भी शब्द उधर दिये गये हैं वे प्रायः अर्धमागधी से ही अन्य प्राकृतों में प्रचलित होने की अधिक संभावना है ।
7. सूत्र नं. 8.1.27 की वृत्ति में मनोसिला (मनःशिला) और अइमुत्तयं ( अतिमुक्तकम् ) आर्ष के लिए दिये गये हैं जबकि प्राकृत के लिए मर्णसिला और अइमं तयं दिये गये हैं । 1 Historical Grammar of Inscriptional Prakrits, 1948, p. 271