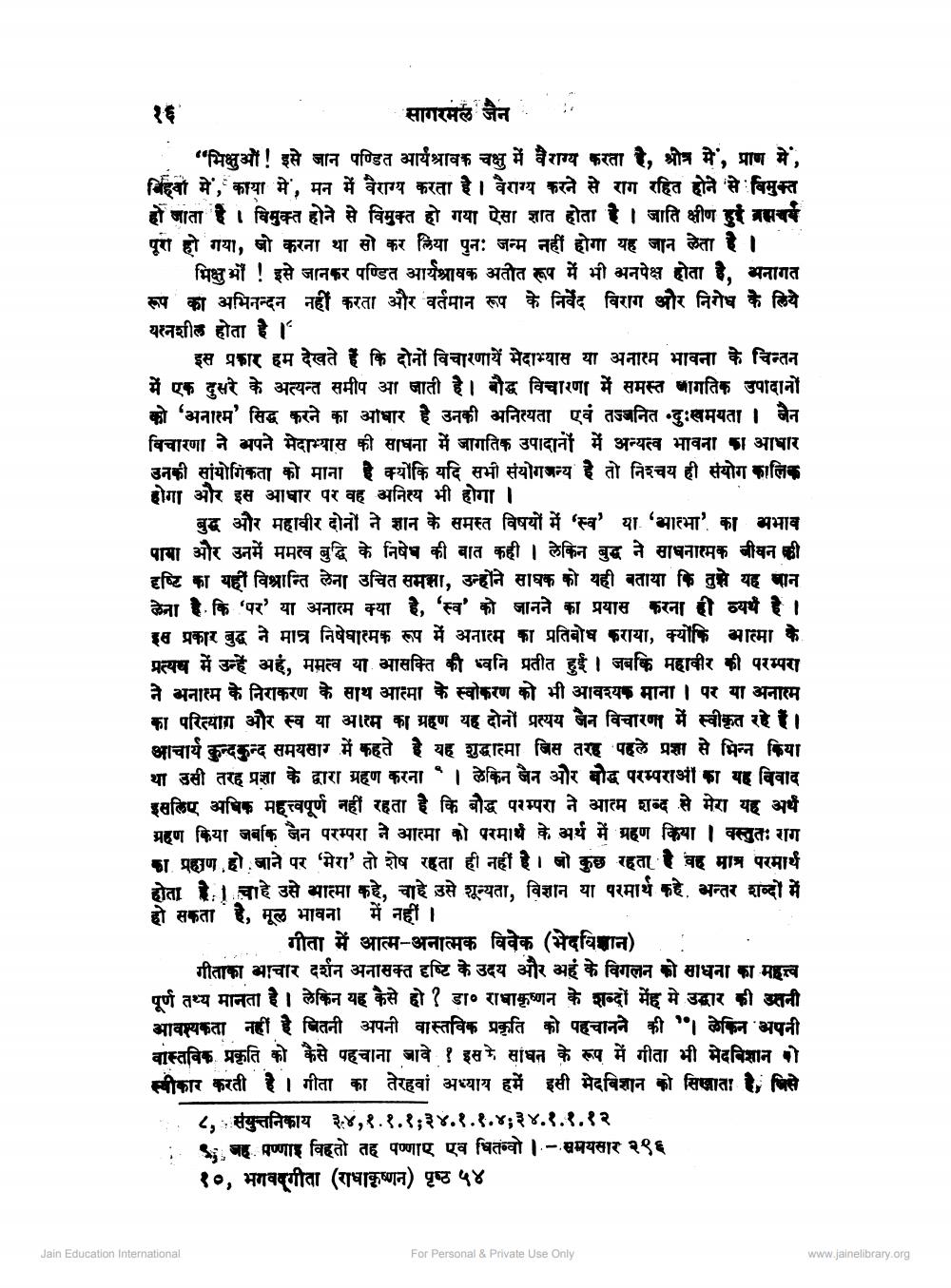________________
सागरमल जैन
"
" भिक्षुओं ! इसे जान पण्डित आर्यभावक चक्षु में वैराग्य करता है, श्रीत्र में प्राण में, हवा में, काया में, मन में वैराग्य करता है। वैराग्य करने से राग रहित होने से विमुक्त हो जाता है। विमुक्त होने से विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञात होता है। जाति क्षीण हुई ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया पुनः जन्म नहीं होगा यह जान लेता है ।
भिक्षु ! इसे जानकर पण्डित आर्यश्रावक अतीत रूप में भी अनपेक्ष होता है, अनागत रूप का अभिनन्दन नहीं करता और वर्तमान रूप के निर्वेद विराग और निरोध के लिये यत्नशील होता है ।
इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों विचारणायें मेदाभ्यास या अनारम भावना के चिन्तन में एक दुसरे के अत्यन्त समीप आ जाती है। बौद्ध विचारणा में समस्त भागतिक उपादानों को 'अनात्म' सिद्ध करने का आधार है उनकी अनित्यता एवं तमनित दुःखमयता | बेन विचारणा ने अपने भेदाभ्यास की साधना में जागतिक उपादानों में अन्यत्व भावना का आधार उनकी सांयोगिकता को माना है क्योंकि यदि सभी संयोगजन्य है तो निश्चय ही संयोग कालिक होगा और इस आधार पर वह अनित्य भी होगा ।
१६
बुद्ध और महावीर दोनों ने ज्ञान के समस्त विषयों में 'स्व' या 'आत्मा' का अभाव पाया और उनमें ममत्व बुद्धि के निषेध की बात कही। लेकिन बुद्ध ने साधनात्मक जीवन की दृष्टि का यहीं विश्रान्ति लेना उचित समझा, उन्होंने साधक को यही बताया कि तुझे यह जान लेना है कि 'पर' या अनारम क्या है, 'स्व' को जानने का प्रयास करना ही व्यर्थ है । इस प्रकार बुद्ध ने मात्र निषेधात्मक रूप में अनात्म का प्रतिबोध कराया, क्योंकि आत्मा के. प्रत्यय में उन्हें अहं ममत्व या आसक्ति की ध्वनि प्रतीत हुई। जबकि महावीर की परम्परा ने अनात्म के निराकरण के साथ आत्मा के स्वोकरण को भी आवश्यक माना । पर या अनारम का परित्याग और स्व या आरम का ग्रहण यह दोनों प्रत्यय जैन विचारणा में स्वीकृत रहे हैं। आचार्य कुन्दकुन्द समयसार में कहते है यह शुद्धात्मा जिस तरह पहले प्रशा से भिन्न किया था उसी तरह प्रशा के द्वारा ग्रहण करना । लेकिन जैन और बौद्ध परम्पराओं का यह विवाद इसलिए अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं रहता है कि बौद्ध परम्परा ने आत्म शब्द से मेरा यह अर्थ ग्रहण किया जबकि जैन परम्परा ने आत्मा को परमार्थ के अर्थ में ग्रहण किया । वस्तुतः राग का प्रहाण हो जाने पर 'मेरा' तो शेष रहता ही नहीं है। जो कुछ रहता है वह मात्र परमार्थ होता है। चाहे उसे भात्मा कहे, चाहे उसे शून्यता, विज्ञान या परमार्थ कहे, अन्तर शब्दों में हो सकता है, मूळ भावना में नहीं ।
९
गीता में आत्म-अनात्मक विवेक (भेदविज्ञान)
गीताका आचार दर्शन अनासक्त दृष्टि के उदय और अहं के विगलन को साधना का महत्त्व पूर्ण तथ्य मानता है। लेकिन यह कैसे हो ? डा० राधाकृष्णन के शब्दों में मे उद्धार की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने की "। लेकिन अपनी वास्तविक प्रकृति को कैसे पहचाना जावे १ इसके साधन के रूप में गीता भी मेदविज्ञान को स्वीकार करती है। गीता का तेरहवां अध्याय हमें इसी भेदविज्ञान को सिखाता है, जिसे
Jain Education International
८, संयुत्तनिकाय ३.४,१.१.१,२४.१.१.४,३४.१.१.१२
S मह प्रण्णा विहतो तद् पण्णाए एव चितन्यो । समयसार २९६
१०, भगवद्गीता (राधाकृष्णन ) पृष्ठ ५४
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org.