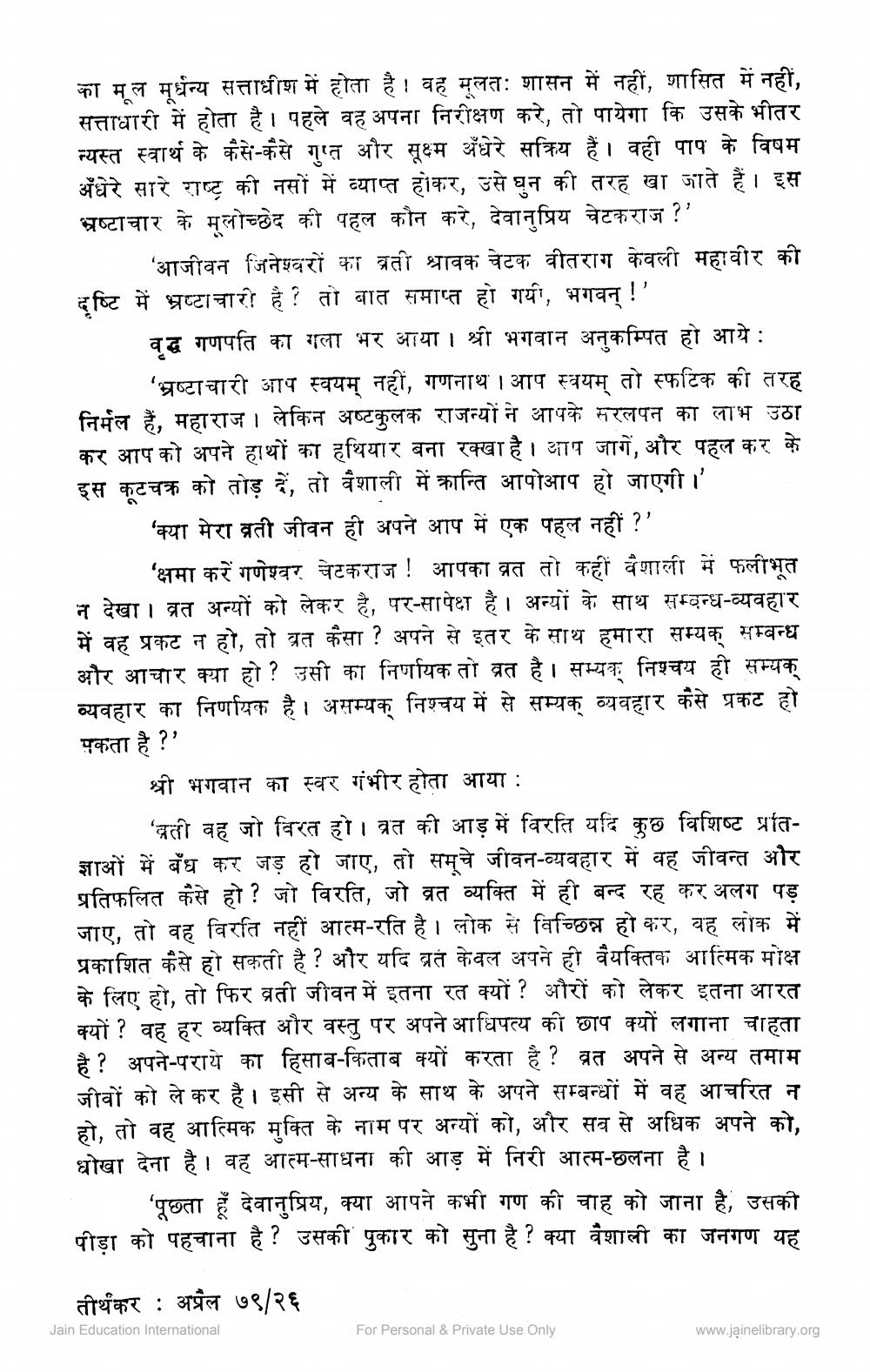________________
का मल मूर्धन्य सत्ताधीश में होता है। वह मूलत: शासन में नहीं, शासित में नहीं, सत्ताधारी में होता है। पहले वह अपना निरीक्षण करे, तो पायेगा कि उसके भीतर न्यस्त स्वार्थ के कैसे-कैसे गुप्त और सूक्ष्म अँधेरे सक्रिय हैं। वही पाप के विषम अँधेरे सारे राष्ट्र की नसों में व्याप्त होकर, उसे घुन की तरह खा जाते हैं। इस भ्रष्टाचार के मलोच्छेद की पहल कौन करे, देवानु प्रिय चेटकराज ?'
___ 'आजीवन जिनेश्वरों का व्रती श्रावक चेटक वीतराग केवली महावीर की दृष्टि में भ्रष्टाचारी है ? तो बात समाप्त हो गयी, भगवन् !'
वृद्ध गणपति का गला भर आया। श्री भगवान अनुकम्पित हो आये :
'भ्रष्टाचारी आप स्वयम् नहीं, गणनाथ । आप स्वयम तो स्फटिक की तरह निर्मल हैं, महाराज। लेकिन अष्टकुलक राजन्यों ने आपके सरलपन का लाभ उठा कर आप को अपने हाथों का हथियार बना रक्खा है। आप जागें, और पहल कर के इस कूटचक्र को तोड़ दें, तो वैशाली में क्रान्ति आपोआप हो जाएगी।'
'क्या मेरा व्रती जीवन ही अपने आप में एक पहल नहीं ?'
'क्षमा करें गणेश्वर चेटकराज! आपका व्रत तो कहीं वैशाली में फलीभूत न देखा। व्रत अन्यों को लेकर है, पर-सापेक्ष है। अन्यों के साथ सम्बन्ध-व्यवहार में वह प्रकट न हो, तो व्रत कैसा? अपने से इतर के साथ हमारा सम्यक् सम्बन्ध
और आचार क्या हो ? उसी का निर्णायक तो व्रत है। सम्यक निश्चय ही सम्यक् व्यवहार का निर्णायक है। असम्यक् निश्चय में से सम्यक् व्यवहार कैसे प्रकट हो पकता है ?'
श्री भगवान का स्वर गंभीर होता आया :
'व्रती वह जो विरत हो। व्रत की आड़ में विरति यदि कुछ विशिष्ट प्रतिज्ञाओं में बँध कर जड़ हो जाए, तो सम्चे जीवन-व्यवहार में वह जीवन्त और प्रतिफलित कैसे हो? जो विरति, जो व्रत व्यक्ति में ही बन्द रह कर अलग पड़ जाए, तो वह विरति नहीं आत्म-रति है। लोक से विच्छिन्न हो कर, वह लोक में प्रकाशित कैसे हो सकती है ? और यदि ब्रत केवल अपने ही वैयक्तिक आत्मिक मोक्ष के लिए हो, तो फिर व्रती जीवन में इतना रत क्यों ? औरों को लेकर इतना आरत क्यों? वह हर व्यक्ति और वस्तु पर अपने आधिपत्य की छाप क्यों लगाना चाहता है? अपने-पराये का हिसाब-किताब क्यों करता है ? व्रत अपने से अन्य तमाम जीवों को ले कर है। इसी से अन्य के साथ के अपने सम्बन्धों में वह आचरित न हो, तो वह आत्मिक मुक्ति के नाम पर अन्यों को, और सब से अधिक अपने को, धोखा देना है। वह आत्म-साधना की आड़ में निरी आत्म-छलना है।
पूछता हूँ देवानुप्रिय, क्या आपने कभी गण की चाह को जाना है, उसकी पीड़ा को पहचाना है? उसकी पुकार को सुना है ? क्या वैशाली का जनगण यह
तीर्थंकर : अप्रैल ७९/२६
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org