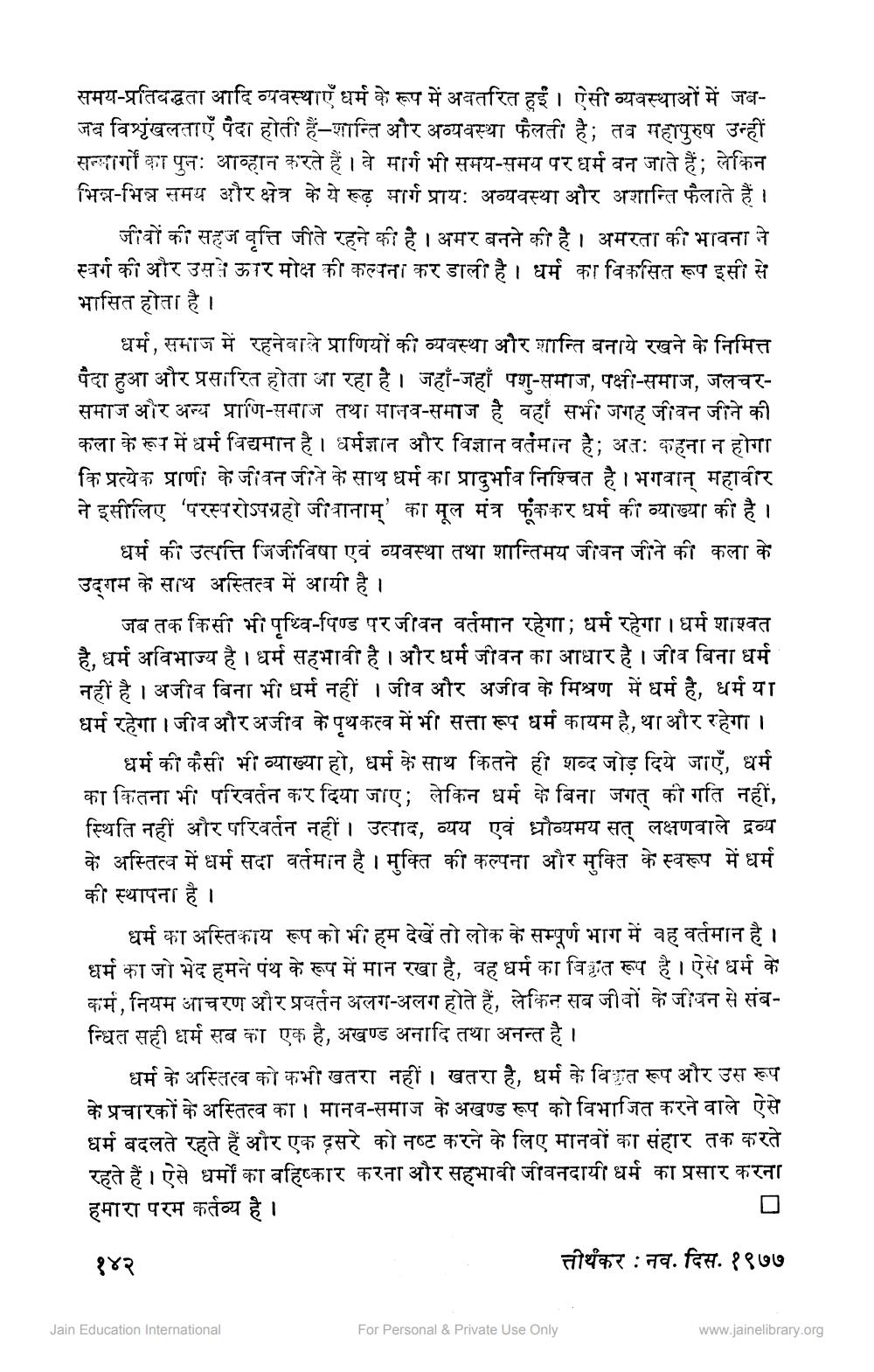________________
समय-प्रतिबद्धता आदि व्यवस्थाएँ धर्म के रूप में अवतरित हुईं। ऐसी व्यवस्थाओं में जबजब विशृंखलताएँ पैदा होती हैं-शान्ति और अव्यवस्था फैलती है; तव महापुरुष उन्हीं सन्मार्गों का पुन: आव्हान करते हैं। वे मार्ग भी समय-समय पर धर्म बन जाते हैं; लेकिन भिन्न-भिन्न समय और क्षेत्र के ये रूढ़ मार्ग प्रायः अव्यवस्था और अशान्ति फैलाते हैं। ___जीवों की सहज वृत्ति जीते रहने की है । अमर बनने की है। अमरता की भावना ने स्वर्ग की और उसो कार मोक्ष की कल्पना कर डाली है। धर्म का विकसित रूप इसी से भासित होता है।
धर्म, समाज में रहनेवाले प्राणियों की व्यवस्था और शान्ति बनाये रखने के निमित्त पैदा हुआ और प्रसारित होता आ रहा है। जहाँ-जहाँ पशु-समाज, पक्षी-समाज, जलचरसमाज और अन्य प्राणि-समाज तथा मानव-समाज है वहाँ सभी जगह जीवन जीने की कला के रूप में धर्म विद्यमान है। धर्मज्ञान और विज्ञान वर्तमान है; अत: कहना न होगा कि प्रत्येक प्राणी के जीवन जीने के साथ धर्म का प्रादुर्भाव निश्चित है। भगवान् महावीर ने इसीलिए 'परस्परोऽपग्रहो जीवानाम्' का मूल मंत्र फूंककर धर्म की व्याख्या की है।
धर्म की उत्पत्ति जिजीविषा एवं व्यवस्था तथा शान्तिमय जीवन जीने की कला के उद्गम के साथ अस्तित्व में आयी है । ___ जब तक किसी भी पृथ्वि-पिण्ड पर जीवन वर्तमान रहेगा; धर्म रहेगा। धर्म शाश्वत है, धर्म अविभाज्य है। धर्म सहभावी है । और धर्म जीवन का आधार है । जीव बिना धर्म नहीं है । अजीव बिना भी धर्म नहीं । जीव और अजीव के मिश्रण में धर्म है, धर्म या धर्म रहेगा। जीव और अजीव के पृथकत्व में भी सत्ता रूप धर्म कायम है, था और रहेगा।
धर्म की कैसी भी व्याख्या हो, धर्म के साथ कितने ही शब्द जोड़ दिये जाएँ, धर्म का कितना भी परिवर्तन कर दिया जाए; लेकिन धर्म के बिना जगत् की गति नहीं, स्थिति नहीं और परिवर्तन नहीं। उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्यमय सत् लक्षणवाले द्रव्य के अस्तित्व में धर्म सदा वर्तमान है । मुक्ति की कल्पना और मुक्ति के स्वरूप में धर्म की स्थापना है। ___ धर्म का अस्तिकाय रूप को भी हम देखें तो लोक के सम्पूर्ण भाग में वह वर्तमान है। धर्म का जो भेद हमने पंथ के रूप में मान रखा है, वह धर्म का विकृत रूप है। ऐसे धर्म के कर्म, नियम आचरण और प्रवर्तन अलग-अलग होते हैं, लेकिन सब जीवों के जीवन से संबन्धित सही धर्म सब का एक है, अखण्ड अनादि तथा अनन्त है।
धर्म के अस्तित्व को कभी खतरा नहीं। खतरा है, धर्म के विकृत रूप और उस रूप के प्रचारकों के अस्तित्व का। मानव-समाज के अखण्ड रूप को विभाजित करने वाले ऐसे धर्म बदलते रहते हैं और एक दूसरे को नष्ट करने के लिए मानवों का संहार तक करते रहते हैं। ऐसे धर्मों का बहिष्कार करना और सहभावी जीवनदायी धर्म का प्रसार करना हमारा परम कर्तव्य है।
१४२
त्तीर्थकर : नव. दिस. १९७७
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org