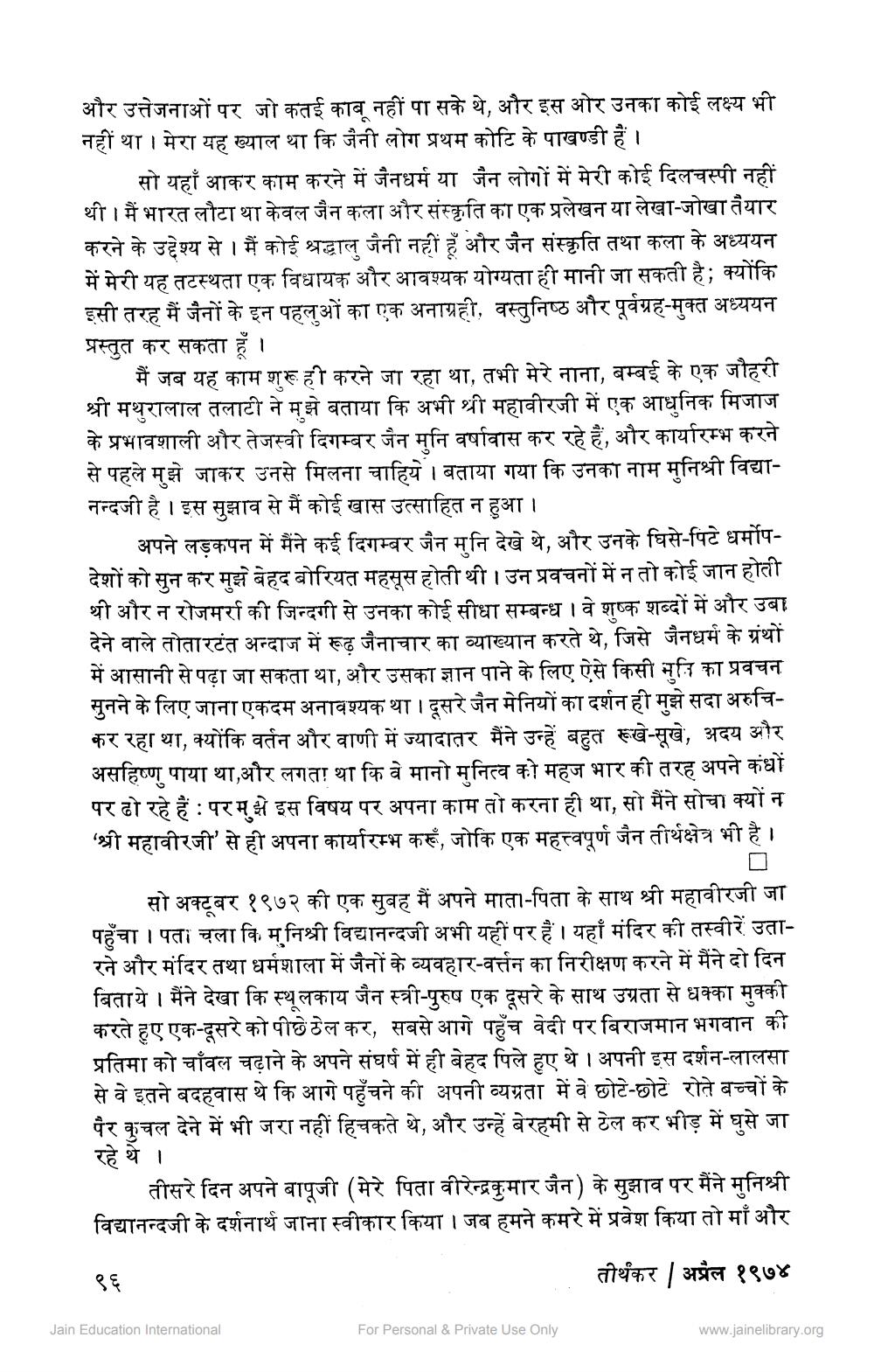________________
और उत्तेजनाओं पर जो कतई काबू नहीं पा सके थे, और इस ओर उनका कोई लक्ष्य भी नहीं था। मेरा यह ख्याल था कि जैनी लोग प्रथम कोटि के पाखण्डी हैं।
सो यहाँ आकर काम करने में जैनधर्म या जैन लोगों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं भारत लौटा था केवल जैन कला और संस्कृति का एक प्रलेखन या लेखा-जोखा तैयार करने के उद्देश्य से । मैं कोई श्रद्धालु जैनी नहीं हूँ और जैन संस्कृति तथा कला के अध्ययन में मेरी यह तटस्थता एक विधायक और आवश्यक योग्यता ही मानी जा सकती है। क्योंकि इसी तरह मैं जैनों के इन पहलुओं का एक अनाग्रही, वस्तुनिष्ठ और पूर्वग्रह-मुक्त अध्ययन प्रस्तुत कर सकता हूँ। ___ मैं जब यह काम शुरू ही करने जा रहा था, तभी मेरे नाना, बम्बई के एक जौहरी श्री मथुरालाल तलाटी ने मुझे बताया कि अभी श्री महावीरजी में एक आधुनिक मिजाज के प्रभावशाली और तेजस्वी दिगम्बर जैन मनि वर्षावास कर रहे हैं, और कार्यारम्भ करने से पहले मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिये । बताया गया कि उनका नाम मुनिश्री विद्यानन्दजी है । इस सुझाव से मैं कोई खास उत्साहित न हुआ।
अपने लड़कपन में मैंने कई दिगम्बर जैन मुनि देखे थे, और उनके घिसे-पिटे धर्मोपदेशों को सुन कर मुझे बेहद बोरियत महसूस होती थी। उन प्रवचनों में न तो कोई जान होती थी और न रोजमर्रा की जिन्दगी से उनका कोई सीधा सम्बन्ध । वे शुष्क शब्दों में और उबा देने वाले तोतारटंत अन्दाज में रूढ जैनाचार का व्याख्यान करते थे, जिसे जैनधर्म के ग्रंथों में आसानी से पढ़ा जा सकता था, और उसका ज्ञान पाने के लिए ऐसे किसी भुति का प्रवचन सुनने के लिए जाना एकदम अनावश्यक था। दूसरे जैन मेनियों का दर्शन ही मुझे सदा अरुचिकर रहा था, क्योंकि वर्तन और वाणी में ज्यादातर मैंने उन्हें बहुत रूखे-सूखे, अदय और असहिष्णु पाया था,और लगता था कि वे मानो मनित्व को महज भार की तरह अपने कंधों पर ढो रहे हैं : पर मुझे इस विषय पर अपना काम तो करना ही था, सो मैंने सोचा क्यों न 'श्री महावीरजी' से ही अपना कार्यारम्भ करूँ, जोकि एक महत्त्वपूर्ण जैन तीर्थक्षेत्र भी है।
सो अक्टूबर १९७२ की एक सुबह मैं अपने माता-पिता के साथ श्री महावीरजी जा पहुँचा। पता चला कि मुनिश्री विद्यानन्दजी अभी यहीं पर हैं। यहाँ मंदिर की तस्वीरें उतारने और मंदिर तथा धर्मशाला में जैनों के व्यवहार-वर्तन का निरीक्षण करने में मैंने दो दिन बिताये । मैंने देखा कि स्थूलकाय जैन स्त्री-पुरुष एक दूसरे के साथ उग्रता से धक्का मुक्की करते हुए एक-दूसरे को पीछे ठेल कर, सबसे आगे पहुँच वेदी पर बिराजमान भगवान की प्रतिमा को चाँवल चढ़ाने के अपने संघर्ष में ही बेहद पिले हुए थे । अपनी इस दर्शन-लालसा से वे इतने बदहवास थे कि आगे पहुँचने की अपनी व्यग्रता में वे छोटे-छोटे रोते बच्चों के पैर कुचल देने में भी जरा नहीं हिचकते थे, और उन्हें बेरहमी से ठेल कर भीड़ में घुसे जा रहे थे ।
तीसरे दिन अपने बापूजी (मेरे पिता वीरेन्द्रकुमार जैन) के सुझाव पर मैंने मुनिश्री विद्यानन्दजी के दर्शनार्थ जाना स्वीकार किया। जब हमने कमरे में प्रवेश किया तो माँ और
२८
तीर्थंकर / अप्रैल १९७४
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org