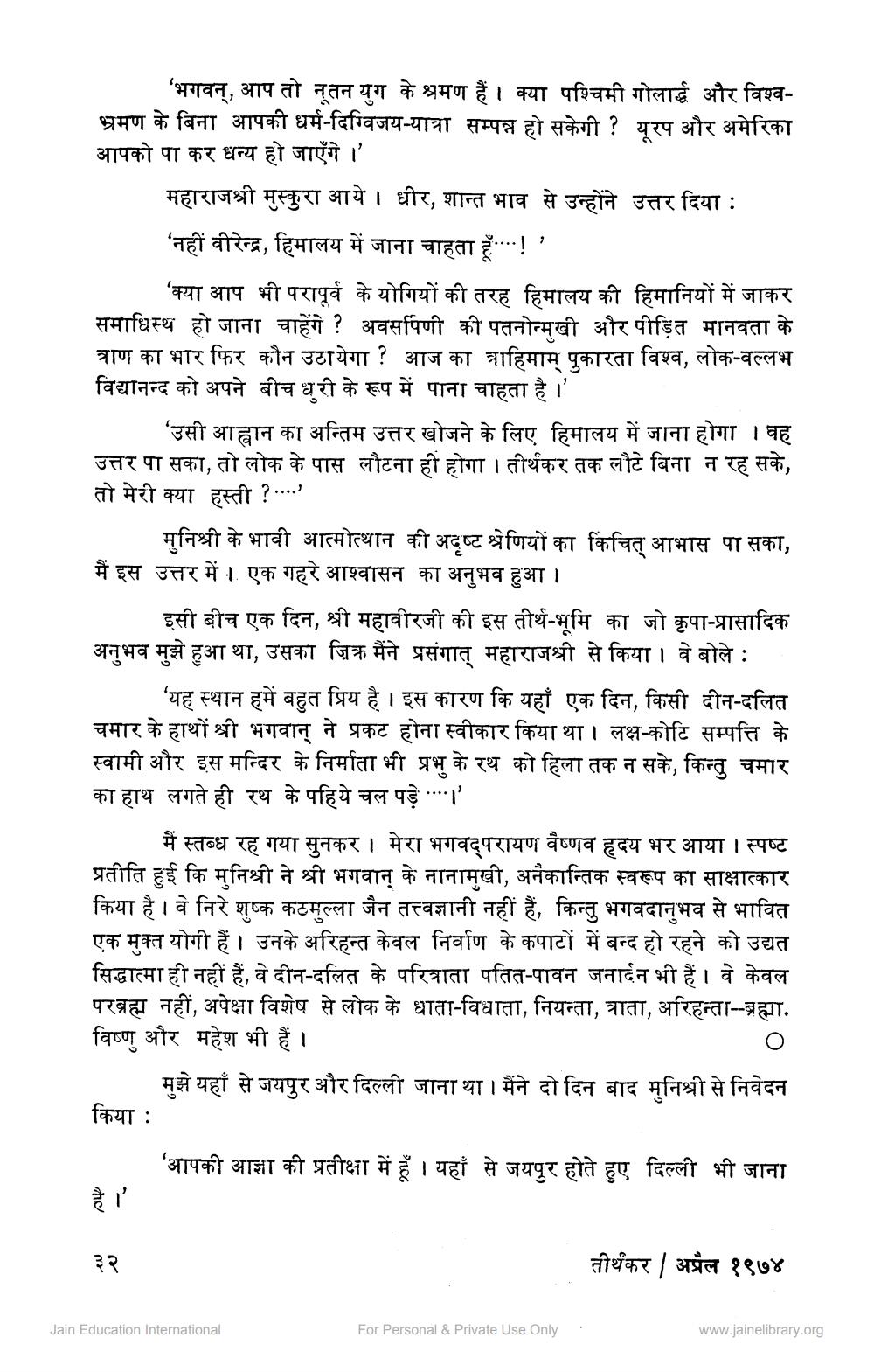________________
'भगवन्, आप तो नूतन युग के श्रमण हैं । क्या पश्चिमी गोलार्द्ध और विश्वभ्रमण के बिना आपकी धर्म - दिग्विजय यात्रा सम्पन्न हो सकेगी ? यूरप और अमेरिका आपको पा कर धन्य हो जाएँगे ।'
महाराजश्री मुस्कुरा आये । धीर, शान्त भाव से उन्होंने उत्तर दिया :
'नहीं वीरेन्द्र, हिमालय में जाना चाहता हूँ...!
'क्या आप भी परापूर्व के योगियों की तरह हिमालय की हिमानियों में जाकर समाधिस्थ हो जाना चाहेंगे ? अवसर्पिणी की पतनोन्मुखी और पीड़ित मानवता के त्राण का भार फिर कौन उठायेगा ? आज का त्राहिमाम् पुकारता विश्व, लोक- वल्लभ विद्यानन्द को अपने बीच धुरी के रूप में पाना चाहता है ।'
'उसी आह्वान का अन्तिम उत्तर खोजने के लिए हिमालय में जाना होगा । वह उत्तर पा सका, तो लोक के पास लौटना ही होगा । तीर्थंकर तक लौटे बिना न रह सके, तो मेरी क्या हस्ती ? -
मुनिश्री के भावी आत्मोत्थान की अदृष्ट श्रेणियों का किंचित् आभास पा सका, मैं इस उत्तर में । एक गहरे आश्वासन का अनुभव हुआ ।
इसी बीच एक दिन, श्री महावीरजी की इस तीर्थ भूमि का जो कृपा - प्रासादिक अनुभव मुझे हुआ था, उसका ज़िक्र मैंने प्रसंगात् महाराज श्री से किया । वे बोले :
'यह स्थान हमें बहुत प्रिय है । इस कारण कि यहाँ एक दिन, किसी दीन-दलित चमार के हाथों श्री भगवान् ने प्रकट होना स्वीकार किया था । लक्ष कोटि सम्पत्ति के स्वामी और इस मन्दिर के निर्माता भी प्रभु के रथ को हिला तक न सके, किन्तु चमार का हाथ लगते ही रथ के पहिये चल पड़े
,
है ।'
****
मैं स्तब्ध रह गया सुनकर । मेरा भगवद् परायण वैष्णव हृदय भर आया । स्पष्ट प्रतीति हुई कि मुनिश्री ने श्री भगवान् के नानामुखी, अनैकान्तिक स्वरूप का साक्षात्कार किया है । वे निरे शुष्क कठमुल्ला जैन तत्त्वज्ञानी नहीं हैं, किन्तु भगवदानुभव से भावित एक मुक्त योगी हैं । उनके अरिहन्त केवल निर्वाण के कपाटों में बन्द हो रहने को उद्यत सिद्धात्मा ही नहीं हैं, वे दीन-दलित के परित्राता पतित-पावन जनार्दन भी हैं । वे केवल परब्रह्म नहीं, अपेक्षा विशेष से लोक के धाता विधाता, नियन्ता, त्राता, अरिहन्ता -- ब्रह्मा. विष्णु और महेश भी हैं ।
३२
।'
मुझे यहाँ से जयपुर और दिल्ली जाना था । मैंने दो दिन बाद मुनिश्री से निवेदन किया :
'आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में हूँ । यहाँ से जयपुर होते हुए दिल्ली भी जाना
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
तीर्थंकर | अप्रैल १९७४
www.jainelibrary.org