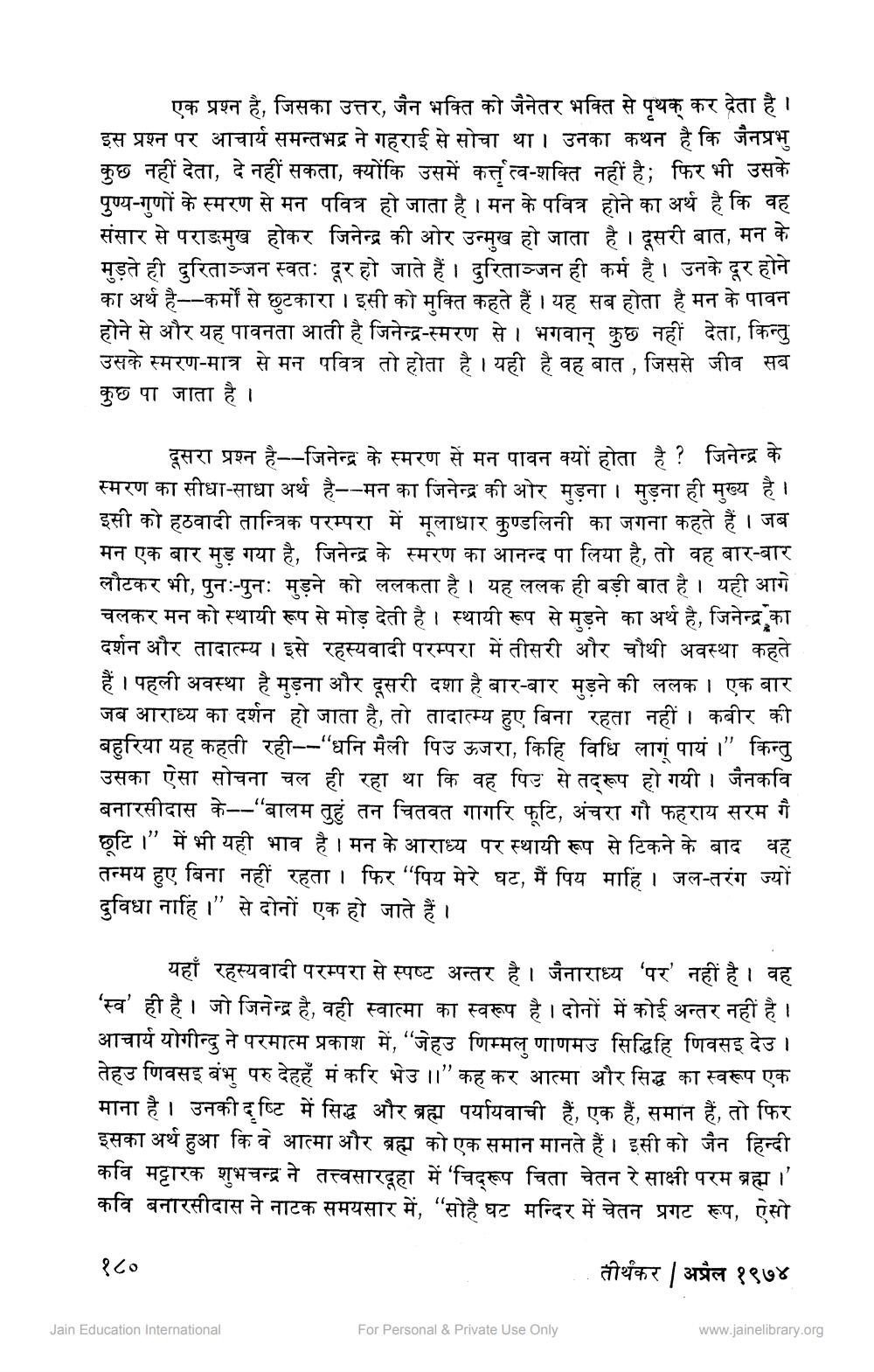________________
एक प्रश्न है, जिसका उत्तर, जैन भक्ति को जैनेतर भक्ति से पृथक् कर देता है । इस प्रश्न पर आचार्य समन्तभद्र ने गहराई से सोचा था । उनका कथन है कि जैनप्रभु कुछ नहीं देता, दे नहीं सकता, क्योंकि उसमें कर्तृत्व-शक्ति नहीं है; फिर भी उसके पुण्य-गुणों के स्मरण से मन पवित्र हो जाता है । मन के पवित्र होने का अर्थ है कि वह संसार से पराङ्मुख होकर जिनेन्द्र की ओर उन्मुख हो जाता है । दूसरी बात, मन के मुड़ते ही दुरिताञ्जन स्वतः दूर हो जाते हैं । दुरिताञ्जन ही कर्म है । उनके दूर हो का अर्थ है—–कर्मों से छुटकारा । इसी को मुक्ति कहते हैं । यह सब होता है मन के पाव होने से और यह पावनता आती है जिनेन्द्र - स्मरण से । भगवान् कुछ नहीं देता, किन्तु उसके स्मरण मात्र से मन पवित्र तो होता है । यही है वह बात, जिससे जीव सब कुछ पा जाता है ।
दूसरा प्रश्न है -- जिनेन्द्र के स्मरण से मन पावन क्यों होता है ? जिनेन्द्र के स्मरण का सीधा-साधा अर्थ है -- मन का जिनेन्द्र की ओर मुड़ना । मुड़ना ही मुख्य है । इसी को हठवादी तान्त्रिक परम्परा में मूलाधार कुण्डलिनी का जगना कहते हैं । जब मन एक बार मुड़ गया है, जिनेन्द्र के स्मरण का आनन्द पा लिया है, तो वह बार-बार लौटकर भी, पुनः-पुनः मुड़ने को ललकता है । यह ललक ही बड़ी बात है । यही आगे चलकर मन को स्थायी रूप से मोड़ देती है । स्थायी रूप से मुड़ने का अर्थ है, जिनेन्द्र का दर्शन और तादात्म्य । इसे रहस्यवादी परम्परा में तीसरी और चौथी अवस्था कहते हैं । पहली अवस्था है मुड़ना और दूसरी दशा है बार-बार मुड़ने की ललक । एक बार जब आराध्य का दर्शन हो जाता है, तो तादात्म्य हुए बिना रहता नहीं । कबीर की बहुरिया यह कहती रही -- “ धनि मैली पिउ ऊजरा, किहि विधि लागूं पायं । " किन्तु उसका ऐसा सोचना चल ही रहा था कि वह पिउ से तद्रूप हो गयी । जैनकवि बनारसीदास के ——“बालम तुहुं तन चितवत गागरि फूटि, अंचरा गौ फहराय सरम गै छूटि ।” में भी यही भाव है । मन के आराध्य पर स्थायी रूप से टिकने के बाद तन्मय हुए बिना नहीं रहता । फिर " पिय मेरे घट, मैं पिय माहि । जल-तरंग ज्यों दुविधा नाहि । " से दोनों एक हो जाते हैं ।
वह
1
यहाँ रहस्यवादी परम्परा से स्पष्ट अन्तर है । जैनाराध्य 'पर' नहीं है । वह 'स्व' ही है । जो जिनेन्द्र है, वही स्वात्मा का स्वरूप है । दोनों में कोई अन्तर नहीं है । आचार्य योगीन्दु ने परमात्म प्रकाश में, “ जेहउ णिम्मलु णाणमउ सिद्धिहि णिवसइ देउ । तेहउ णिवसइ बंभु परु देहहँ मं करि भेउ ।। " कह कर आत्मा और सिद्ध का स्वरूप एक माना है । उनकी दृष्टि में सिद्ध और ब्रह्म पर्यायवाची हैं, एक हैं, समान हैं, तो फिर इसका अर्थ हुआ कि वे आत्मा और ब्रह्म को एक समान मानते हैं । इसी को जैन हिन्दी कवि मट्टारक शुभचन्द्र ने तत्त्वसारगुहा में 'चिद्रूप चिता चेतन रे साक्षी परम ब्रह्म ।' कवि बनारसीदास ने नाटक समयसार में, “सोहै घट मन्दिर में चेतन प्रगट रूप ऐसो
१८०
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
तीर्थंकर | अप्रैल १९७४
www.jainelibrary.org