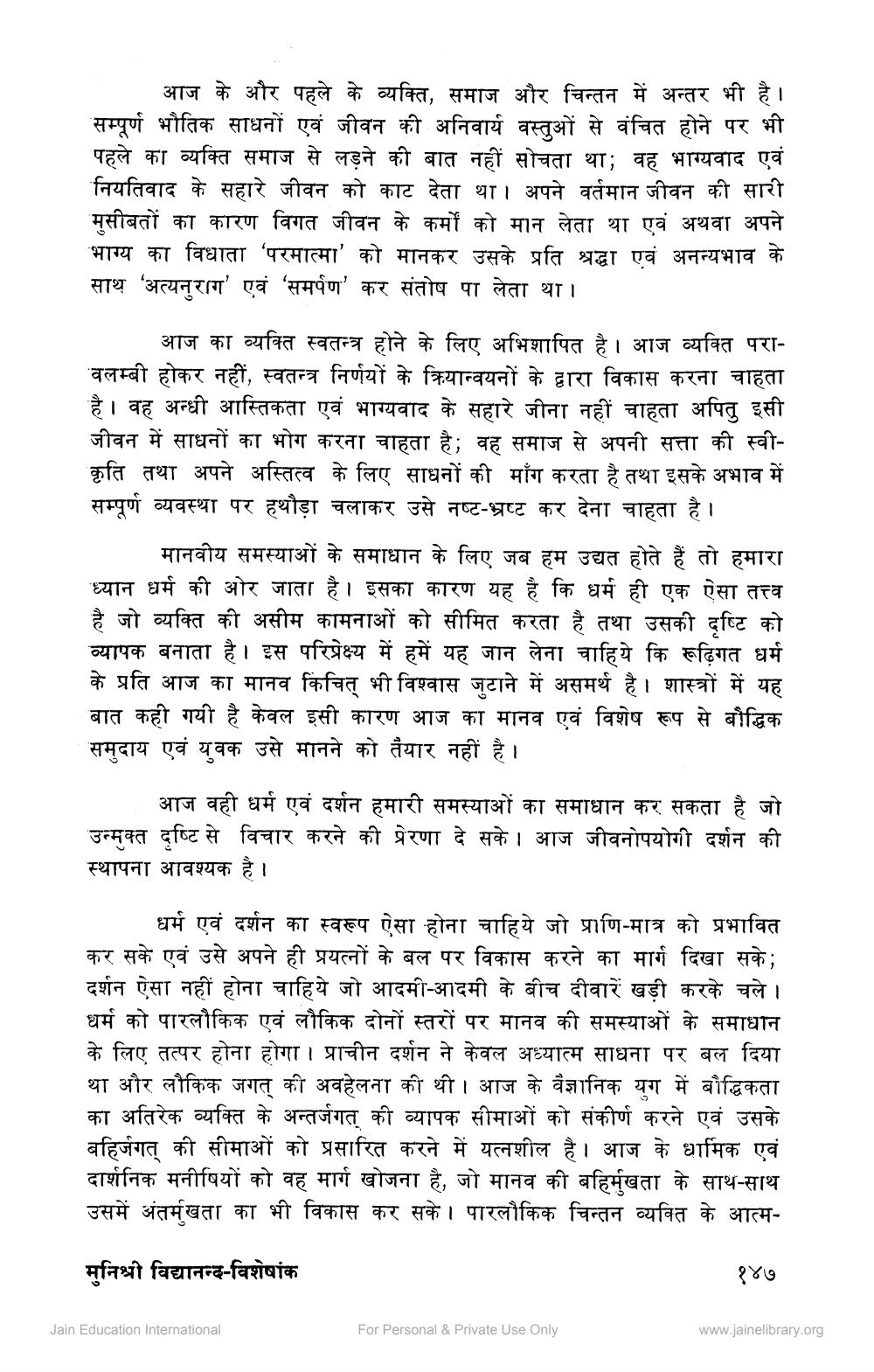________________
आज के और पहले के व्यक्ति, समाज और चिन्तन में अन्तर भी है । सम्पूर्ण भौतिक साधनों एवं जीवन की अनिवार्य वस्तुओं से वंचित होने पर भी पहले का व्यक्ति समाज से लड़ने की बात नहीं सोचता था; वह भाग्यवाद एवं नियतिवाद के सहारे जीवन को काट देता था । अपने वर्तमान जीवन की सारी मुसीबतों का कारण विगत जीवन के कर्मों को मान लेता था एवं अथवा अपने भाग्य का विधाता 'परमात्मा' को मानकर उसके प्रति श्रद्धा एवं अनन्यभाव के साथ ‘अत्यनुराग' एवं 'समर्पण' कर संतोष पा लेता था ।
आज का व्यक्ति स्वतन्त्र होने के लिए अभिशापित है । आज व्यक्ति परावलम्बी होकर नहीं, स्वतन्त्र निर्णयों के क्रियान्वयनों के द्वारा विकास करना चाहता है। वह अन्धी आस्तिकता एवं भाग्यवाद के सहारे जीना नहीं चाहता अपितु इसी जीवन में साधनों का भोग करना चाहता है; वह समाज से अपनी सत्ता की स्वीकृति तथा अपने अस्तित्व के लिए साधनों की माँग करता है तथा इसके अभाव में सम्पूर्ण व्यवस्था पर हथौड़ा चलाकर उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देना चाहता है ।
मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए जब हम उद्यत होते हैं तो हमारा ध्यान धर्म की ओर जाता है। इसका कारण यह है कि धर्म ही एक ऐसा तत्त्व है जो व्यक्ति की असीम कामनाओं को सीमित करता है तथा उसकी दृष्टि को व्यापक बनाता है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें यह जान लेना चाहिये कि रूढ़िगत धर्म के प्रति आज का मानव किंचित् भी विश्वास जुटाने में असमर्थ है। शास्त्रों में यह बात कही गयी है केवल इसी कारण आज का मानव एवं विशेष रूप से बौद्धिक समुदाय एवं युवक उसे मानने को तैयार नहीं है ।
आज वही धर्म एवं दर्शन हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है जो उन्मुक्त दृष्टि से विचार करने की प्रेरणा दे सके । आज जीवनोपयोगी दर्शन की स्थापना आवश्यक है ।
धर्म एवं दर्शन का स्वरूप ऐसा होना चाहिये जो प्राणिमात्र को प्रभावित कर सके एवं उसे अपने ही प्रयत्नों के बल पर विकास करने का मार्ग दिखा सके; दर्शन ऐसा नहीं होना चाहिये जो आदमी आदमी के बीच दीवारें खड़ी करके चले । धर्म को पारलौकिक एवं लौकिक दोनों स्तरों पर मानव की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर होना होगा। प्राचीन दर्शन ने केवल अध्यात्म साधना पर बल दिया था और लौकिक जगत् की अवहेलना की थी । आज के वैज्ञानिक युग में बौद्धिकता का अतिरेक व्यक्ति के अन्तर्जगत् की व्यापक सीमाओं को संकीर्ण करने एवं उसके बहिर्जगत् की सीमाओं को प्रसारित करने में यत्नशील है । आज के धार्मिक एवं दार्शनिक मनीषियों को वह मार्ग खोजना है, जो मानव की बहिर्मुखता के साथ-साथ उसमें अंतर्मुखता का भी विकास कर सके । पारलौकिक चिन्तन व्यक्ति के आत्म
मुनिश्री विद्यानन्द - विशेषांक
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
१४७
www.jainelibrary.org